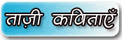बागीचा
‘माँ’ ने ख्वाबों का
बागीचा बना रखा है
वहीं से हर रोज़
तोड़ लाती है
हौसलों के फल
इत्तेफ़ाक़
उसके ख्वाब ...
मेरे ख्वाब ...
अलग-अलग हैं
ये महज इत्तेफ़ाक़ है
दोनों के ख्वाब में ...
दोनों ही हैं!
वंशज
बहन ने
भाई सरीखे पति के लिए
मन्नत माँगी थी
भाई ने भी
अपनी बहन जैसी ही
लड़की से शादी की ठानी है
ये आदम के वंशज
कहाँ आ गए हैं!
रहस्य
सुबह रास्ते पर...दोनों मिले थे
मैं भी...मेरा साया भी
शाम को मैं लौटा घर
रास्ते में साया कहीं रह गया...
ये नियम था या इंतज़ार..
..क्योंकि जिस दिन सिर्फ साया लौटा
उसके बाद से अब तक
मैं नहीं दिखा हूँ !
उलझन (1)
सड़क के किनारे
ख़ुद से टकरा कर
वो गिर पड़ा है...
वो निकला था शिकार को..
ख़ुद को पाकर
अब हिल चुका है
उलझन (2)
सड़क पर ही दोनों पड़े थे
ज़िंदगी भी...मौत भी...
संभल जाता तो मौत मिलती
बिखर जाता तो ज़िंदगी...
लेकिन वो सोच रहा है...
ठीक वैसे ही
जैसे...पहली बार
आदम फल खाने को सोच रहा था।
फितूर
इक चाहत...
उससे लिपटीं चाहतें...
उनके अंदर सिमटी चाहतें...
उन चाहतों से जुड़ी...
छोटी-छोटी शबनमी चाहतें....
...और फिर बेवजह
कोनों को देखना..मुस्कुरा देना...
फितूर ही तो है...
मजबूरी
बेवजह ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ
बेवजह हँसना-गाना...खाना-पीना...बहुत कुछ
लेकिन सच कह रहा हूँ
बेवजह आजतक रोया नहीं हूँ...
और रोना हर रोज़ पड़ता है...
पता नहीं क्यों….???
बुढ़ापा
अनुभव के पराकाष्ठा के साथ
समय के आगे नतमस्तक हो जाना
बुढ़ापा...कई कमियों का नाम है
इस अवस्था में कम हो जाती है...
नींद...भूख...प्यास और आकर्षण
लेकिन खत्म कुछ भी नहीं होता!
आकर्षण
विपरीत गुण-धर्म के बीच
आकर्षण...एक नियम है
समय के सापेक्ष
इसमें कमी भी...एक सत्य है
लेकिन एक झुकाव बना रहता है....
क्योंकि...नियम है !