दोहा सागर है अगम, कहीं न मिलती थाह.
उतनी गहराई मिले, जितना लो अवगाह.
रश्मि प्रभा जी-श्याम जी, स्वागत कर स्वीकार.
उपकृत हमको कीजिये, कुछ दोहे उच्चार..
डॉ. श्याम गुप्ता जी!
आपने बिलकुल सही कहा है, गोष्ठी १२ के प्रथम दोहे के तृतीय चरण में १३ के स्थान पर १४ मात्राएँ हैं. दोहा है-
दोहा दे शुभकामना, रहिये सदा प्रसन्न.
कीर्ति सफलता लाई है, बैसाखी आसन्न..
आँखों में तकलीफ के कारण जैसे-तैसे इस सामग्री को टंकित किया...चूक हुई, पूरी कक्षा और युग्म परिवार के प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, भविष्य में अधिक सजग रहने का प्रयास होगा. तीसरे चरण को इस तरह १३ मात्राओं में रखा जा सकता है-
'लाई है यश-सफलता', शेष दोहा पूर्व की तरह.
शन्नो जी! आपको साधुवाद...निरंतर प्रयास करने और द्रुत गति से छंद पर अधिकार पाने के प्रयास के लिए. आये! आपकी पंक्तियों का मंथन करें.
दुखी बहुत ही मन हुआ, समझ ना कुछ आया
जब मिला आपका साथ, तब जरा लिख पाया
आदत गिनती की पड़ी, मनु का कहना मान
बूँद-बूँद पी ज्ञान की, अब आई मुसकान.
उक्त पंक्तियों में १३-१३ मात्रा हैं. यह दोहा का विधान है किन्तु प्रथम दो पंक्तियों में दीर्घ पदांत है जो दोहे में वर्जित है. इन्हें देख लीजिये. अंतिम दो पंक्तियाँ दोहा हैं और त्रुटिरहित हैं.
पाया मैंने बस तनिक, मुझे बहुत ना ज्ञान
मैं छोटी सी कंकरी, आप ज्ञान की खान
आप ज्ञान की खान, चमकते हीरे जिसमे
तुलना कोई करे, हो सके साहस किसमें
रहे सभी के साथ, 'शन्नो' को भी बताया
साथ आपका मिला, हमने बहुत ही पाया.
प्रथम ४ पंक्तियाँ बिलकुल सही हैं. अंतिम दो पंक्तियों विशेषकर अंतिम चरण को शायद आप परिवर्तित करना चाहें 'हमने बहुत ही पाया' पद के भाव को आप सी प्रतिभावान कवयित्री बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकती है. कृपया एक प्रयास और...
कुंडली:
खड़ी हुई रसोई में, मैं करती थी कुछ काम
उसी समय याद आया, एक गाने का नाम
एक गाने का नाम, जिसमे आँसू भरे तराने
मूड में कुछ आकर, लगी मैं उसको गाने
मनु की बातें पढीं, 'शन्नो' बहुत हँस पड़ी
आज्ञा पा 'सलिल'की, मैं कुंडली लिखूं खड़ी.
रोला:
किया किचन में काम, लगी मैं गाने गाना
मनु ने जान तुंरत, शुरू कर दिया खिझाना
हंसी में फंसकर, फिर गयी किचन को भूल
ही, ही, ही मैं हंसी, मैं भी कैसी हूँ फूल.
इन दोनों रचनाओं में आपने प्रत्युत्पन्नमतित्व का परिचय दिया है, बधाई। यह गुण जिस कवि में हो वह हमेशा सराहा जाता है. आप रचना लिखने के बाद शीघ्रता न कर एक बार दोहरा लें तो वे बिलकुल सही हो जायेंगी.
रही रसोई में खडी, मैं करती कुछ काम
आया याद उसी समय, एक गीत का नाम
एक गीत का नाम, थे अश्रु भरे तराने
मस्ती में आ गयी, लगी मैं उसको गाने
मनु की बातें पढीं, हँस पड़ी 'शन्नो' बरबस.
बात 'सलिल' की मान, कुंडली लिखी मिले जस..
रोला:
किया किचन में काम, लगी मैं गाने गाना
मनु ने जान तुंरत, शुरू कर दिया खिझाना
फँसी हँसी में 'शन्नो', गयी किचन को भूल
ही, ही, ही मैं हँसी, लगी फूल या फूल.
तपन शर्मा said...
मात्रा का नहीं है भय, करूँ हमेशा जोड़
शब्दों का न ज्ञान मुझे, मैं शिल्प न दूँ तोड़..
रामचरित लो खोल, सोरठा देखने के लिये
जी भर कर लो बोल, हैं अनेकों उदाहरण
तपन जी! शुभकामनाएँ...दोहा लेखन का सफ़र बिना किसी हिचक के प्रारंभ कर दें, उक्त में किये जा रहे संशोधनों को समझें और तद्नुसार लिखें.
मात्रा का भय नहीं है ,करुँ हमेशा जोड़.
ज्ञान न शब्दों का मुझे, शिल्प न दूं मैं तोड़..
देख सोरठा छंद, रामचरित मानस उठा.
पा जी भर आनंद, हैं अनेकों उदाहरण
पूजा जी!
दोहा सत के निकट, ज्यों-, छिपा ह्रदय में सत्य
मिथ्या जग संसार यह , अजब कराये नृत्य .
ता-ता-थैया जगत की, समझ न आती रीत.
लालच की लौ ना बुझे, रुसवा हो मन मीत..
गुरु नानक देव के दोहों को अनूदित करने के प्रयास के लिए आप साधुवाद की पात्र हैं. मैंने इन्हें इस तरह किया है-
पहले मरण कुबूल कर, जीवन दी छंड आस.
हो सबनां दी रेनकां, आओ हमरे पास..
मृत्यु प्रथम स्वीकार कर, जीवन की तज आस.
सबकी जाग्रति हो सके,आओ मेरे पास..
सोचै सोच न होवई, जे सोची लखवार.
चुप्पै चुप्प न होवई, जे लाई लिवतार..
नहीं सोचने से मिले. सोचो लाखों बार.
हो कदापि वह चुप नहीं, कोशिश करो हजार..
इक दू जीभौ लख होहि, लख होवहि लख वीस.
लखु लखु गेडा आखिअहि, एकु नामु जगदीस..
जीभ एक-दो लाख या, बीसों लाखों बार.
बाद अनंतों चक्र के,हो जगदीश उचार..
जुड़े सुरिंदर जी नमन, रत्ती-रत्ती ज्ञान.
तब मिलता जब कर सकें, नित्य निरंतर ध्यान.
दोहा लेखन के कला दोहाकार की सामर्थ्य को निरंतर कसौटी पर कसती है. 'दोहा मंजरी' के रचनाकार श्री गजाधर कवि ने दोहा के २३ प्रकारों का वर्णन एक छंद में कर अपने नैपुण्य का परिचय दिया है-
भ्रमर सुभ्रामर शरभ श्येन मंडूक बखानहु.
मरकत करभ सु और नरहि हंसहि परिमानहु..
गनहु गयंद सु और पयोधर बल अवरेखहु.
वानर त्रिकल प्रतच्छ, कच्छपहु मच्छ विसेखहु.
शार्दूल अहिबरहु व्यालयुत वर विडाल अरु.अश्व्गनि
उद्दाम उदर अरु सर्प शुभ तेइस विधि दोहा करनि.
दोहा की चौपाल में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक अंग्रेज से. चकराइये मत, वे आपको दोहा तो सुनायेंगे पर अंगरेजी में नहीं हिन्दी में ही सुनायेंगे. इन महाशय क नाम है श्री फ्रेडरिक पिंकोट जो संवत १९४३ में भारत में थे. वे भारत में बाल शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तक लिखनेवाले तथा उस समय के श्रेष्ठ साहित्यकारों से पत्राचार में दोहा-सोरठा का प्रयोग करनेवाले प्रथम अंग्रेज थे. श्री पिंकोट ने इंग्लैंड लौटकर नगरी तथा कैथी लिपि में 'बाल-दीपक' (४भाग) तथा 'विक्टोरिया चरित' पुस्तकें लिखीं. ये पुस्तकें खड्गविलास प्रेस बांकीपुर से मुद्रित हुईं थीं. श्री पिंकोट ने बाबू कार्तिक प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र कों गद्य-पद्य में कई पत्र लिखे. दोहा-सोरठा के अद्भुत शैल्पिक सौंदर्य पर मुग्ध श्री पिंकोट रचित निम्न सोरठा तथा दोहा स्मरण कर हम उन्हें नमन करेंगे...इन छंदों कों कठिन पानेवाले सोचें कि हिन्दी न जाननेवाले इस अंग्रेज ने पहले हिंदी और फिर छंद-पिंगल कैसे सीखा होगा? क्या हमारी कठिनाई इससे भी अधिक है या हमारे प्रयास कम हैं? श्री पिंकोट ने पत्र का उत्तर न मिलने पर स्नेह-सिक्त शिकायत सोरठा रचकर की -
बैस वंस अवतंस, श्री बाबू हरिचंद जू.
छीर-नीर कलहंस, टुक उत्तर लिख दे मोहि.
श्रीयुत सकल कविंद, कुलनुत बाबू हरिचंद.
भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो जनु चंद.
---शेष फिर




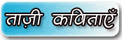



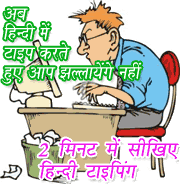
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
16 कविताप्रेमियों का कहना है :
दोहा गाथा से हुए, सारे श्रोता गोल.
क्या चुनाव में लीन हो बदल रहे भूगोल?
बदल रहे भूगोल, न इसको स्वर्ग बना दें.
जीते जी ही नहीं स्वर्ग की सैर करा दें.
'सलिल' डाल मत, अवसर चूक न अब हाथ से.
सारे श्रोता गोल हुए दोहा गाथा से.
'सलिल' जी,
अरे नहीं, मेरी तरफ से ऐसी बात नहीं है. दोहा के मैदान से अभी नहीं भाग रही हूँ. मैं भी जरा कुछ दोहा की सामिग्री जुटा लूं तब फिर से प्रकट हो जाऊंगी. यह कमेन्ट आपको तसल्ली देने के लिए है. दिमाग टटोलना होगा, हो सकता है कल तक कुछ भेजे में आ जाये. आज जरा कुछ अन्य कार्य में व्यस्त थी.
दिव्यनर्मदा.ब्लागस्पाट.कॉम
शन्नो जी हैं साथ तो,'सलिल'करे क्यों फ़िक्र?
साथ हूर लंगूर का, भी होता है ज़िक्र.
हा हा हा, ही ही ही, हू हू हू ...
(केवल हास्य के लिए, कृपया अन्यथा न लें...)
क्या बात है आचार्या,,,,,?
वाकई में आप हूर हैं,,,,,,,हा,,,हा,,,हा,,,,
ये अंग्रेज वाला दोहा समझ में तो कम आया पर ये जानकार ही मजा आ गया के एक अंग्रेज का लिखा हुआ है,,,,,,सच में कितना जतन किया होगा उसने,,,,,
शन्नो जी से भी ज्यादा,,,,,
ऐसी जानकारी के लिए धन्यवाद,,,,
और ये दोहा मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ या वाकई ये शब्द मुश्किल हैं,,,,,
मनु जी!
शन्नो जी जैसी दृढ़ संकल्पी विदुषी के साथ सतत चलायमान सलिल...हूर और लंगूर ही तो हुए. प्रथम पंक्ति में जिस क्रम में उल्लेख है द्वितीय पंक्ति में उसी क्रम में उपमा है. शन्नो जी से कभी मिलने का सौभग्य नहीं मिला पर युग्म पर उनके सृजन-संसार का सौन्दर्य देख अभिभूत हूँ, सौन्दर्यमयी को हूर ही कहेंगे न? सलिल अर्थात जल-धार कभी स्थिर न रहनेवाली...सदा गतिमय...चंचल और चंचलता ही लंगूर की विशिष्टता है...सो मतिमयी और गतिमय की जोड़ी हूर और लंगूर हुई कि नहीं?...हास्य इसलिए कि जिसे स्नेहीजन 'आचार्य' कहकर सराहते हैं वह तो अपनी औकात जान ले कि वह सिर्फ लंगूर है, कहीं प्रशसा पाकर खुद को कुछ समझने न लगे... यह दोहा खुद मुझे आइना दिखा रहा है...अस्तु. इसे पढ़कर कक्ष का गाम्भीर्य भूल कर ठहाका लगायें यही भाव है इस दोहे के उतरने का...इसे रोकता तो सत्य को सर्व के पास जाने से रोकने का पातक लगता... अतः, तेरा तुझको अर्पण की भावना के साथ...हा..हा..
आचार्य जी
आपकी कक्षा से किसी ने भी पलायन नहीं किया है, बस भोपाल यात्रा पर थी, अभी-अभी ही आयी हूँ। शीघ्र ही अपना होमवर्क पूरा करके आपको प्रस्तुत करूँगी।
नहीं, नहीं 'संजीव' जी, मैं ना कोई हूर
मनु की ही, ही से लगे, मुझसे हुआ कसूर
मुझसे हुआ कसूर, बनाई मेरी गाथा
सोच रही मैं यहाँ, पकडे हाथ में माथा
मिला युग्म का साथ, 'शन्नो' भी लिखती रही
इतनी तारीफ की, मैं तो हूँ काबिल नहीं.
आचार्य जी,
अब आप को शिकायत नहीं होगी कि कक्षा से सब क्यों गोल हो गये. सब लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं. लीजिये मैं फिर परेशान करने आ गयी. आशा है की मनु जी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी मेरे इस दोबारा के आगमन से. आज एक कुंडलिनी भेज चुकी हूँ. एक और भेजे में आ गयी तो वह भी आप देख लीजिये, please.
नेह बिन सूना जीवन, सारा जग निस्सार
दुख बांटे से न बंटे, नेह करे कम भार
नेह करे कम भार, तो बन मेघ सब बरसो
मिले नेह का नीर, न फिर तुम उसको तरसो
शन्नो कहे अधीर, सावन का बन कर मेह
सींच मुरझाया मन, भर दे उसमें कुछ नेह.
आचार्य,
मैंने मजाक किया था,,,,,, ( अब यहाँ पर मजाक किस से करून,,? )
आपने सही कहा के शन्नो जी ने इतनी जल्दी ही जो दोहे में जानकारी हासिल की है वो अपने आप में एक बड़ी बात है,,,,,,,,शुरू में कैसे कहा था के डरते डरते क्लास में झांका है बस,,,,,,
और आज हमारी मोनिटर बना दी गयीं,,,,,,,,,,
नहीं,,,मोनिटर तो बाल उद्यान की हैं,,,यहाँ तो कक्षा-नायिका हैं ,,,
पर हैं विनम्र,,,,इसमें दो राय नहीं,,,,,
और बहुत मेहनती भी,,,
par wo angrej waalaa dohaa samjhaayen,,,,
chaahe aap ,,,chaahe dohaa naayikaa,,,,,
आचार्यजी
एक कुण्डली प्रस्तुत है -
सूरज ढलता देख के, चन्दा ढाँढस देय
दर्पण आँखों में चुभे, बिटिया यौवन देय
बिटिया यौवन देय, समय जब पीछे छूटे
अपने से जज्बात, सरल मन स्रोता फूटे
मावस की हो रात, बने तब बिटिया धीरज
बादल चाहे छाय, निकलता देखो सूरज।
आचार्य जी,
इस दोहे को लिखा पर बाद में मन संतुष्ट नहीं हुआ तो इसकी जरा क़तर-ब्योंत की. अब यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित है आप की दया-दृष्टि के लिये.
मिल बैठें हैं 'सलिल'मनु, दोहा आयें रास
आये थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास
ओटन लगे कपास, यहाँ दोहे की कक्षा
अँधा बैठ सोच रहा, कर ईश्वर रक्षा
डर गयी अब शन्नो, बन बैठे मनु बीरबल
अब खिचड़ी पकेगी, दोनों साथ बैठे मिल.
बहुत सुंदर भाव है आदरणीया पर रचनाओ के शिल्प पर भी ध्यान देना होता है। किसी भी रचना में कथ्य एवं शिल्प का बड़ा महत्व होता है....
पकडे हाथ में माथा ...शिल्प ठीक नहीं।
'शन्नो' भी लिखती रही...लय बाधित
इतनी तारीफ की...11 वीं मात्रा दीर्घ होने से लय भंग, मैं तो हूँ काबिल नहीं.
कुण्डलिया सृजन के लिए जहां तक हो आप दोहे की शुरुआत चौकल से कीजिए...क्योंकि कुण्डलिया का अंत कभी भी द्विकल या त्रिकल से नहीं होता। इसका अंत निम्नरूप में हो सकता है...।।।। / SS /11S
यहां ज्यादतर रचनाओं में दोष दिखाई देता है ..मंच पर आपको या मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
सादर प्रणाम🙏🙏🙏
जी सादर प्रणाम आदरणीय🙏🙏
क्षमा करें...दोहे में कथन साम्य पर विचार करें।
कुण्डलिया छंद विधान:
कुण्डलिया छंदों में हो रही छोटी-छोटी कमियों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ साथी इसके विधान से परिचित नहीं है।
कुण्डलिया छंद एक ऐसा छंद है जो एक दोहा और उसके बाद एक रोला से मिलकर बनता है।
इसके प्रारंभ में एक दोहा अर्थात दो पंक्तियाँ होतीं हैं और उसके बाद एक रोला अर्थात रोला के चार चरण होते हैं। इस तरह एक कुण्डलिया छंद में 6 पंक्तियाँ होतीं है। प्रत्येक पंक्ति को कुण्डलिया का एक चरण कहा जाता है।
कुण्डलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। दो क्रमागत चरण समतुकांत होते हैं।
दोहा के चरणों में दोहा के नियम लगते हैं और रोला के चरणों में रोला के नियम।
दोहा का अन्तिम चरण अर्थात चौथा चरण, रोला के पहले चरण के प्रारंभ में ज्यों का त्यों आता है। उसके आगे 13 मात्राओं के वाक्य खंड को रोला के विधान के अनुसार जोड़कर पहला रोला चरण पूरा करते हैं।
इसके बाद विषय की जरूरत के अनुसार रोला के शेष 3 चरण और लिखते हैं।
रोला चरण के अंत में कम से कम एक दीर्घ (2) या 2 लघु (11) आने अनिवार्य है।
कुण्डलिया के विधान के अनुसार, रोला के अंतिम चरण के अंत में वह शब्द या वाक्यांश आता है जिस शब्द या वाक्यांश से कुण्डलिया छंद (या यों कहें कि दोहा) प्रारंभ हुआ होता है।
यह विधान श्री नारायण दास के "हिंदी छन्दोलक्षण" ग्रंथ के अनुसार है।
रोला:
रोला एक 24 मात्राओं का समपाद सममात्रिक छंद है।
जिसकी मात्राबाँट 8-6-2-6-2 है।
मात्राबाँट हमें यह बताती है कि रोला के किसी चरण में 8-9वीं, 14-15वीं, 16-17वीं और 22-23वीं मात्राएँ सयुंक्त नहीं होनी चाहिए।
इसकी पहली, 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं और 21वीं मात्रा पर न तो कोई शब्द पूरा होना चाहिए। न यहाँ से जगण शब्द शुरू होना चाहिए।
मात्रा मैत्री नियम लगता है अर्थात विषम शब्द के बाद विषम और सम के बाद सम मात्रिक शब्द आना चाहिए। पर दो विषम शब्दों के बीच में जगण आ सकता है।
कुछ लोग अधूरी और सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर कहते हैं कि रोला के अंत में दो दीर्घ होने चाहिए, यह गलत है। रोला चरण के अंत में कम से कम एक दीर्घ (2) या दो लघु (11) आने अनिवार्य है।
दो क्रमागत चरणों में तुक आवश्यक है।
कुछ लोग कहते हैं कि रोला में 9वीं, 10वीं और 11वीं मात्राएं दीर्घ-लघु (21) रूप में ही होनी चाहिए। किंतु विधान के हिसाब से रोला में यह जरूरी नहीं है कि ये तीनों मात्राएँ दीर्घ-लघु (21) रूप में ही हों। ये मात्राएँ 111, 21 या 12 किसी भी रूप में हो सकतीं हैं।
कुछ लोग यह कहते हैं कि रोला की 24 मात्राओं की एक पंक्ति में 11 और 13 मात्राओं के दो चरण होते है, यह बात सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये दोनों खंड दोहा के चरणों की तरह स्वतंत्र होते जो ये नहीं होते हैं। इस तरह के खंडों में 13 मात्राओं का खंड पिछले 11 मात्राओं में खंड से स्वतंत्र नहीं होता है।
कुछ लोग कहते हैं कि रोला में 11वीं मात्रा पर यति जरूरी है। यह भी पूर्णरूपेण सही नहीं है। यह यति 11वीं मात्रा पर भी हो सकती है और वाक्य संरचना के अनुसार इसके आगे भी हो सकती है। हाँ यह बात सच की कुंडलिया में सामान्यता यह यति 11वीं मात्रा पर होती है।
इस विधान पर कवि गिरधर जी तथा अन्य कवियों ने कई सुंदर लययुक्त कुंडलियाँ लिखीं हैं जिनमें 9, 10 और 11वीं मात्राएँ ताल रूप में नहीं हैं, उनके कुछ फोटो संलग्न हैं।
नोट:-
नवोदित साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि कुण्डलिया छन्द लिखने के लिए विधान का अध्ययन कतई जरूरी नहीं है। मेरी सलाह है कि वे कवि गिरधर जी या इस पटल पर चुनी गईं कुण्डलियों को पढ़ें और उनकी लय को ध्यान में रखकर और उसे गुनगुनाकर उसी लय में अपनी रचना लिखें। इस प्रकार लिखी गयीं कुण्डलियाँ अपने आप विधान में आ जाएंगीं
लक्ष्मीकान्त शर्मा 'रुद्र'
उत्तम
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)