आपने हिन्द-युग्म के वर्तमान अतिथि कवि हरे प्रकाश उपाध्याय की पिछली कविता में लोहार, चमार का शाश्वत सच देखा। अगली कविता उसी लुहार की नियति के कारण खोजने की कोशिश है। आप भी पढ़िए-
'लुहार'
लोहे का स्वाद भले न जानते हों
पर लोहे के बारे में
सबसे ज़्यादा जानते हैं लुहार
मसलन लुहार ही जानते हैं
कि लोहे को कब
और कैसे लाल करना चाहिए
और उन पर कितनी चोट करनी चाहिए
वे जनाते हैं
कि किस लोहे में कितना लोहा है
और कौन-सा लोहा
अच्छा रहेगा कुदाल के लिए
और कौन-सा बन्दूक की नाल के लिए
वे जानते हैं कि कितना लगता है लोहा
लगाम के लिए
वे महज़
लोहे के बारे में जानते ही नहीं
लोहे को गढ़ते-सँवारते
ख़ुद लोहे में समा जाते हैं
और इन्तज़ार करते हैं
कि कोई लोहा लोहे को काटकर
उन्हें बाहर निकालेगा
हालाँकि लोहा काटने का गुर वे ही जानते हैं
लोहे को
जब बेचता है लोहे का सौदागर
तो बिक जाते हैं लुहार
और इस भट्टी से उस भट्टी
भटकते रहते हैं!
इनकी कविताओं में वर्तमान खौफ़नाक, खूनी और विभत्स चेहरा लिये ज़िंदा हूँ। यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि चल-फिर रहा है, पूरी अकड़ के साथ। 'ख़बरें छप रही हैं', 'महान आत्माएँ' और 'हम पत्थर हो रहे हैं' में वही सच दात-निपोरे हँस रहा है।
'हम पत्थर हो रहे हैं'
कितने लाख लोग दुनिया के भीख माँग रहे हैं
कितने अपाहिज हो गये हैं मेरी तरह
कितने प्रेमियों के साथ दग़ा हो गया है
बस यही बचा है सुनने-बताने को
मेरी तरह कितने ही लोग
इन ख़बरों में हाय-हाय कर रहे हैं
हाय-हाय की दहला देने वाली चीखें
घुटी-घुटी हैं
न जाने कौन इनका गला घोंट रहा है
मैं सोचता हूँ
निकलूँ और दौड़ू सड़कों पर
अपने तमाम ख़तरों के बावज़ूद
चिल्लाऊँ शोर मचाऊँ
कि पड़े सोये लोगों की नींद में खलल
पृथ्वी की छाती में
कील ठोका जा रहा है
और अज़ीब-सी बात है कि मेरे साथी सब सो रहे हैं
बस चिल्लाने का काम ही मेरे वश में है
जो मैं नहीं कर रहा हूँ
नहीं तो करने को बचा ही क्या है
भरोसाहीन इस दौर में
निराशा की यह घनी शाम
दुख की बूँदा-बाँदी
तुम्हारी यादें
गलीज़ ज़िन्दगी की ऊब
और एक सख़्तजान बुढ़िया की क़ैद
जो उल्लास के हल्के पत्तों के संगीत से भी
चौंक जाती है और चीखने लगती है
इन सबसे बिंधा
कितना असहाय हो रहा हूँ मैं
कहीं कोई भरोसा नहीं
पता नहीं किस भय से काँप रहा हूँ मैं
सारी चिट्ठियाँ अनुत्तरित चली जाती हैं
कहीं से कोई लौटकर नहीं आता
दोस्त मतलबी हो गये हैं
देखो मैं ही अपनी कुंठाओं में
कितना उलझ गया हूँ
संवेदना के सब दरवाज़ों को
उपेक्षा की घुन खाये जा रही हैं
बेकार के हाथ इतने नाराज़ हैं
कि पीठ की उदासी हाँक नहीं सकते
हम लगातार अपरिचित होते जा रहे हैं
हमारे पाँव उन गलियों का रास्ता भूल रहे हैं
जिनमें चलकर वे बढ़े हैं
देखो तुम ही इस गली से गयी
तो कहाँ लौटी फिर!
घास के उन घोंसलों की उदासी तुम भूल गयी
जिन्हें हम अपने उदास दिनों में देखने जाते थे
और लौटते हुए तय करते थे
परिन्दों की गरमाहट लौटाएँगे
किसी-न-किसी दिन इन घोंसलों को
देखो हम किस क़दर भूले सब कुछ
कि ख़ुद को ही भूल गये
हमें प्यास लगी है
और हमें कुएँ की याद नहीं
हम एक पत्थर की ओर बढ़ रहे हैं
पूरी बेचैनी के साथ..........।
और पूरी बेचैनी से इंतज़ार कीजिए आगामी रचनाओं का॰॰॰




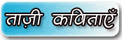




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
2 कविताप्रेमियों का कहना है :
शैलेश जी,
इंसान को लोहे में बदल कर फिर ढाल देना पत्थर में, दिल को छू जाता है.
निम्न पंक्तियों में यह बात प्रभावित करती है कि आज की मारा-मारी भरे दौर में हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा को ही भूल जाते है जैसे कि कोई मृग कस्तूरी को अपने से अलग अन्यत्र तलाशता फिरता है :-
वे महज़
लोहे के बारे में जानते ही नहीं
लोहे को गढ़ते-सँवारते
ख़ुद लोहे में समा जाते हैं
और इन्तज़ार करते हैं
कि कोई लोहा लोहे को काटकर
उन्हें बाहर निकालेगा
हालाँकि लोहा काटने का गुर वे ही जानते हैं
और इन पंक्तियों में तो बात सीधे दिल में उतर जाती है कि कस्तूरी को तलाशता मृग किसी मरीचिका में भटक जाता है :-
हमें प्यास लगी है
और हमें कुएँ की याद नहीं
हम एक पत्थर की ओर बढ़ रहे हैं
पूरी बेचैनी के साथ..........।
बहुत अच्छी कविताओं के लिये बधाईयाँ.
मुकेश कुमार तिवारी
लोहे के बारे में
सब कुछ जानते हुए भी
लुहार कभी नहीं हो पाते
लौह पुरुष...
हम पत्थर हो रहे हैं...
यह भ्रम है हमें
पत्थर होते तो
टूटने तक
चोट तो सहते...
अच्छी रचनाये...
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)