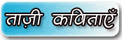काव्य-पल्लवन सामूहिक कविता-लेखन (विशेषांक)
विषय - पहली कविता
अंक - अट्ठाइस (भाग-२)
माह - जुलाई २००९
हमारे पाठकों की
पहली कविताओं की दूसरी पारी की शुरुआत पिछले अंक से हो चुकी है। ये कवितायें कुछ खास हैं, इनमें अपरिपक्वता भी नजर आयेगी, बचपना भी होगा। ये उन कविताओं में से भी नहीं होंगी जिन पर लोग वाह-वाह कर सकें, जिन पर गीत रचे जा सकें, और हो सकता है सम्मेलनों में सुनाई भी न जा सकें। लेकिन फिर भी इनका विशेष महत्व है। क्योंकि ये उन सभी कविताओं की जननी हैं। ये पहली सीढ़ी होती है। ऐसी ही २० सीढ़ियों को लेकर हम हाजिर हैं।
जैसे-जैसे हमें और कवितायें मिलती जायेंगी, हम 20-20 कविताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। हमारे पाठकों ने हमें भूमिका भी लिख भेजी है जिसे हम कविता के साथ ही प्रकाशित कर रहे हैं। अलग अलग अनुभवों पर लिखी गईं वो चंद पंक्तियाँ आज हमारे इस मंच का हिस्सा बन रही हैं। हम आशा करते हैं इससे हमारे अन्य पाठकों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे हमें कविता लिख भेजेंगे। चलिये पढ़ते हैं 20 कवियों की पहली कवितायें।
हमें आप अपनी "पहली कविता" kavyapallavan@gmail.com पर भेज सकते हैं।
आपको हमारा यह आयोजन कैसा लग रहा है और आप इसमें किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं, कॄपया हमें ईमेल के जरिये जरूर बतायें। अपने विचार ज़रूर लिखें
बहुत अच्छा लग रहा है अपनी पहली कविता आपके साथ बाँटने में. दुनिया को भी पता चलेगा. तो शुरू करता हूँ उस पल का सफ़र जब यह पहली कविता मेरे जेहन में आई थी.
1993 या 1994 कि बात है. शायद तब मैं क्लास 6th या 7th में रहा होऊँगा. एक रोज़ घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था और घर के सामने लगे अशोक के पेड़ को देखते हुए बस येही सोच रहा था कि अगर मैं अभी इस पेड़ को काट दूं या कोई चीज़ इस पर मार दूं तो यह अपने दर्द के बारे में बोल भी नहीं सकता. टीवी पर पेड़ बचाओ कि काफी विज्ञापन देख चुका था. टीवी और दूरदर्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे तब. तो बैठे बैठे कहाँ से तुकबंदी बैठानी शुरू कर दी और यों बन गयी मेरी पहली कविता. जब मम्मी को सुनाई तो उन्होंने कागज़ पर उतार दी और तब से लेकर अब तक उन्होंने मेरी बचपन कि साड़ी कवितायें संभाल कर रखीं हैं. तो अपनी पहली कविता आप सबके सामने पेश करता हूँ जिसका शीर्षक है "पेड़".
पेड़पेड़ एक बेजुबान चीज़ आशियाना है,
जो है उसका दुश्मन वह ज़माना है,
अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहेंगे,
अगर इसी तरह से पेड़ मरते रहेंगे,
तो एक दिन ऐसा भी आएगा
जब सूरज कि कड़ी किरणों में
चलते चलते हम औंधे मुँह गिरेंगे.
तो पेडों को काटने से रोको,
इस तरह पेडों को लालच कि आग में मत झोकों!!
--गौरव शर्मा 'लम्स’
माँ तो माँ होती है,क्या कहूँ क्या सोचकर लिखा , बस जो लिखा मन से लिखा , प्रभु के निकट एक दीप जलाया ....
माँ इस दुनिया में माँ का रिश्ता
है अपने बच्चो से ऐसा
जैसा रिश्ता होता जड़ों का
अपने प्रिय पेड़ो के संग
हर सुख से प्यारे लगते हैं
अपने बच्चे
सारी दुनिया में लगते हैं वे ही अच्छे|
तभी तो माँ के दिल से निकले
आशीर्वाद ,
होते है मोती से सच्चे|
नहीं हो सकते सर्वत्र विराजमान खुदा
तभी करुणा में डूबकर माँ को बनाया|
यू ही नहीं माँ ने भगवान के बाद
दूसरा स्थान पाया |
पाया जिसने माँ का प्यार
हो गया वह धन्य-धन्य
--विनीता श्रीवास्तव 
सिमटना यूँ अपनेआप में...
मुझे रास न आया कभी....
मै तो उन्मुक्त गगन में ...
सीमाओं के बंधन से मुक्त हों...
सोच के पंखो को फैला के...
दूर दूर तक उड़ते रहना चाहती हूँ...
धरती पे मेरे अहसासों का समंदर बड़ा गहरा है..
अक्सर उसमे गोते लगाती हूँ..
.कभी खुद डूबती हूँ
तो कभी अपने आप को डुबोती हूँ...
अहसासों की लहरे बड़ी तीव्र होती है...
टकरा टकरा के और ज्यादा तेज हों जाती है...
अपने किनारे को तलाशने में रात दिन उछलती रहती है..
अहसासों के इस टकराव से अक्सर
तन् और मन् घर्षित हों जाते है...
"मन रूपी सागर" में उठनेवाली
"भावना रूपी लहरों" को
"शब्द रूपी किनारा" न दिया जाए तो ये
"तन् रूपी चट्टानों" से टकरा टकरा के घर्षित हों जायेगी...!!!!!!
इन लहरों को किनारा देने का मेरा ये एक प्रयास................
चंचल से इस मन् की बाते
कितनी उलझी-सुलझी ...
कभी लगे मानो जग अपना
तो कभी सब से बेरुखी सी !
खुद से जवाब पूछे ये और
देता उत्तर खुद से ही
न मिले संतुष्टि उत्तर से तो
नाराजगी भी खुद से ही !!
भ्रम जाल में उलझा ये जीवन,
पार पाना है खुद से ही...
मिलेंगे साथी यहाँ बहुतेरे लेकिन
उलझन सुलझेगी खुद से ही!!!
--कविता
माई मेरी पहली कविता है.. 1995 मे मैने इसे लिखा . जून 1997 मे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के मासिक मुख पत्र भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका मे यह कविता छपी और फिर भोजपुरी मे जो लिखने का सिलसिला शुरु हुआ .आज तक जारी है. हां यह सच है कि इसके पहले हिन्दी मे मैने कुछ तुकबंदी की थी या यूं कहे कि चिचरी पारने की कोशिश की थी पर उन कविताओँ का अब कोई अता- पता नहीँ है..
माईअबो जे कबो छूटे लोर आंखिन से
बबुआ के ढॉंढ़स बंधावेले माई
आवे ना ऑंखिन में जब नींद हमरा त
सपनो में लोरी सुनावेले माई
बाबूजी दउड़ेनी जब मारे-पीटे त
अंचरा में अपना लुकावेले माई
छोड़ी ना, बबुआ के मन ठीक नइखे
झूठहूं बहाना बनावेले माई
ऑंखिन का सोझा से जब दूर होनी त
हमरे फिकिर में गोता जाले माई
आंखिन का आगा लवटि के जब आई त
हमरा के देखते धधा जाले माई
अंगना से दुअरा आ दुअरा से अंगना ले,
बबुआ का पाछे ही धावेले माई
किलकारी मारत, चुटकी बजावत,
करि के इशारा बोलावेले माई
हलरावे, दुलरावे, पुचकारे प्यार से
बंहियन में झुला झुलावेले माई
अंगुरी धराई, चले के सिखावत
जिनिगी के ´क-ख´ पढ़ावेले माई
गोदी से ठुमकि-ठुमकि जब भागी त
पकडि के तेल लगावेले माई
मउनी बनी अउर “भुंइया लोटाई त
प्यार के थप्पड़ देखावेले माई
पास-पड़ोस से आवे जो ओरहन
काने कनइठी लगावेले माई
बाकी तुरन्ते लगाई के छाती से
बबुआ के अमरित पियावेले माई
जरको सा लोरवा ढरकि जाला अंखिया से
देके मिठाई पोल्हावेले माई
चन्दा ममा के बोला के, कटोरी में
दूध- भात गुट-गुट खियावेले माई
बबुआ का जाड़ा में ठण्डी ना लागे
तापेले बोरसी, तपावेले माई
गरमी में बबुआ के छूटे पसेना त
अंचरा के बेनिया डोलावेले माई
मड़ई में “भुंइया “भींजत देख बबुआ के
अपने “भींजे, ना भिंजावेले माई
कवनो डइनिया के टोना ना लागे
धागा करियवा पेन्हावेले माई
“भेजे में जब कबो देर होला चिट्ठी त
पंडित से पतरा देखावेले माई
रोवेले रात “भर, सूते ना चैन से
भोरे भोरे कउवा उचरावेले माई
जिनिगी के अपना ऊ जिनिगी ना बूझेले
´बबुए नू जिनिगी ह´ बोलेले माई
दुख खाली हमरे ऊ सह नाहीं पावेले
दुनिया के सब दुख ढो लेले माई
´जिनिगी के दीया´ आ ´ऑंखिन के पुतरी´
´बुढ़ापा के लाठी´ बतावेले माई
´हमरो उमिरिया मिले हमरा बबुआ के´
देवता-पितर गोहरावेले माई
--मनोज भावुक
विश्व पिता दिवस पर मैंने पापा को पिता पर कविता लिखते देखा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहें हैं यह सुनकर वे बोले कि तुम्हारे बाबाजी पर कविता लिख रहा हूँ | मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आप पर कविता लिखूं ? तो पापा नें कहा हाँ लिख लो तो मैंने यह कविता लिखी और पापा को दिखाई तो पापा ने कहा कुछ ठीक है खैर अब तुम कविता लिखने लगोगे |
पापापापा बहुत अच्छे ...
मुझे बहुत प्यार करते ....
जब भी मैं गलती करता ....
वे मुझको डांट भी देते ....
और तो और ...
मेरा छोटा भाई....
जब शैतानी करता .....
तो पापा साथ-साथ.....
मुझको भी डांटते हैं ....
मेरे पापा.....
मेरे साथ खूब खेलते हैं .....
मेरे पापा ....
हर कठिन घड़ी में ....
मुझको....
हिम्मत बंधाते हैं ....
मैं अपने पापा का .....
खूब रखता ख्याल .....
और करता .....
उनको बहुत प्यार ......
--नील श्रीवास्तव 
यह कविता उस समय लिखी जब मैं बी ए कर रही थी| अचानक चलते चलते एक दोस्त बना और दोस्ती बहुत गहरी हो गई ,तब अनायास ही ये पंक्तियाँ कविता बन गई ,आज भी वह मेरा अच्छा दोस्त है |मैंने इन पंक्तियों को उसी रूप में संजों कर याद के रूप में रक्खा है |
मिल जाते हैं मीत कभी पथ चलते चलते
चौराहे पर मिलने वाले मीत नहीं होते ,
हर हंसने वाले चहरे पर आकर्षण है
किन्तु नहीं प्रत्येक हंसी में अपनापन है
नहीं ठहरती नज़र कहीं भी किसी रूप पर ,
कहीं अटक जाता वैरागी मन है ,
मंजिल मिलती नहीं शाम तक चलते-चलते ,
कभी काम मिलता शाम के ढलते -ढलते |
चौराहे का मीत न हो ,पथ साथ निभा दे जीवन भर ,
इच्छाओं के कंधे पर अरमान संजोये बैठे हैं ,
जो मिल जाते हैं राह चले वह साथ निभा पते हैं ,
जीवन के इस धूप छाँव को खेल कहाँ हम पाते है |
मीत बिना मन वैरागी हो ,तो प्रीत कहाँ कर पाते हैं ,
अरमानों की लाशों पर प्रेम नहीं कर पाते हैं |
बिखरे हुए जीवन में ,प्यार के गीत नहीं होते ,
चौराहे पर मिलने वाले मीत नहीं होते ||
इस कविता में कुछ त्रुटियां अब दिखाई देती है पर मेंने कुछ भी संशोधन नहीं किया |
--करूणा पाण्डे
उन दिनों की बात है जब में बारवीं का इम्तहान दे रही थी. एक दिन दोपहर की पारी में इम्तहान था.मैं और मेरी बहिन पढ़ रहे थे बीच-बीच में एग्जामनर को कोस भी रहे थे कि पता नही कैसा पेपर आयेगा. तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खयाल कौंधा. और वो मेने पेपर पर लिख दिया.बाल मन की जो भी भावनायें थीं सब काग़ज पर उड़ेल दीं. हो सकता है उस समय ये एक तुकबंदी हो या फिर कविता की दिशा में मेरा पहला कदम. लिखने के बाद घर में सबको सुनायी तो सभी ने उत्साह वर्धन किया. हालांकि यह कविता पूर्ण रूप से मुझे याद नहीं है कुछ लाइने ही जह़न में हैं वही लिख भेज रही हूँ. साथ में उसके बाद जो दूसरी कविता लिखी थी वो भी भेज रही हूँ आपको जो उचित लगे छाप दीजियेगा. दूसरी कविता लिखने का कारण यह था की हमारे पड़ोसी अक्सर हमसे सिलेण्डर ले जाते थे लेकिन जब हमें जरूरत होती तो हमें ना कह दिया जाता. ऐसे में एक दिन अचानक ही मेरे मुँह से ये शब्द निकल पड़े और कविता का रूप बन गये वही लिख भेज रही हूँ.
है प्रभु तेरी माया(प्रथम)
है प्रभु तेरी माया
ये पेपर किसने बनाया
तू उसे अक्ल तो देता
कि वो ऐसा पेपर ना देता
उसने ऐसा पेपर दिया
बच्चों का साल ख़राब किया
पछताया तो होगा वो भी
बच्चों की बददुआ लगेगी
लेकिन अब देर हो गयी बहुत
समय से उसे क्यों नहीं चेताया
हे प्रभु तेरी माया
--दीपाली पन्त तिवारी"दिशा"
पहली कविता. जैसे ही ये दो शब्द पढ़े , मुझे अपनी एक बहुत पहले लिखी कविता याद आ गई. मै ठीक से तो नहीं कह सकता यह कविता मैंने कब लिखी किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूँ की यह मेरे कालेज के दिनों की कविता है. उन दिनों मै मंदसोर के कालेज के B.Sc. प्रथम वर्ष का छात्र था. बात शायद १९७३-७४ की होगी. मै अपने घर की छत पर शाम के समय अकेला टहल रहा था , आसमान में सूरज के डूबने के वक्त की लालिमा छाई हुई थी. धीरे धीरे हल्का हल्का सा अंधकार हो चल था ओर चाँद एक हंसिये के आकार में दिखाई देने लगा था. आसमान में सूरज के अस्त होनें पर छाने वाली लाली ओर चाँद के हंसिये नुमा आकार ने मेरे मन में जिन विचारो को जन्म दिया वे जब शब्द के रूप में कागज पर उभरे तो जो कविता सामने आई वही कविता आज मै आप के सामने रख रहा हूँ.
सूरज , चाँद और तारे
आसमान में अभी अभी
हो गया खून सूर्य का
देखो चारों तरफ खूनी लाली
छा गई है
सितारों की पुलिस सारे गगन पर छा गई है ,
थोडी देर में पकड़ लिया गया
खूनी को , खूनी था चाँद
रात की अदालत में , कुछ तारों की वकालत में
सजा दे दी गई , चाँद को
रात भर ठण्ड में ठिठुरना होगा ,
और
हर सुबह दुनिया के जिन्दा होते ही
तुझे मरना होगा
--विद्यासागर 
यह मेरी पहली कविता है जो पहले सिर्फ एक पंक्ति थी "इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे" मुझे किसी ने कहा की यह बहुत अच्छी पंक्ति है | फिर मैंने इसे कविता में बदलने की कोशिश की |
इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे,
इनती खुशियाँ भी न देना, दुःख पे किसी के हंसी आने लगे ।
नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर उपयोग करूँ,
नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी को देख जल-जल मरूँ ।
ऐसा ज्ञान मुझे न देना अभिमान जिसका होने लगे,
ऐसी चतुराई भी न देना लोगों को जो छलने लगे ।
इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे ।
इतनी भाषाएँ मुझे न सिखाओ मातृभाषा भूल जाऊं,
ऐसा नाम कभी न देना कि पंकज कौन है भूल जाऊं ।
इतनी प्रसिद्धि न देना मुझको लोग पराये लगने लगे,
ऐसी माया कभी न देना अंतरचक्षु भ्रमित होने लगे ।
इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे ।
ऐसा भग्वन कभी न हो मेरा कोई प्रतिद्वंदी हो,
न मैं कभी प्रतिद्वंदी बनूँ, न हार हो न जीत हो।
ऐसा भूल से भी न हो, परिणाम की इच्छा होने लगे,
कर्म सिर्फ करता रहूँ पर कर्ता का भाव न आने लगे ।
इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे ।
ज्ञानी रावण को नमन, शक्तिशाली रावण को नमन,
तपस्वी रावण को स्विकारू, प्रतिभाशाली रावण को स्विकारू ।
पर ज्ञान-शक्ति की मूरत पर, अभिमान का लेपन न हो,
स्वांग का भगवा न हो, द्वेष की आँधी न हो, भ्रम का छाया न हो,
रावण स्वयम् का शत्रु बना, जब अभिमान जागने लगे ।
इतनी ऊँचाई न देना ईश्वर कि धरती पराई लगने लगे ।
--प्रकाश पंकज 
इस रचना का जन्म तब हुआ जब मैं 1971 में बी.ए.पार्ट 1 में थी. सोचा करती थी की लोग कविताएँ कैसे लिख लेते हैं? अपने भावों को अभिव्यक्ति कैसे देते हैं? मेरी एक सीनियर थीं प्रतिभा वो बहुत अच्छी हिन्दी की कविताएँ लिखतीं थीं...उन्होने कहा की अपने आस - पास देखो...जो तुमको आकर्षित करे उस पर कुच्छ लिखने का विचार करो...तो एक दिन कॉलेज के बगीचे में बैठी थी कि एक गुलाब के पौधे पर नज़र गयी ..उसका एक फूल मुरझा कर गिर रहा था और एक नयी कली खिल रही थी....उसको देख जो विचार मॅन में आया वो मेरी पहली कविता के रूप में आप सबके साथ बाँटना चाहती हूँ....
राज़ फूल ने कली से मुस्कुरा कर कहा
तेरे पर भी बहार आएगी
तू भी फूल बनते - बनते
यूँ ही बिखर जाएगी
पर कली ने उस बात का
वह राज़ ना जाना
उसकी इस बात को
ज़रा सच ना माना
पर आया जब वक़्त तो
वह फूल बन गयी
मस्ती से भरी कली
यूँ ही बिखर गयी
अपने हालात पर वो
काफ़ी दुखी थी
कहती है फूल से-
मुझे माफ़ करो
मैं तुम पर
यूँ ही हँसी थी.
24-07-1971
--संगीता स्वरूप
कविता सन १९९८ में लिखी गई थी जब मैं कॉलेज का छात्र था | ये कविता मैंने अपने गृहनगर बागली में लिखी थी जो मध्यप्रदेश के देवास जिले की एक तहसील है |
क्यों लिखी थी ये तो कविता पढ़ कर ही ज़ाहिर हो जाता है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी बता देता हूँ | वाक़या ये था कि हमें प्रेम हो गया था और इस हद तक हुआ कि उसने हमें कवि बना दिया |
कविता प्रस्तुत है -
मन चाहता है तुम्हें देखता ही रहूँ
तब तक
जब तक कि
इन आँखों की ज्योति न बुझ जाए
पलक झपकने का अंतराल भी
मुझे स्वीकार नहीं
मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ
तब तक
जब तक कि
मेरी आँखें तृप्त न हो जाएँ
और मैं जानता हूँ
ये कभी तृप्त न होंगी
ये जितना तुम्हें देखेंगी
उतनी ही और व्याकुल होंगी
तुम्हें देखने के लिए
अनंत काल तक
अनवरत...
--अनिरुद्ध शर्मा 
यह मेरी पहली कविता है जिसे मैंने दिसम्बर 2007 में लिखा था. यह मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी थी जो हिन्दू थी और मुझसे चार साल बड़ी थी. इस बात को लेकर मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते थे, खास तौर तौर पर रेहान. वह कहता था यह कोई प्यार नहीं है बल्कि आकर्षण है और तू उसे कुछ ही महीने में भूल जायेगा. लेकिन मुझे लगता था कि मानो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सारी ज़िन्दगी उसे याद रख सकूँ. इसी दरम्यान मैंने एक कविता लिखी थी जो मेरे और मेरी प्रेमिका के इर्द गिर्द घूमती थी. हालाँकि यह कविता मैंने बस ऐसे ही लिखी थी. लेकिन इस के बाद कविता लिखना मेरा शौक़ बन गया. वैसे तो वह एक साल बाद मेरी ज़िन्दगी से चली गई लेकिन मुझे कविता लिखना सिखा गई.
"एक दुनिया बसा ली है"दिल के कमरे में बैठ कर
प्यार का स्वेटर बुनते हुए
जब तुम्हारी तस्वीर उभर आती है
कुछ यूँ अतीत के आसमान से गिर
तुम्हारी यादों की फुहार
मुझे भिगो जाती है.
यह एक सच है कि
मज़हब की दीवार पिघल के
मुहब्बत के सांचे में न ढल पाई
कभी तुम मजबूर हुईं रस्मो रिवाज को लेकर
कभी मैं मजबूर हुआ इस समाज को लेकर
यह एक सच है कि
मैं और तुम हम नहीं बन पाए
मगर यह भी एक सच है
कि अब तूने भी एक दुनिया बसा ली है
कि मैंने भी एक दुनिया बसा ली है.
--शामिख फ़राज़
ग़ज़ल मैंने १२ साल की उम्र में लिखी थी.जब मुझे पता भी नहीं था की ग़ज़ल क्या होती है. स्कूल की एक प्रतियोगिता के दौरान पहला इनाम न मिलने पर मायूसी के शब्द कागज़ पर कुछ इस तरह उतरे.
हरदम वही बस चाहा,जो मेरे मुकद्दर में नहीं,
अपनी तो हर ख्वाइश से रही शिकायत ही मुझे
चाहा होता गर ,जो तकदीर में है वही
शायद ये खुदा कुछ तवज्जो दे देता मुझे.
आंसूं की लहरों से उबर कर साहिल पर आई जो कभी,
जहाँ ने फिर डुबो दिया गमें सागर में मुझे.
सोचती हूँ बैठकर कितनी गमजदा है जिन्दगी,
ख्याल कर दूजों का सब्र होता है मुझे.
क्या मांगूं खुदा जो देना चाहे अगर,
ग़मों का सागर लगती है दुनिया ही मुझे
चाहत की है काश कुछ बनू जिन्दगी मैं,
वेसे तो अपनी हर तमन्ना से शिकायत है मुझे
--शिखा वार्श्नेय
हमेशा से बहुत संवेदन-शील थी , पचास साल की उम्र में अचानक कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया |
पहली कविता यही थी , 'पहली कविता , जैसे कोई सीख '
रे मन
तू क्यों भूल गया
हर ओर उसी की छाया है
हर ओर उसी का आनँद है
आशाओं ने हैं जाल बुने
निराशा के भँवर में फँसाया है
अन्धकार में मन भरमाया है
रे मन , तू क्यों भूल गया
सौगातें तुझे बिन माँगे मिलीं
उपलब्धियों से तेरी झोली भरी
पर तुझे सदा खाली ही दिखी
रे मन , तू क्यों भूल गया
सीमाओं को न आड़ बना
निर्मल मन से देना सीख जरा
इसमें भी मैं , उसमें भी मैं , इसमें भी वो , उसमें भी वो
रे मन , तू क्यों भूल गया
--शारदा अरोड़ा
स्कूल के जमाने से ही कुछ न कुछ लिख्नने की कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन पहली गजल कालेज के दिनो मे ही पूरा हो सका। प्रस्तुत गजल १९९३ मे लिखी गयी है।
अब तो जीने क ये अन्दाज बना रखा है
बह्ते अश्को को भी पल्को पे सजा रखा है।
गिर के आँखों से टपक जाये कहीं न मोती
चश्मे पूर्णम मे वो एक राज छुपा रखा है।
जिन्दगी ख्वाबे परेशा के सिवा कुछ भी नही
नामुरादी के सिवा दहर मे क्या रखा है।
शामे गम ने मेरे कानो मे ये चुपके से कहा
पर्दा ए शब ने तेरा ख्वाब छुपा रखा है।
रस्म ए दुन्या है हमे शिक्वा गीला क्या करना
सम्झे वो जिस ने के आलम ये बना रखा है।
छेड मेरे दिल ए मजरुह् को न अब अख्तर
ये है शोला जो शरारो को दबा रखा है।
--शाहनवाज अख्तर
ये कविता जब लिखी तो करीब ११-१२ साल की थी. उन दिनों दूरदर्शन पर भगवान् के सीरियल बहुत आते थे. सीरियल ख़त्म हो जाने के बाद भी राक्षसों और देवताओं के बारे में सोचा करती. कल्पना करना मेरे पसंदीदा कार्यो में से एक था....ईश्वर के बारे में सोचती...... संसार के बारे में सोचती........ पता नहीं अपने नन्हे से दिमाग में उन दिनों इतना बोझ ले कैसे मस्त रहती थी. ईश्वर ने इस स्रष्टि का सर्जन किया ,पर क्या कोई भी सृजन बिना कल्पना के सम्भव हैं । अगर नही ........ तो स्रष्टि निर्माण के पूर्व विधाता ने एक योजनाबद्ध कल्पना कर दुनिया कि रूपरेखा तैयार की होगी । संभवतः यही हुआ होगा ..........और वैसे भी हम अगर गौर करे तो रोजमर्रा की जिन्दगी में भी तो कार्य को किर्यान्वित करने के पूर्व हम कल्पना ही तो करते हैं. बचपन में मैंने ये कविता लिखी थी ...... सोचा तो कुछ ऐसा ही था पर उन दिनों सोंच इतनी परिपक्व नही थी ...........खैर अब प्रस्तुत हैं मेरी रचना "कल्पना"
कल्पनाकल्पना तू क्या हैं, क्या तू एक सपना हैं,
नहीं तू सपना नहीं, वास्तविकता हैं जीवन की ,
अडिग हैं विश्व का ये भार , तुझ पर ही निर्भर समस्त ब्रह्माण्ड ,
पर तुझे न समझ पाया ये मनुष्य ,
यदि तू न होती, तो ये स्रष्टि नहीं होती,
ये स्रष्टि नहीं होती ,तो मनुष्य नहीं होता,
मनुष्य नहीं होता , तो तू कैसे जीवित रहती,
और आज मेरी कलम तेरे बारे में न लिखती !!
जानती हूँ इतनी छोटी सी रचना का विश्लेषण लम्बा दिया हैं........ पर ये हैं भी तो बालमन की उपलब्धि ........... उम्मीद हैं आप इसे पसंद करेगे ---------------
--प्रिया चित्रांशी
रात के लगभग बारह बज रहे थे,दिल्ली दूरदर्शन पर फ्रांस में हुए हिंदी सम्मलेन का प्रसारण चल रहा था,गुलजार साब का नंबर आया ओर उन्होंने कुछ ऐसी नज्म पढ़ी ''मेरे घर में अब कोई नहीं रहता''यह नज्म मेरे दिल तक पहुंची और मेरी आँखें नाम हो गयी!
प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद लगभग १ बजे मैंने कलम और पन्ने की मदद से जो शब्द लिखे बह आप सब के सामने है!
यह मेरी पहली कविता है और शायद ऐसी कविता फिर कभी मैं अपनी जिंदगी मे लिख भी ना पाऊँ!
यह कविता देनिक भास्कर के रसरंग में प्रकाशित हो चुकी है!
बह मुझे माँ कहता है
वह मुझे मां कहता है।
वह अब भी मुझे मां कहता है।
सताता हैं रुलाता है
कभी कभी हाथ उठाता है पर
है वह मुझे मां कहता है।
मेरी बहू भी मुझे मां कहती हैं
उस सीढ़ी को देखो,मेरे पैर के
इस जख्म को देखो,
मेरी बहू मुझे
उस सीढ़ी से अक्सर गिराती है।
पर हाँ,वह मुझे मां कहती है।
मेरा छोटू भी बढिया हैं,जो मुझको
दादी मां कहता है,
सिखाया था ,कभी मां कहना उसको
अब वह मुझे डायन कहता हैं
पर हाँ
कभी कभी गलती सें
वह अब भी मुझे मां कहता है।
मेरी गुड़िया रानी भी हैं ,जो मुझको
दादी मां कहती है
हो गई हैं अब कुछ समझदार
इसलिए बुढ़िया कहती हैं,
लेकिन हाँ
वह अब भी मुझे मां कहती है।
यही हैं मेरा छोटा सा संसार
जो रोज गिराता हैं
मेरे आंसू ,
रोज रुलाता हैं खून के आंसू
पर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वे सभी
मुझे मां कहते है।
--संजय सेन सागर
ये कविता मैने 2003 मे लिखी थी मगर सिर्फ़ सॅंजो कर रखी हुई थी
क्यो पहचान कही बिखर गये मेरे
हर गुमान आज बिखर गये मेरे
हक़ीकत से जब वास्ता हुआ
हर ख्वाब बिखर गये मेरे
दर्द से बाहर निकले ही थे की
नये दर्द फिर से सवर गये मेरे
अब तो दस्त की लकीरो से भी उठ गया भरोसा
की ज़िंदगी के हर ख़याल बिखर गये मेरे
ज़िंदगी गनीमत सलामत है मेरी
वरना लगता था ज़िंदगी के सब सवाल
बिखर गये मेरे
और आज बहुत दर्द से गुज़री है “शबा”
गैरो की तरह सारे अपने बिछड़ गये मेरे
(दस्त-हाथ)
--रज़िया शबा खान
यह मेरी पहली कविता थी।जो स्थानीय समाचार पत्र ‘राष्ट्रविचार’ में 11।7।1996 में प्रकाशित हुई थी।
प्रश्नप्रश्न से प्रारंभ
प्रश्न ने प्रश्न किया
प्रश्न चुप रहा
शांत रहा
प्रश्न प्रतिदान न कर सका
प्रश्न असर्मथ असहाय रहा
प्रश्न बनकर
--मंजु गुप्ता
मैं आमोद कुमार श्रीवास्तव परिवार में सबसे छोटा वाराणसी जन्म स्थान तथा हाईस्कूल तक वहीं पढ़ाई इसके पश्चात बलिया से ईण्टर जौनपुर से ग्रेजुएशन। फिलहाल मेरठ कर्मभूमि है । निम्न कविता मेनें तब लिखी जब में सुबह आठ बजे से लेकर सायं 5 बजे तक शुगर मिल की नौकरी करने के पश्चात सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कम्प्युटर पढ़ने मेरठ बस से जाया करता था इसमें मेनें जो महसूस किया वही लिखा है आशा करता हूँ कि आप को पसन्द आएगा।
थकान दिमाग इतनी थकान के बाद
एक कप चाय मॉंगता है
ऑंखे ऑंसू पोछने के लिए रूमाल
पेट मॉंगता है रोटी
और कैसी भी सब्ज़ी
शरीर कहता है ले आना च्यवनप्राश
एक ग्लास दूध के साथ
और तो और
हाथ पैर भी बंद कर देते हैं
थक कर काम करना
क्हते हैं ला दो 600 एमजी की ब्रुफेन
सभी कुछ न कुछ मॉंगते हैं
मैं पूछता हूँ क्या मॉंगू इस जमाने से
दौलतमंद को सोना
हत्यारों को हथियार
बीमारों को बीमारी
कमजोरों को निर्बलता
अन्यायी को सत्ता
कहॉं से आयी इतनी बात
पैदा करो जज्बात
कि मैं और तुम दोनों
हंस सके बिना कुछ
मॉंगे हुए मॉंगे हुए
--आमोद कुमार श्रीवास्तव