कवि सत्यप्रसन्न समकालीन बोध की छांदस कविताएँ लिखते हैं। आज हम उनकी जो कविता प्रकाशित कर रहे हैं, उसने फरवरी माह की प्रतियोगिता में दसवाँ स्थान बनाया और थोड़ा बहुत तुक की तरफ झुकाव भी है।
पुरस्कृत कविताः जी चुका हूँ मैं
शिथिल नहीं हुईं पेशियाँ,
नासिका रंध्रों की
अभी तक।
पहचान ही लेती हैं वे;
देह गंध तुम्हारी
अभी भी।
मंद नही हुई है तनिक भी;
श्रवण शक्ति
अभी तक;
सुन ही लेते हैं कान,
ख़नक तुम्हारी चूड़ियों की
अभी भी।
दृष्टि में भी दम-खम
इतना तो बाकी है
अभी तक;
कि दिख ही जाती है,
तुम्हारे माथे पर
बार- बार झुक आती वो
एक लट चाँदी की,
जिसे जब तब हटाने की
अपनी नाकाम कोशिश में,
लगा बैठती हो;माथे पर
बेसन या आटा
अभी भी।
स्पर्श की संवेदना भी;
महफ़ूज़ है अभी तक;
कि; काँपतें हैं ओंठ मेरे
अल सुबह
तुम्हारी तर्जनी के
प्रथम हस्ताक्षर से
अभी भी।
लरज़ते नहीं हैं पाँव;
उठ ही जाते हैं,
दृढ़ता से
लेकर सहारा तुम्हारे कंधे का
अभी तक।
और चढ़ जाते हैं सीढ़ियाँ
देवालय की;
करने साक्षात्कार ईश्वर से;
रोज शाम,
अभी भी।
इसीलिये तो जिंदा है
चहल क़दमी साँसों की
अभी तक,
वर्ना जीने भर के लिये तो;
कब का जी चुका हूँ मैं।
पुरस्कार- विचार और संस्कृति की मासिक पत्रिका 'समयांतर' की ओर से पुस्तक/पुस्तकें।




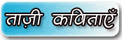




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
3 कविताप्रेमियों का कहना है :
आपकी रचना पढने के बाद अनायास किसी का ये शेर याद आ गया ...
किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी
मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी .
जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब कुछ छोटे छोटे महीन पल ही जिंदा होने का एहसास दिलाते रहते हैं , वर्ना शेष सब धुंधला होता चला जाता है
सत्यप्रसन्न जी तो अपनी कविताओं के जरिये भावनाओं को घनीभूत करने मे उस्ताद हैं ही..आपकी यह कविता तेजी से भागते वक्त के साथ बदलती हुई हर चीज के बीच भी कुछ अमूर्त चीजों के वैसे-का-वैसा रहने की आश्वस्ति की तरह प्रतीत होती है..प्रातःकाल की मुक्त श्वास की तरह..जो पूरे दिन आश्वस्ति की तरह फ़ेफ़ड़े मे अटकी रहती है..
इसीलिये तो जिंदा है
चहल क़दमी साँसों की
अभी तक,
वर्ना जीने भर के लिये तो;
कब का जी चुका हूँ मैं।
सच ही कहा आपने सुंदर रचना है..............
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)