पिछले कुछ दिनों में हरेप्रकाश उपाध्याय, अंजना बख्शी, रामजी यादव और मुहम्मद अहसन की कविताओं को प्रकाशित करने के बाद जो प्रतिक्रियाएँ मिली उससे यह अंदाज़ा लगा कि हमारे पाठक बासी और टटका कविता को पहचानना जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कौन सी कविता हमेशा खाई जा सकती है। आज इसी कड़ी में युवा कवि सुशील कुमार की बिलकुल टटका कविता हम आपको पढ़वा रहे हैं। इनका विस्तृत परिचय फिर कभी, फिलहाल इनका वक्तव्य प्रकाशित कर इस भार से मुक्त हो रहे हैं- इस आशा के साथ कि इनकी कलम हमारी बातों, हमारे इर्द-गिर्द और उसमें पसरी विडम्बनाओं तथा हमारे सपनों पर जमी धूल को थोड़ा सा उड़ाएँगी ज़रूर। शायद इसे टटका भात की तरह नहीं, बल्कि मकई की रोटी की तरह धीरे-धीरे खाना पड़े।
घर और घर
सुशील कुमार

वक्तव्य- "जब मेरे मन की समप्रवाहित नदी में कोई पत्थर फेंकता है या वातावरण का भूगोल कोई उछाल लाता है तब स्वमेव वहाँ भावों के प्रपातों की सृष्टि होने लगती है। तब भीतर शब्द बजने लगते हैं नगाड़े की तरह और विवश हो उठता हूँ मैं अभिव्यक्ति के लिये। तब ही कहीं शब्द मुझे रच पाते हैं...। जितनी बार मैं कविता लिखता हूँ, शब्द मुझे झिंझोरते हैं, जगाते हैं तो कभी मदहोश करते हैं और अपनी गोद में सुलाते हैं । उनकी आहट पाकर मैं बेचैन हो जाता हूँ उसे आकार देने के लिये। सृजन की यह बेला मेरे लिये बड़ी ताजा, निराली... पर कसक भरी होती है जहाँ समय मेरे लिये स्थिर हो जाता है और घड़ी की सुईयाँ मानो रुक सी जाती हैं। ऐसे कितने ही क्षण मैंने उन भावतरंगों की सम्मोहनावस्था (हिप्नोटिक स्टेट) में जिये हैं कविता के पालने में झूलते हुए। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता क्योंकि वही अपनी उर्जा है जिसे जीवन-यात्रा की बीहड़ घाटियों के बीच गुजरते हुए मैंने उन क्षणों की चिर-नवीन तह से ही निचोड़कर पाये हैं। यह मेरे जीवन के तपते जंगल में तरुवर-सी छाया और श्रांति देती है जहाँ जन (मॉस) के उस विराट रूप का साक्षात्कार कर पाता हूँ जिसने अपने श्रम-सौंदर्य से इस उबड़-खाबड़ धरती को रहने और जीने के लायक बनाने में कोई कोर-कसर तो नहीं छोड़ रखा है पर जो आज भी चंद मुठ्ठी-भर लोगों की जकड़न में कराह रहा है।"
वह मेरे भीतर-कहीं से निकलकर
वक्तव्य- "जब मेरे मन की समप्रवाहित नदी में कोई पत्थर फेंकता है या वातावरण का भूगोल कोई उछाल लाता है तब स्वमेव वहाँ भावों के प्रपातों की सृष्टि होने लगती है। तब भीतर शब्द बजने लगते हैं नगाड़े की तरह और विवश हो उठता हूँ मैं अभिव्यक्ति के लिये। तब ही कहीं शब्द मुझे रच पाते हैं...। जितनी बार मैं कविता लिखता हूँ, शब्द मुझे झिंझोरते हैं, जगाते हैं तो कभी मदहोश करते हैं और अपनी गोद में सुलाते हैं । उनकी आहट पाकर मैं बेचैन हो जाता हूँ उसे आकार देने के लिये। सृजन की यह बेला मेरे लिये बड़ी ताजा, निराली... पर कसक भरी होती है जहाँ समय मेरे लिये स्थिर हो जाता है और घड़ी की सुईयाँ मानो रुक सी जाती हैं। ऐसे कितने ही क्षण मैंने उन भावतरंगों की सम्मोहनावस्था (हिप्नोटिक स्टेट) में जिये हैं कविता के पालने में झूलते हुए। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता क्योंकि वही अपनी उर्जा है जिसे जीवन-यात्रा की बीहड़ घाटियों के बीच गुजरते हुए मैंने उन क्षणों की चिर-नवीन तह से ही निचोड़कर पाये हैं। यह मेरे जीवन के तपते जंगल में तरुवर-सी छाया और श्रांति देती है जहाँ जन (मॉस) के उस विराट रूप का साक्षात्कार कर पाता हूँ जिसने अपने श्रम-सौंदर्य से इस उबड़-खाबड़ धरती को रहने और जीने के लायक बनाने में कोई कोर-कसर तो नहीं छोड़ रखा है पर जो आज भी चंद मुठ्ठी-भर लोगों की जकड़न में कराह रहा है।"
मेरे सामने खड़ा हो गया
और बुदबुदाने लगा -
घर वह नहीं
जहाँ आदमी रहता है
घरों में आदमी अब कहाँ रहता है
जिसे तुम घर कहते हो
वह तो एक तबेला है
लानतों के सामान यहाँ
लीदों की तरह पसरे रहते हैं
हाँ, काँखते घोड़ों को अपनी देह से उतार
जिन खूँटों से आदमी
देर रात गये रोज़ बांधता है
सहुलियत के लिये उस जगह को
तुम घर कह सकते हो
क्योंकि तब उसके रोशनदानों से दरवाजों तक
अँधेरा परदे की तरह गिरता है
और ऊब और तनाव से लिपटे
सन्नाटे के साये में
कुछ देर के लिये वह जगह
एकान्त-निकेतन में तब्दील हो जाती है
जहाँ औरतें काम से निबरती हैं
बच्चे सपने बुनते हैं और
बुड्ढे अपने दाँत किटकिटाते हैं
ठीक इसी वक्त गगनचुंबी महलातों
की बत्तियाँ बुझा दी जाती है
और रात निर्वस्त्र होकर ‘हिपॉक्रिटिक’ चेहरों
को अपनी आगोश में ले लेती है
जिसके अँधेरे में लावारिस कुत्ते
डरावनी आवाज़ में भौंकते हैं
(तो कभी तेज स्वर में रोते हैं)
पर यह सब महज़ चंद घंटों का खेल है !
सहमति में मैंने सिर हिला दिया,
कहा - हाँ, घर अब फक़त
बूढे़ जवान बच्चे... सबकी
नींद की ख्वाहिशें हैं
जो उनके कल के घर की वसीयतें हैं
जहाँ रात कहीं सुनसान होती है कहीं बदनाम
यह सुनकर वह बिगड़ गया -
उसे घर मत समझो
न नींद को उसके घर की वसीयत...
दरअसल वह कोई सराय जैसा है
या बनजारों के डेरा सा
या फिर रात की खुमारी में डूबे
उन महलों सा जहाँ
दिगम्बराओं की बाँहों में
कितने ही झक्क सफ़ेद कामदेव
झूलते नज़र आते हैं !
‘और नींद ...?’ - मैंने घबराकर पूछा ।
वह तो लोगों के दिमाग में
पलता एक वहम है
अब न घर सोता है
न धड़
क्योंकि घर बेहद डरा-सहमा
एक इंसान है
जो मुर्गे की पहली बांग पर
तिलमिला उठता है और
सुबह होने तक
तिनका सा बिखर जाता है
क्या तुम्हें मालुम नहीं कि
ख्यालों में कई-कई घर होते हैं लोगों के
जिन्हें ढोते फिरते हैं अपने भीतर दिन-भर ?
एक घर माँ की कोख़ थी
पर वह एक था, सुख-शांति की
छाया फैली थी उस घर में
पर अब ...?
अब तो आदमी अपने घरों में नाशाद रहता है !
जितना नाशाद रहता है
उतने ही नये घरों की कामना करता है
हाँ, यह बात अलग है कि
जिनके घर नहीं होते
वे राह-बाट.. कहीं भी अपना घर बना लेते हैं
पर तुम उसे घर कहने से सकुचाते हो
क्योंकि उन घरों में दीवारें नहीं होती
न परदे ही झूलते हैं वहाँ
लाज की दीवारों से बनी इन घरों
को कोई कब उजाड़ दे, पता नहीं
फिर भी घर न होने का दु:ख
उन्हें सालता नहीं
जितना सालता है मौके़-बेमौके़
अपनी आबरू की दीवारें दरकने का दर्द
बिलों में कन्दराओं में
मांदों में घोंसलों में
पेड़ों पर भी इसी दुनिया के जीव
बसेरा डालते हैं
पर तुम उन्हें ‘घर’ की संज्ञा नहीं देते
जहाँ उनकी संततियाँ जनमती है
और पलती है
पर यह आदमी ही है सिर्फ़
जो दीवारें बनाता है
घर बनाने के नाम पर
और अपने सिर पर छतें
ढोता है घर रचने के खेल में
और एक साथ कई-कई घरों के बोझ तले
कहीं नहीं रहता है !
...और रात को दाग़दार करता है !!
उसकी बातें सुन मैं
हक्का-बक्का होने लगता हूँ, तभी
वह फिर मुझे झिंझोरता है-
सदियों से अपने को
स्थापित करने के उपक्रम में
आदमी अपने घर की तलाश में
रोज़ भटकता है
और आजीवन निर्वासन भोगता हुआ
एक दिन सो जाता है चिर-निद्रा में कहीं भी...
इतिहास के पन्ने पर अगर कहीं नाम भी
दर्ज कर जाता है
तो कहाँ होता है उसका पता-ठिकाना ?
कहाँ होता है तब घर उसका ? ?
- कहता हुआ वह फिर
मुझमें प्रवेश कर जाता है।




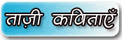




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
34 कविताप्रेमियों का कहना है :
अच्छी थी कविता..पर ऐसा लगा थोडा अनावश्यक लंबाई थी..
पर फिर भी दिमाग में हलचल मचाने वाली थी...
रुखड़ी भाषा में जीवन के सच और विडम्बनाओं पर कई सवाल खड़ी करती बहुत ही बेहतरीन कविता है भाई सुशील कुमार की। बधाई । और हिंद युग्म को भी कि समय-समय पर इतनी बेजोड़ चीज़ें पढवाती है।
Really a nice poem that put me in hypnotic state for a while. Thanks
कविता के भाव प्रभावी हैं, पर लम्बाई अनावश्यक रूप से बढाई गयी है।
-Zakir Ali ‘Rajnish’
{ Secretary-TSALIIM & SBAI }
Ek prabhavshali kavita ! Beshak kuchh lambi ho gayi hai, par pathak ko giraft meiN leti hai. Badhai !
सुशील कुमार की कविताओं को पढ़कर सर्वेश्वर दयाल सकेसेना और धूमिल की याद ताजा हो आयी। उसी परम्परा की कविता लगती है।
पूरी कविता बिना कहीं रुके एक बार में पढ़ गया. सीधी और सपाट कहन में सुशील जी ने एक लम्बे अरसे से उमड़-धुमड़ रहे भावों को समेट कर हमारे सामने परोसा है, और पाठक को अवसर दिया है यथाशक्ति डाइजेस्ट करने का. रचना में भाई सुश्हेल जी का आक्रोश स्पष्ट नज़र आ रहा है, उन्होंने घर के यथार्थ आशय को हमारे सामने लाने का प्रयास किया है और वो काफी हद तक अपने मकसद में सफल भी हुए हैं.
बधाई.
- विजय
जीवन के यथार्थ को उजागर करती कविता के लियेसुधील जि को बहुत बहुत बधा हिन्द युग्म की हिन्दी सेवा का उपक्रम सराह्नीय है
सुशील कुमार की यह कविता समकालीन साहित्य के चालू मुहावरे को तोडती हुई घर के उस मिथक को तोडती है जिसमे सबकुछ होम स्वीट होम में रिड्यूस कर दिया जाता है और इस तरह वह मध्यवर्गीय हदबंदी भी जिसने कविता की रीढ सोख ली है। इन्हीं अर्थों में वह टटका भी है।
हां कहीं कहीं सपाटबयानी खलती है सो कोई नहीं!!
अच्छी लगी कविता .
सुशील जी, कविता में ही नहीं गद्य में भी नए मुहावरे गढ़ते हैं, इसलिए किसी किसी को लम्बाई की शिकायत हो सकती है, लेकिन कविता नए अर्थों को , नए प्रतिमानों को जगह देती हुई सफलता से अपनी बात कह रही है।
बधाई!!
Rati Saxena
HINDI YUGM PAR KAVIVAR SUSHEEL
KUMAR JEE KEE KAVIT" GHAR AUR GHAR
KAA ANTAR" PADH KAR BAHUT ACHCHHA
LAGAA HAI.YUN TO UNKEE KAVITAAON
MEIN PRAKRITI KAA SWAR MUKHYA HOTA
HAI LEKIN JEEVAN SE SAMBANDHIT UN
KEE YE KAVITA NISSANDEH BEJOD HAI,
MUN KO JHAKJHORNE WALA AESA YTHARTH
MAINE ANYATRA KAM HEE DEKHA HAI.
KAVITA JITNEE LAMBEE HAI UTNE HEE
UNCHE BHAAV HAIN.SASHAKT BHASHA-
SHAELEE MEIN LIKHEE IS KAVITA KO
PADHVAANE KE LIYE MAIN HINDI YUGM
KO SALAAM KARTAA HOON
बहुत अच्छी कविता लगी.
धन्यवाद
bahut prabhavit hua,sachchai ka yatharth parak varnan,dhanyawad.
बेहद विचारोत्तोजक रचना। पढकर एक नया हीं अनुभव मिला। हाँ कविता लंबी है, लेकिन मुझे इसकी लंबाई ज्यादा नहीं लगी। कविता की लंबाई बित्तों से नहीं नापी जानी चाहिए, बल्कि इस बात से नापी जानी चाहिए कि पढते समय बोरियत तो महसूस नहीं हो रही। और मुझे कहीं भी बोरिय्त की अनुभूति नहीं हुई। इसलिए मेरे लिए यह कविता प्रशंसनीय है।
-विश्व दीपक
अच्छा लिखा है
समझ आता है
सरलता भाती है
कविता की थाती है।
बहुत खूब
मेरे ईमेल पर रेखा मैत्रा जी (rekha.maitra@gmail.com)एक संदेश आया है, उसे यहां दे रहा हूं-
रतिजी की कविता सुन्दर है और आपकी घर कविता भी ! बढ़ाई !
दिगम्बराओं की बाँहों में
कितने ही झक्क सफ़ेद कामदेव
Sabdo ka cyan bhut badiya hai aur saral, pervahmaie sheelie hai.
Ghar aur hgar ka antar tiik veesha jeesa maanavtaa aur amaanabtaa, neetikta aur aneetikta.Yaatharth ka chintan hai.Lanbi kavita hai.
Badhaie.
Manju Gupta.
दीना नाथ जी,
कम से कम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल को तो बख्श दें. अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को रखना चाहें तो कोई बात नहीं लेकिन धूमिल को अवश्य छोड़ दें.
दिलो-ज़िह्न की भी सूरत मेरे मकां सी है,
के सामां कम है सही और, कबाड़ ज़्यादा है..
अच्छी लम्बी कविता....
वाह मनु साहब वाह, क्या बात है!
उचटती नींद के काँधे हिला के ख़्वाब ए परीशां ने यूं कहा
वो घर कहाँ है जहां बस्तियां थीं बेफिक्र नींदों की !
चिढ़ के नींद ने कहा अब मकानों में मकीं नहीं रहते
सामान ए आसाइश रहता है, मकीं रातें बिताने घर में आते हैं
-अहसन
वाह मनु साहब वाह, क्या बात है!
उचटती नींद के काँधे हिला के ख़्वाब ए परीशां ने यूं कहा
वो घर कहाँ है जहां बस्तियां थीं बेफिक्र नींदों की !
चिढ़ के नींद ने कहा अब मकानों में मकीं नहीं रहते
सामान ए आसाइश रहता है, मकीं रातें बिताने घर में आते हैं
-अहसन
'वह घर नहीं जहां आदमी रहता है '
सच सुशील कुमार जी की कविता ने सचाई से रूबरू करवाया है |
वह मेरे भीतर-कहीं से निकलकर
मेरे सामने खड़ा हो गया
और बुदबुदाने लगा -
घर वह नहीं
जहाँ आदमी रहता है
घरों में आदमी अब कहाँ रहता है
जिसे तुम घर कहते हो
वह तो एक तबेला है
लानतों के सामान यहाँ
लीदों की तरह पसरे रहते हैं
हाँ, काँखते घोड़ों को अपनी देह से उतार
जिन खूँटों से आदमी
देर रात गये रोज़ बांधता है
सहुलियत के लिये उस जगह को
तुम घर कह सकते हो
आपने एक मिल भेजा था. जिसे मैंने आज देखा.और आपकी कविता पढ़ी..सुशील जी आपकी कविता में जो फिलोसफी है वेह बहतु अच्छी लगी.
Ek kahavat kahi jaati hai ki gady lekhak jo baat 6 sau lines mein kahta vo kavi pady ki 6 lines mein kah deta hai. kavi ya lekhak blogaron kii jhoothi tareef ke shikar ho jate hain. kavi svayam aatm manthan kare to jada behtar. main aapki rachna se behad khush nahin hua. fir bhi badhai deta hoon. meri tippani ko anyatha na lekar sakaratmak lenge yahi asha karta hoon.
कल से कविता को पढने की कोशिश कर रही थी, किन्तु नेट पर यह पृष्ठ खुल ही नहीं रहा था, आज कविता की शुरू की चंद पंक्तियाँ पढ़ी बाकी कविता पढने से पहले सारे कमेंट्स पढ़े फिर कविता पढ़ी . सभी ने तारीफ़ की है, और यह कहा है कि कविता की लम्बाई ज्यादा है, क्या वास्तव में जो कुछ इतना कहा या लिखा गया है , वो लिखने की जरूरत थी? मुझे लगा कि सारी कविता का सार इन चंद पंक्तियों में है......
सदियों से अपने को
स्थापित करने के उपक्रम में
आदमी अपने घर की तलाश में
रोज़ भटकता है
और आजीवन निर्वासन भोगता हुआ
एक दिन सो जाता है चिर-निद्रा में कहीं भी...
इतिहास के पन्ने पर अगर कहीं नाम भी
दर्ज कर जाता है
तो कहाँ होता है उसका पता-ठिकाना ?
कहाँ होता है तब घर उसका ? ?
घर अच्छी कविता है लेकिन कहीं कहीं absurd हो जाती है शायद यह कवी की सम्मोहनावस्था में लिखी पंक्तियाँ होंगी
सशक्त कविता.
इस से अधिक तारीफ़ करने पर अपने आप से बगावत होती है
इस से कम तारीफ करने पर समाज का भय खाता है
-अहसन
बिलकुल सही !
ठीक इसी वक्त गगनचुंबी महलातों
की बत्तियाँ बुझा दी जाती है
और रात निर्वस्त्र होकर ‘हिपॉक्रिटिक’ चेहरों
को अपनी आगोश में ले लेती है
जिसके अँधेरे में लावारिस कुत्ते
डरावनी आवाज़ में भौंकते हैं
(तो कभी तेज स्वर में रोते हैं)
बधाई|
कई बार पढी कविता को........पर सच कहूँ कि जो अनुभूत हुआ उसे अभिव्यक्ति देने के लिए उपयुक्त शब्द संधान नहीं कर पा रही.....
बहुत ही भावपूर्ण और प्रभावशाली रचना है,जो सोचने को खुराक देती है...
सतत सुन्दर लेखन के लिए आपको अनंत शुभकामनाये...
घर बनाने के नाम पर
और अपने सिर पर छतें
ढोता है घर रचने के खेल में
और एक साथ कई-कई घरों के बोझ तले
कहीं नहीं रहता है !
जिन्दगी का बेहद सजीव चित्रण करती ये पंक्तियां बहुत ही सुन्दर लगी, आभार्
अच्छी कविता बहुत बहुत बधाई
विमल कुमार हेडा
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)