सितंबर माह की प्रतियोगिता के माध्यम से हिंद-युग्म के एक पुराने नाम पीयूष पंड्या लंबे वक्त के बाद पाठकों से मुखातिब हुए हैं। इससे पहले इनकी पिछली कविता मार्च 2008 मे हिंद-युग्म पर प्रकाशित हुई थी। सितंबर माह मे इनकी कविता तीसरे स्थान पर रही है। किसी शहर से अपनी मुहब्बत को कोई कवि किस तरह खूबसूरत हर्फ़ों के नाज़ुक पैरहन पहना सकता है, प्रस्तुत कविता इसकी एक बानगी है। कविता झीलों के शहर भोपाल, जिसे दरवाजों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, का शहरनामा है।
पुरस्कृत कविता: शहरनामा
मैं आता हूँ और खो जाता हूँ,
जाता हूँ तो रह जाता हूँ,
रहता हूँ और बह जाता हूँ,
हाँ...
हाँ, नहीं छूटती ये बादानोशी,...
ये शहर ज़िंदगी पिलाता है|
सर्पिल-उर्मिल, राहों-लहरों में,
बहता-डूबता पी लिया गया हूँ,
और मैने इसे पी लिया है,
और जी लिया है
हम शहर और ये शज़र है,
जड़ें, सड़कें और धमनियाँ
अब जुदा नहीं..
तिलिस्मी पानियों पर टप्पे खाता हुआ चाँद फेंको तो,
सुबह को सूरज बन जाता है
पानी ये..
प्यास बुझाता है या बढ़ाता है
नहीं जानता मैं
मगर झीलों के इस शहर में,
मीलों के इस शजर में
वज़ू कर लेने के बाद
इबादत की ज़रूरत नही होती !
चौक की फिरनियों, अमरकों और क़बाबों से,
दुनियादारी के स्वाद नमूदार हुए हैं,
यहाँ कई बंजारों के घर-बार हुए हैं,
और कोई इकबाल के कौंवों से पूछो,
यहाँ कितने शायर तैयार हुए हैं !
झीलों की मीनाकारी,
संग-ए-शब्ज़ पर,
किसने ये ताजमहल बनाया,
कि शाहजहाँ यहाँ के सारे,
खुद को फ़क़ीर समझते हैं |
दरवाज़ो को शहर है ये,
हरे-लाल-धानी,
कितने ही कमरों को इसने जोड़ा है..
घुटनों को हमारे पेट की ओर मोड़ा है !
या कि ज़िंदा सूफ़ी है ये,
और दुआओं की दरगाह से उठते धुएँ...
पेड़ बन गये है इसके सीने पे
या जैसे बेपरवाह कोई लड़का,
खीसों में हाथ और झीलों मे पैर डाले,
बेफिक्री की सिटी बजाता है !
हो जाऊं फ़ना इस...
कौह-ए-फ़िज़ा-ओ-कूबा-ए-यार में
कभी फ़ुर्सत मे मर जाना चाहता हूँ,
कि बाकी की ज़िंदगी के लिए...
ये काफ़ी होगा !
सुना है,
औरंगज़ेब गुजरा था यहाँ से, (सफ़र-ए-सल्तनत के लिये)
पर ठहरा नहीं..
किसी ने कहा था उससे,
ठहरना नहीं यहाँ
वरना छोड़ नहीं पाओगे.
________________________________________________________________
पुरस्कार: विचार और संस्कृति की चर्चित पत्रिका समयांतर की एक वर्ष की निःशुल्क सदस्यता।




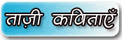




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
7 कविताप्रेमियों का कहना है :
कौन जाए ज़ोंक , मगर,
अपने शहर की गलियां छोड़ कर ..
मनमोहक रचना, nostalgic , लिखते रहिये ...
Very Nice!
अपनों के लिए अपनापन जगाती अच्छी कविता।
yah kavita kuch adbhut images le ke aati hai ...bhopal dekhne ka dil karta hai .... behad pasand aayi..
हो जाऊं फ़ना इस...
कौह-ए-फ़िज़ा-ओ-कूबा-ए-यार में
कभी फ़ुर्सत मे मर जाना चाहता हूँ,
कि बाकी की ज़िंदगी के लिए...
ये काफ़ी होगा !
बहुत ही सुन्दर प्रस्तुति ।
बहत ही शानदार दोस्त.. मज़ा आ गया पढकर!
“सुना है,
औरंगज़ेब गुजरा था यहाँ से, (सफ़र-ए-सल्तनत के लिये)
पर ठहरा नहीं..
किसी ने कहा था उससे,
ठहरना नहीं यहाँ
वरना छोड़ नहीं पाओगे.” इस तरह के अशार गालिबन नामचीन शायर मीर साहेब के थे “याद उसकी कुछ खास नहीं अय मीर बाज़ आ. वरना उसको इस दिल से भुला ना पायेगा.” अब आपने ये बात और खूबी भोपाल के बारे में कही है. खैर हमें तो इसका इतना इल्म नहीं है कि जो भोपाल ठहर गया सो छोड़ नहीं पायेगा. बहरहाल आपकी मंज़रकशी और शायरी बेहतरीन है. भोपाल के लिए अप्पके दिल में जो मोहब्बत का ज़ज्बा है वह काबिले तारीफ़ है और आपकी कविता इसे हूबहू बयान कर रही है. आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद. अश्विनी कुमार रॉय
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)