विजयशंकर चतुर्वेदी हिन्द-युग्म के यूनिकवि रह चुके हैं। कवि की कई कविताएँ हिन्द-युग्म पर प्रकाशित हैं। हाल ही में राधाकृष्ण प्रकाशन से कवि का एक कविता-संग्रह 'पृथ्वी के लिए तो रुको' प्रकाशित हुआ है, उसमें कुछ ऐसी कविताएँ भी संकलित हैं जो हिन्द-युग्म पर पहले से ही प्रकाशित हैं (जैसे- गुरुजन, श्राप, बीड़ी सुलगाते पिता, धीरे-धीरे, हरकारे से अनुरोध, रुदन इत्यादि)। हमने अच्छी कविताओं के संग्रह को हिन्द-युग्म पर हमेशा महत्व दिया है। पाठकों को याद होगा कि हमने हरेप्रकाश उपाध्याय के कविता संग्रह 'खिलाड़ी दोस्त तथा अन्य कविताएँ' और अंजना बख्शी के कविता संग्रह 'गुलाबी रंगों वाली वो देह' से कविताएँ प्रकाशित की थी। आज हम विजयशंकर चतुर्वेदी के कविता संग्रह से कुछ कविताएँ प्रकाशित कर रहे हैं। बिना अपनी टिप्पणी के। आप आज पढ़िए किताब पर प्रकाशित वरिष्ठ कवि लीलाधर जगूड़ी की टिप्पणी-
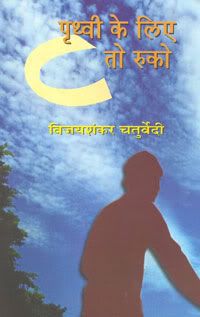 विजयशंकर चतुर्वेदी एक ऐसे नवोदित कवि हैं जो अपने को आज के सूर्योदय के साथ-साथ उस सुबह से भी जोड़कर देखते हैं जो निर्माणाधीन सृष्टि की पहली सुबह रही होगी। इतने विराट समय में अपनी निरन्तरता को देखना कवि की अद्भुत विशेषता है, जो ध्यान खींचे बिना नहीं रहती। प्राकृतिक विपत्तियों से लड़ते, सीखते मनुष्य की कूवत कैसे-कैसे अपने को अभिव्यक्ति के लायक तरासती रही है और कैसे उन सारे द्वन्द्वों से मनुष्य ने एक निर्द्वंद्व सभ्यता के लिए अपने को संघर्षरत रखा है; इस तरह के तमाम संधि-समयों से गुजरते हुए कैसे वह मनुष्य आज तक के समय में पहुंचा है कवि अपनी उस युद्धगाथा को एक बार फिर से कहने की बेचैनी से भरा हुआ दिखता है।
विजयशंकर चतुर्वेदी एक ऐसे नवोदित कवि हैं जो अपने को आज के सूर्योदय के साथ-साथ उस सुबह से भी जोड़कर देखते हैं जो निर्माणाधीन सृष्टि की पहली सुबह रही होगी। इतने विराट समय में अपनी निरन्तरता को देखना कवि की अद्भुत विशेषता है, जो ध्यान खींचे बिना नहीं रहती। प्राकृतिक विपत्तियों से लड़ते, सीखते मनुष्य की कूवत कैसे-कैसे अपने को अभिव्यक्ति के लायक तरासती रही है और कैसे उन सारे द्वन्द्वों से मनुष्य ने एक निर्द्वंद्व सभ्यता के लिए अपने को संघर्षरत रखा है; इस तरह के तमाम संधि-समयों से गुजरते हुए कैसे वह मनुष्य आज तक के समय में पहुंचा है कवि अपनी उस युद्धगाथा को एक बार फिर से कहने की बेचैनी से भरा हुआ दिखता है।इस सांस्कृतिक यात्रा और यातना में मनुष्य ने कितने असुन्दर के बदले कितना सुन्दर गंवाया है, उस भूल-चूक भरे अंधकार को कवि ने अपनी अभिव्यक्ति के विस्फोटक उजालों से भर दिया है। सामाजिक दिक् और काल के बीच इस ब्रह्माण्ड के शंख को सुनने की शक्ति हमें कवि की बिम्बपूर्ण भाषा से मिलती है। कुछ लोगों ने इस पृथ्वी को एक परिवार की जगह सिर्फ बाज़ार और कार्यालय की मेज़ बनाकर रख दिया है। कवि, इस पृथ्वी पर एक मनुष्योचित सूर्योदय की प्रतीक्षा में है। अपनी सुन्दर, प्यारी और वैचारिक पृथ्वी को कवि रसातल में जाने से रोकना चाहता है। यही चिन्ता और संघर्ष इन कविताओं के केन्द्र में है। पौधों और भाई-बहनों के बीच विजयशंकर की कवितायें अपने को बड़ा होती हुई देखती हैं। जहां गर्व करने लायक `झील-सी आंखों वाली लड़कियां` भी किसी
परमात्मा को प्यारी हो जाती हैं। जिन्दगी के इस ट्रैफिक में कवि को ऐन मौके पर सही ब्रेक लगने की उम्मीद है, जो बता सकेगा कि -`दुनिया अभी जीने लायक है।` टेक्नॉलॉजी के साथ कवि जीवन के उत्सव को नयी तरह से मनाना चाहता है, जहां धरती और घर से अलविदा कहने का मन न हो। कवि पृथ्वी और घर में एक नये अनुशासन की कामना करता है। दुनिया इतनी सुन्दर और अनुशासित हो कि `आकाशगंगा जैसा जगमग बस स्टैण्ड` लगे। और इन्हीं बसों में लोग अपने चन्द्रयात्रियों का इन्तज़ार कर रहे हों। इस तरह कवि पृथ्वी रूपी घर में रहकर गृहस्थी का अर्थ बदलना चाहता है।
विजयशंकर की कविता में माइथोलॉजी और टेक्नॉलॉजी, दोनों का अंगीकार दिखता है। यह बात तब और साफ हो जाती है जब कवि कहता है कि `शोकाकुल परिजन ले जायें तो ले जायें, मैं जलूंगा नहीं।` पर विज्ञापन का दंश कवि की चेतना का पीछा वहां भी नहीं छोड़ता। स्त्री के तीन रूप विजय की कविताओं में अक्सर आते हैं बेटी, स्त्री और मां। स्त्री के तीनों रूप इन कविताओं में खतरों से घिरे हुए दिखते हैं। वे रूप सुख के किन्हीं चमकीले दिनों में नहीं बल्कि अक्सर बारिश के डूबते दिनों में ज्यादा दिखते हैं। कवि खुद को मां और पिता के रूप में कई बार नये सिरे से जूझते हुए देखता है। वह टूटता नहीं बल्कि उसी डाल से एक नये पत्ते की तरह अपने लिए कोई राह निकाल लेता है। इस संग्रह की कविताओं में कई जगह यह कायान्तरण या रूपान्तरण दिखता है जो कि उनकी भावी निर्मिति के प्रति हमें आश्वस्त करता है और वह भी तैंतीस करोड़ देवताओं के बावजूद।
विजयशंकर को मैं उनके पहले कविता संग्रह के प्रकाशन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि उनकी इन कविताओं को देखकर उनके विकास और बदलाव की प्रबल संभावनायें अपनी ओर खींचती हैं। विजयशंकर अपने भीतर के सन्देहशील कवि को निरन्तर खोजते और तराशते जा रहे हैं इसलिए उनकी यात्रा निश्चय ही अर्थपूर्ण और लंबी होगी।
-लीलाधर जगूड़ी
सम्बंधीजन
मेरी आंखें हैं मां जैसी
हाथ पिता जैसे
चेहरा-मोहरा मिलता होगा जरूर
कुटुंब के किसी आदमी से.
हो सकता है मिलता हो दुनिया के पहले आदमी से
मेरे उठने बैठने का ढंग
बोलने बतियाने में हो उन्हीं में से किसी एक का रंग
बहुत सम्भव है मैं होऊं उनका अंश
जिन्होंने देखे हों दुनिया को सुन्दर बनाने के सपने
क्या पता गुफाओं से पहलेपहल निकलने वाले रहे हों मेरे अपने
या फिर पुरखे रहे हों जगद्गुरु शिल्पी
गढ़ गये हों दुनिया भर के मन्दिरों में मूर्तियां
उकेर गये हों भित्तिचित्र
कौन जाने कोई पुरखा मुझ तक पहुंचा रहा हो ऋचायें
और धुन रहा हो सिर.
निश्चित ही मैं सुरक्षित बीज हूं सदियों से दबा धरती में
सुनता आया हूं सिर पर गड़गड़ाते हल
और लड़ाकू विमानों का गर्ज़न
यह समय है मेरे उगने का
मैं उगूंगा और दुनिया को धरती के किस्सों से भर दूंगा
मैं उनका वंशज हूं जिन्होंने चरायी भेड़ें
और लहलहा दिये मैदान.
सम्भव है कि हमलावर मेरे कोई लगते हों
कोई धागा जुड़ता दिख सकता है आक्रान्ताओं से
पर मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा चीजों को नष्ट करने के लिए
भस्म करने की निगाह से नहीं देखूंगा कुछ भी
मेरी आंखें मां जैसी हैं
हाथ पिता जैसे.
कोई नहीं गिरता पृथ्वी से नीचे
पृथ्वी एक विशाल मेज है गोलाकार
जिस पर चलता आया है दुनिया का कारोबार
इसी मेज पर जन्मीं प्राचीन से प्राचीनतम सभ्यतायें
मिटते गये बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम और यूनान
मगर सदा बहता रहा अनन्त भविष्य का जीवन-जल
वेद, अवेस्तां, बाइबल, कुरआन, श्रुति
ब्राम्हण ग्रन्थ, आरण्यक, मीमांशा, निरुक्त
रचे गये इसी मेज पर बैठकर.
इसी पर लपलपायी ज्वालामुखियों की जीभ
तरबूज की तरह कंपाया भूकंपों ने इसे असंख्य बार
मेज पर उगती रहीं पर्वत श्रृंखलायें अनगिन
फूट पड़ीं नील, दज़ला, फरात, गंगा, अमेजन
पेड़ों की पता नहीं कितनी पीढ़ियां होती रहीं कोयला
बन्दर से बनता रहा मनुष्य.
मगर यह भी नहीं है मनुष्य का अन्तिम रूप
गो कि पड़ती है उस पर पहले जैसी ही छांव-धूप
काल के रन्दे से छीलती रही है प्रकृति
करती रही है उसे अपने अनुरूप.
फिर ईश्वर आया और कण-कण में घुस गया
आये देवी-देवता, किन्नर-गन्धर्व आये
कुछ बिला गये कालान्तर में
कुछ बस्तियों में समा गये
फिर बने वर्ण और उनके प्रकार
वहीं से शुरू होता है हमारा अंधकार.
समय-समय पर आते रहे पैगंबर
लाते रहे अपने-अपने आकाओं के सन्देश
मनुष्य बदलता रहा अपना चेहरा
रूप-रंग-खान-पान-भूषा-वेश
घूमती रही यह मेज़ अहर्निश
दिक् और काल की वक्रता में.
मेज के आरपार हवा बहती रही बेरोकटोक
बजता रहा आसमान का नीला शंख
बहते रहे उन्चास पवन दशों दिशाओं में
मनुष्य जाति रही सदा अजर-अमर
मगर इस विराट मेज से लुढ़कर
नीचे नहीं गिरा कोई आज तक
फिर कैसे लुढ़क गये हमारे खेत?
हमारे शस्यश्यामला भूखण्ड, नदियां, वनप्रांतर?
कौन निगल गया हमारा मलयानिल,
किसने बुझा दी हमारी बड़वानल?
हम चीत्कार से तनी प्रत्यंचायें हैं
हमारे देव अलग हैं
असुर अलग
अलग है हमारा देवासुरसंग्राम.
फेन की तासीर में शामिल है समुद्र
समुद्र की तासीर में शामिल है फेन
हम नहीं चाहते कि फेन प्रलय बनकर बिखर जाये इस मेज पर.
जो अग्निपुंज बंधे रह गये थे कपास से
कहां गये वे हमारे अग्निगर्भा रिश्ते?
अब जो आग दिखती है हमारी नहीं
जो पर्वत श्रृंखलायें हैं,
जंजीरें हैं हमारे मन की
जो उपत्यकायें हैं,
असुरक्षित अन्तस हैं हमारा.
हमारा नहीं है सूर्योदय
सूर्यास्त भी नहीं है हमारा
हम रह गये हैं अपने त्रिशंकु
इसी दिक्-काल में स्थिरांक.
हम परिन्दों के लिए नहीं हैं
छांव देने वाले पेड़ों के लिए भी नहीं
पेड़ों की शाखाओं और उसकी अमरबेलों के लिए तो कुछ भी नहीं.
ये हाथियों की चिग्घाड़ें,
मेघों की गर्ज़नायें भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती.
क्यों लुढ़काये जा रहे हैं हम मेज से नीचे लगातार?
किसी हाथी का हौदा नहीं थी यह मेज
हमारा रंगमंच भी नहीं सजा था किसी अर्जुन के लिए,
तब क्यों ढीली कर दी कृष्ण ने अपनी तर्ज़नी?
हमारे गले, उनके सुदर्शन चक्र
हमारे धड़ों की जोड़ियां मिलाये नहीं मिलतीं सिरों से.
क्यों फेंका जा रहा है हमें घसीटकर मेज से नीचे
जहां नहीं है कोई आधार, कोई तल?
जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं
वह लगती है बाघिन जरख़रीद गुलाम संस्कारों की,
हे बाघिन, तुम रौंदो इस मेज को कुछ इस तरह
कि आन्दोलित हो जाये तन-मन
मिट जायें समस्त पन्थ, कुलनाम, गोत्र
मनुष्य मात्र का हो शिवताण्डवस्तोत्र
ताकि सूर्योदय हो सके हमारा
सूरज हो निखालिस हमारा अपना.
कोई गुरुत्वाकर्षण बांधे न बांधे
हम नहीं छोड़ेंगे इस विराट मेज का दामन
जिसकी गति हो रही है तेज़ से तेज़तर
लेकिन गिरता नहीं एक कण,
एक क्षण भी गिरता नहीं
फिर कैसे चले जायेंगे हम रसातल में?
देवता हैं तैंतीस करोड़
बहुत दिनों से देवता हैं तैंतीस करोड़
उनके हिस्से का खाना-पीना नहीं घटता
वे नहीं उलझते किसी अक्षांश-देशान्तर में
वे बुद्धि के ढेर
इन्द्रियां झकाझक उनकी
सर्दीखांसी से परे
ट्रेन से कटकर नहीं मरते
रहते हैं पत्थर में बनकर प्राण
कभी नहीं उठती उनके पेट में मरोड़
देवता हैं तैंतीस करोड़.
हम ढूंढ़ते हैं उन्हें
सूर्य के घोड़ों में
गंधाते दु:खों में
क्रोध में
शोक में
जीवन में
मृत्यु में
मक्खी में
खटमल में
देश में
प्रदेश में
धरती में
आकाश में
मन्दिर में
मस्जिद में
दंगे में
फ़साद में
शुरू में
बाद में
घास में
काई में
बाम्हन में
नाई में
बहेलिये के जाल में
पुजारी की खाल में
वे छिप जाते हैं
सल्फास की गोली में.
देवता कंधे पर बैठकर चलते हैं साथ
परछाई में रहते हैं पैवस्त
सोते हैं खुले में
धूप में
बारिश में
गांजे की चिलम में छिप जाते हैं हर वक्त.
नारियल हैं वे
चन्दन हैं
अक्षत हैं
धूप-गुग्गुल हैं देवता
कुछ अंधे
कुछ बहरे
कुछ लूले
कुछ लंगड़े
कुछ ऐंचे
कुछ तगड़े
बड़े अजायबघर हैं.
युगों-युगों के ठग
जन्मान्तरों के निष्ठुर
नहीं सुनते हाहाकार
प्राणियों की करुण पुकार
हम तमाम उम्र अधीर
मांगते वर गम्भीर
इतनी साधना
इतना योग
इतना त्याग
इतना जप
इतना तप
इतना ज्ञान
इतना दान
जाता है निष्फल.
वे छिपे रहते हैं मोतियाबिन्द में
फेफड़ों के कफ में
मन के मैल में
बालों के तेल में
हमारी पीड़ायें नुकीले तीर
छूटती रहती हैं धरती से आकाश
और बच-बच निकल जाते हैं तैंतीस करोड़ देवता.
हमारा घोर एकान्त
घनी रात
भूख-प्यास
घर न द्वार
राह में बैठे खूंखार
तड़कता है दिल-दिमाग
लौटती हैं पितरों की स्मृतियां
राह लौटती है
लौटते हैं युग
वह सब कुछ लौटता है
जो चला गया चौरासी करोड़ योनियों का
और तिलमिला उठते हैं
तैंतीस करोड़ देवता.




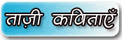




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
3 कविताप्रेमियों का कहना है :
sunder..
ham bhi jaane kab se sochte aa rahe hai ki ye devtaa log ghatate badhte kaahe nain...??
..मनुष्य मात्र का हो शिवताण्डवस्तोत्र
ताकि सूर्योदय हो सके हमारा..
..वाह! बेहतरीन कविता के लिए बधाई.
आज तो यही एक पढ़ सका.
पर मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा चीजों को नष्ट करने के लिए
भस्म करने की निगाह से नहीं देखूंगा कुछ भी
मेरी आंखें मां जैसी हैं
हाथ पिता जैसे.
बहुत ही गहरे उतरती यह पंक्तियां, बेहतरीन शब्द रचना, आभार ।
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)