नवंबर माह की प्रतियोगिता की दसवीं कविता के रचनाकार आलोक तिवारी हिंद-युग्म पर नये कवि हैं। हिंद-युग्म पर यह उनकी पहली ही कविता है।
 आलोक जी अपने बारे मे खुद कहते हैं- "सबसे कठिन होता है सच लिखना । तब और भी जब वह सच अपने विषय में हो । बहरहाल मैं पेशे से शिक्षक हूँ ‘राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, शालीमार बाग , दिल्ली -११००८८’ में। पिता भी शिक्षक हैं... सच्चे अर्थों में। बचपन फैजाबाद में बीता। घर में सबसे छोटा था, अत: दुलारा भी। किशोरावस्था तक कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। बड़े भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मैं तुलनात्मक दृष्टि से कम.... और तब और भी कम हो जाता था जब भाई से तुलना कर दी जाती थी.... ऐसा अक्सर ही होता था। धीरे-धीरे मन के किसी कोने में कुंठा घर करने लगी। मुझे ठीक-ठीक याद है.... कक्षा दस का नतीजा निकला था। जैसा कि उम्मीद थी मैं लगभग ५५% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। घर में मातम छा गया। मुझे दिलासे के तौर पर मेरे उस समय के विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय में विज्ञान या वाणिज्य विषय दिलवाने के आश्वासन दिए गए। किन्तु मुझे न जाने क्या हो गया कि... मैंने पहली बार विद्रोह कर दिया। मैंने कला वर्ग से आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया.... और कायम रहा। यह मेरे द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया गया पहला फैसला था। सबकी उम्मीदों के विपरीत बारहवीं में मैं प्रथम श्रेणी से तथा विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बचपन से ही किस्से-कहानियाँ पढ़ने का शौक था। विश्वविद्यालय में साहित्यिक समझ का विकास होने लगा....और न जाने कब मैं लिखने लगा। मित्रों ने मेरी रचनाओं को पढ़ा, सराहा, आलोचनाएं की और हिन्दी विभाग (हिन्दी भाषा परिषद् प्रकाशन) की पत्रिका में छापने के लिए भेज दिया। परिणामस्वरूप पहली कहानी (बुलडोज़र) छपी। फिर हिन्दी साहित्य सम्मलेन की पत्रिका ‘माध्यम’ में दो कवितायें छपी.... और सिलसिला चल निकला।"
आलोक जी अपने बारे मे खुद कहते हैं- "सबसे कठिन होता है सच लिखना । तब और भी जब वह सच अपने विषय में हो । बहरहाल मैं पेशे से शिक्षक हूँ ‘राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, शालीमार बाग , दिल्ली -११००८८’ में। पिता भी शिक्षक हैं... सच्चे अर्थों में। बचपन फैजाबाद में बीता। घर में सबसे छोटा था, अत: दुलारा भी। किशोरावस्था तक कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। बड़े भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मैं तुलनात्मक दृष्टि से कम.... और तब और भी कम हो जाता था जब भाई से तुलना कर दी जाती थी.... ऐसा अक्सर ही होता था। धीरे-धीरे मन के किसी कोने में कुंठा घर करने लगी। मुझे ठीक-ठीक याद है.... कक्षा दस का नतीजा निकला था। जैसा कि उम्मीद थी मैं लगभग ५५% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। घर में मातम छा गया। मुझे दिलासे के तौर पर मेरे उस समय के विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय में विज्ञान या वाणिज्य विषय दिलवाने के आश्वासन दिए गए। किन्तु मुझे न जाने क्या हो गया कि... मैंने पहली बार विद्रोह कर दिया। मैंने कला वर्ग से आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया.... और कायम रहा। यह मेरे द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया गया पहला फैसला था। सबकी उम्मीदों के विपरीत बारहवीं में मैं प्रथम श्रेणी से तथा विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बचपन से ही किस्से-कहानियाँ पढ़ने का शौक था। विश्वविद्यालय में साहित्यिक समझ का विकास होने लगा....और न जाने कब मैं लिखने लगा। मित्रों ने मेरी रचनाओं को पढ़ा, सराहा, आलोचनाएं की और हिन्दी विभाग (हिन्दी भाषा परिषद् प्रकाशन) की पत्रिका में छापने के लिए भेज दिया। परिणामस्वरूप पहली कहानी (बुलडोज़र) छपी। फिर हिन्दी साहित्य सम्मलेन की पत्रिका ‘माध्यम’ में दो कवितायें छपी.... और सिलसिला चल निकला।"पुरस्कृत कविता: बार्बी, चिंची और.....
मेरे दोस्त के बच्चे की गुडिया--‘बार्बी’
जी! इम्पोर्टेड है
जी हाँ! अपने पाँव पर चलती है
मॉडर्न है न!
खुद देख लो-
हेयर स्टाइल, ड्रेस, शूज़....
किन्तु ! चेहरे की चमक ?
क्या हुआ ?
गायब लगता है.... आत्मविश्वास ?
अरे छोडो यार !
तुम भी कहाँ उलझ गए....
नहीं भई, देखो तो !
चेहरे की मुस्कान....
विक्षिप्त सी है !
तू ही देख ---- पागल !
क्यों गायब है चमक ?
क्यों विक्षिप्त है मुस्कान ?
समझ नहीं आता....
आखिर सबकुछ तो है उसके पास !
कौंध सा जाता है
मन में वाक्य यह
सबकुछ तो था उसके पास
फिर क्यों मर गई.... चिंची !
बच्चा ही तो था मैं तब
चिंची फुदका करती थी जब
‘माँ चिंची त्यों आती है..’
‘तुमसे मिलने प्यारे बेटे..’
‘मेले पाछ त्यों नहीं आती?..’
‘शायद तुमसे डरती है..’
‘माँ मैं उछे नहीं मालूंगा..’
‘उसे विश्वास तो होने दो..’
धीरे-धीरे चिंची मेरे पास
तक आने लगी|
फिर हाथ पर
बैठ तक जाने लगी|
कभी कंधे पर फुदकती
फिर हौले से उड़ जाती|
कभी आँख में आँख डालकर
जाने क्या टटोल जाती|
मेरे सिर का लगा के चक्कर
कानों में चीं – चीं कहती|
फिर इक दिन मैं पिंजरा लाया|
माँ ने मुझे बहुत समझाया..
‘आती तो है तेरे पास..’
‘पल लोज़ चली भी जाती है..’
‘मैं तो उछको पालूंगा..’
मेरी ज़िद के आगे माँ
धीरे-धीरे चुप हो गई
जैसे पापा के आगे
अक्सर हो जाया करती थी !
अगली सुबह बैठ गया मैं|
पिंजरा युक्त, पानी-दाने से संयुक्त|
आयी फिर से चिंची मुक्त..!
वैसे ही कंधे पर बैठी,
आँखों में देखा वैसे,
वैसे ही फुदकी पिंजरे पर,
वैसे ही बोली चिंची|
पर मैं आज कहाँ वैसा था..
पिंजरा टेढ़ा किया ज़रा सा|
चिंची झट से उड़ी वहाँ से
बैठी जाके पेड़ की डाल,
कुछ देरी तक जाने क्या--
करती रही ख्याल|
फिर लौटी पिंजरे के पास
देखा मुझको भरकर आस
पिंजरे के फुदकी अंदर
मैंने बंद किया झट दर !
पीछे देखा माँ थी खड़ी
डबडबाई थी आँखें उसकी
‘माँ चिंची खुद ही आयी है’
माँ कुछ भी न बोल सकी
जाने क्या ताकती रही...!
अब चिंची निशि-दिन
मेरी थी|
मुझे देख चीं-चीं करती थी|
मैं भी उसको बहुत चाहता,
पानी-दाना रोज़ डालता|
पर चौथे दिन ....ठीक सुबह ही
चिंची उसमें गिरी मिली...!
माँ से पूछा,‘माँ चिंची त्यों नहीं उठ रही..’
माँ एकदम से ठिठक गयी
बोली बस इतना
‘मर गयी..!’
फिर शुन्य में देखने लगी|
मैं कुछ भी न समझ पाया था....
पर अब समझ रहा हूँ शायद....
इसीलिए तो आज ..बा..र्बी..!
‘----दोस्त, तुम भी अब समझो..!’
_____________________________________________________________
पुरस्कार- विचार और संस्कृति की चर्चित पत्रिका समयांतर की एक वर्ष की निःशुल्क सदस्यता।




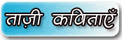




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
5 कविताप्रेमियों का कहना है :
कविता की शुरुआत अच्छी है, अगर बार्बी पर और चिंची पर अलग अलग कविताएँ लिखी जातीं तो शायद दोनों ही बहुत अच्छी होतीं, पर दोनों को मिलाने के कारण कविता ढंग से कुछ कह पाने में असमर्थ है और ज्यादातर मात्र वर्णन बनकर रह गई है। फिर भी कहीं कहीं पर काफी सुंदर बन पड़ी है। बधाई
धन्यवाद,
क्या कहूँ मित्र ....बार्बी और चिंची दोनों को शायद कलात्मक तरीकों अलग से किया जा सकता था, कविता भी इससे अधिक सम्प्रेषणीय हो जाती किन्तु इससे कविता अपनी मूल संवेदना से भटक जाती ........
"मैं कुछ भी न समझ पाया था....
पर अब समझ रहा हूँ शायद....
इसीलिए तो आज ..बा..र्बी..!
‘----दोस्त, तुम भी अब समझो..!’"
बहुत ही सुन्दर अभिव्यक्ति ।
Excellent Poem Alok ji. Keep it up in future also.........Hitendra kumar
very nice , many more like to read pl send more.
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)