नवम्बर माह की यूनिकवि प्रतियोगिता की अंतिम कविता डॉ॰ अनिल चड्डा की है। इससे पहले अनिल चड्डा की दो कविताएँ (एक नन्ही-मुन्नी के प्रश्न और त्रासदी) हिन्द-युग्म पर प्रकाशित हैं।
पुरस्कृत कविता-फिर बनती कैसे पहचान मेरी
बचपन के दिन थे
आँगन अपने में
खेलने के
कुछ लिखने के
कुछ पढ़ने के
मेरे अंदर के छुपे हुए
व्यक्तित्व के बाहर उभरने के
पर मुझको था घर में झोंक दिया
कुछ करने से
कुछ बनने से
मुझको अपनों ने रोक दिया
फिर बनती कैसे पहचान मेरी?
थी ज्यों-ज्यों कुछ मैं बड़ी हुई
परेशानी सबकी बढ़ती गई
घर से बाहर निकलने में
मेरी मुश्किल भी बढ़ती गई
इस जग में था बसता जंगल
मन में सबके था पशु छुपा
और आंखें भी लोलुपता से भरी
घर वाले थे परेशान बड़े
और मैं भी थी कुछ डरी-डरी
कच्चेपन में था विदा किया
हाथ मेरे पीले करके
कुछ समझ न पाई थी जीवन
फिर भी बोझे से लाद दिया
फिर बनती कैसे पहचान मेरी?
कुछ सहमी-सी
कुछ हिचकी-सी
जब तक थे होश संभल पाते
इक और जान के बोझ तले
मेरी नन्ही सी देह दबी
मेरा अंदर मेरा बाहर
था ममता से सरोबार हुआ
नये आने वाले की धुन में
जीवन मेरा घर-बाहर हुआ
फिर बनती कैसे पहचान मेरी?
माँ का दिल तो माँ का है
लड़का हो चाहे लड़की हो
दोनों उसके दिल के टुकड़े
कुदरत ने लक्ष्मी थी बख्शी
वो बनी थी मेरे दिल की खुशी
पर अपनों ने था नकार दिया
उसके कारण मुझ पर वार किया
मैं अंदर ही अंदर टूट गई
सारी खुशियाँ थी बिखर गईं
फिर बनती कैसे पहचान मेरी?
पर दिल मैंने नहीं हारा था
बेशक किस्मत ने मारा था
नहीं चूकी फर्ज निभाने से
किस्मत में लेकिन ताने थे
हर रिश्ते का निर्वाह किया
जीवन भर नहीं था आह किया
पग-पग पर निकलती हुई देखी
मैंने अभिलाषाओं की अर्थी
जिसे अश्रु-सुमन चढ़ा कर के
अपने हाथों ही विदा किया
यूँ बीत गया मेरा जीवन
और जग का कुछ न पता चला
फिर बनती कैसे पहचान मेरी?




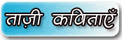




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
4 कविताप्रेमियों का कहना है :
इसके बाद तो पहचान बनाना शुरू होता है अभी तक माँ-बाप के साये में पली-बढ़ी बाहरी दुनिया में तो अब आगे निकलना हुआ....बहुत ही बढ़िया कविता एक सुंदर भावनात्मक अभिव्यक्ति...धन्यवाद अनिल जी!!
बहुत सुन्दर अभिव्यक्तु है कई दिन की अनुपस्थिति के लिये क्षमा चाहती हूँ । नये साल की बहुत बहुत बधाई।
"पग-पग पर निकलती हुई देखी
मैंने अभिलाषाओं की अर्थी
जिसे अश्रु-सुमन चढ़ा कर के
अपने हाथों ही विदा किया"
समसामयिक, संदेशवाहक भावपूर्ण एवं रचना - सामाजिक जाग्रति के लिए ऐसी रचनाओं की आज शख्त जरुरत है. डॉ॰ अनिल चड्डा जी का आभार और धन्यवाद्.
मेरी मुश्किल भी बढ़ती गई
इस जग में था बसता जंगल
मन में सबके था पशु छुपा
और आंखें भी लोलुपता से भरी
घर वाले थे परेशान बड़े
और मैं भी थी कुछ डरी-डरी
bahut sunder badhai
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)