तुमने इंसान को बख्शी तो थी जन्नत-सी ज़मीं...
हमने परिस्तिश के लिए बुत में तराशा तुमको....
तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया,
आह! हमने हर तरह बना डाला तमाशा तुमको.....
ये है मस्जिद मेरी, बसता है खुदाया मेरा,
और ये मंदिर है, मेरे राम यहाँ बसते हैं....
यहाँ होते हैं सबद, और ये गिरजाघर है,
एक ही मंजिल पे जाने के कई रस्ते हैं.....
एक ही दर को मजहब से कई नाम मिले,
मैं मुन्तजिर हूँ, कब अल्लाह के घर राम मिले....
मेरे मालिक, मेरे मौला, मुझे इतना तू बता,
खूँ के धब्बों में तेरा अक्स भी दिखता है क्या....
गर तेरी हाँ है, तो ले तलवार मैं उठाता हूँ !
जो न राम रटें, उनकी अब तो खैर नहीं....
और इधर से भी कुछ बलवाई चले आते हैं !
मेरे शहर के ही मुल्ला हैं, कोई ग़ैर नहीं...
एक भी घर न बचा, देखो सियासतदानों !
तुमने चाहा, वो हुआ, फख्र से सीना तानो,
तुमने जो आ रही नस्लों को विरासत में ज़हर बांटे हैं,
नफरत-ओ-ज़ुल्म के शामो-सहर बांटे हैं...
देखना, एक दिन तुम पर भी कज़ा आएगी,
वक़्त के कटघरे में तुम भी तो आओगे कभी...
बिक चुके खून की हर बूँद धिक्कारेगी तुम्हे,
साजिशें तुम्हारी ही इक रोज़ को मारेंगी तुम्हे....
निखिल आनंद गिरि
+919868062333




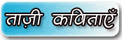




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
15 कविताप्रेमियों का कहना है :
एक भी घर न बचा, देखो सियासतदानों !
तुमने चाहा, वो हुआ, फख्र से सीना तानो,
तुमने जो आ रही नस्लों को विरासत में ज़हर बांटे हैं,
नफरत-ओ-ज़ुल्म के शामो-सहर बांटे हैं...
बहुत खूब
तुमने इंसान को बख्शी तो थी जन्नत-सी ज़मीं...
हमने परिस्तिश के लिए बुत में तराशा तुमको....
तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया,
आह! हमने हर तरह बना डाला तमाशा तुमको.....
शब्द नही हैं तारीफ के लिए............. बहुत खूब
तुमने इंसान को बख्शी तो थी जन्नत-सी ज़मीं...
हमने परिस्तिश के लिए बुत में तराशा तुमको....
तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया,
आह! हमने हर तरह बना डाला तमाशा तुमको.....
बहुत ही सही लिखी यह पंक्तियाँ आपने निखिल ..सच और सुंदर भाव हैं इसके .काश यह बात सब समझ पाते तो कोई झगडा ही क्यों होता !! शुभकामना के साथ
रंजू
निखिल जी इस रचना में आपने वर्तमान परिस्थिति पर सही कटाक्ष किया है.यूं तो बहुत सी रचनाएँ इस विषय पर पढीं.आप की रचना अच्छी लगी.ख़ास कर अन्तिम यह पंक्तियाँ-
देखना, एक दिन तुम पर भी कज़ा आएगी,
वक़्त के कटघरे में तुम भी तो आओगे कभी...
बिक चुके खून की हर बूँद धिक्कारेगी तुम्हे,
साजिशें तुम्हारी ही इक रोज़ को मारेंगी तुम्हे....'
कवि मन का आक्रोश साफ साफ झलक रहा है-
अपनी बात कहने में यह रचना पुरी तरह सफल रही -ऐसा मेरा मत है-बधाई-
nikhil bhai,apne akrosh ko bayan karne ka hunar to koi apse sikhe.
kaumi fasadon aur samajik vishamata ka jo aks apne ukera hai,wo qayamat hai.
ek jabardast kavita,
alok singh "sahil"
निखिल जी कविता ठीक है.
अगर थोडा और गहराई में जाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता?..
बहुत बढिया अक्स..
सुन्दर शब्द-योजन, सुन्दर चयन..
साधूवाद
एक ही दर को मजहब से कई नाम मिले,
मैं मुन्तजिर हूँ, कब अल्लाह के घर राम मिले....
मेरे मालिक, मेरे मौला, मुझे इतना तू बता,
खूँ के धब्बों में तेरा अक्स भी दिखता है क्या....
निखिल अब इससे आगे मैं की कहूँ, इतना मार्मिक है और इस कदर मन को चूती है ये पंक्तियाँ की शब्द कम पढ़ जाते हैं tareef के लिए, samvedaano को jaagaati एक utkrisht रचना
कविता पढ़कर टिपण्णी करने वालों को धन्यवाद....
अल्पना जी, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि धर्म के नाम पर जो नफरतें हम अपने दिलों में भर रहे हैं, उसे जड़ से ख़त्म किया जाए.....
रंजू जी, हिंद युग्म जैसा बड़ा सामूहिक मंच साम्प्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ बुलंद रखे, इसके लिए हम सदा प्रयासरत हैं...
अवनीश जी, एक कविता में इतनी गहराई ही रख पाया, आगे और कोशिश रहेगी..
nikhil anand giri
निखिल जी!
कोमल शब्दों में,नर्म तेवर में जो तीखा आक्रोश दिखाया है आपने,काबिले तारीफ़ है।
मुझे जिन लाईनों ने प्रभावित किया-
तुमने इंसान को बख्शी तो थी जन्नत-सी ज़मीं...
हमने परिस्तिश के लिए बुत में तराशा तुमको....
तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया,
आह! हमने हर तरह बना डाला तमाशा तुमको.....
मेरे मालिक, मेरे मौला, मुझे इतना तू बता,
खूँ के धब्बों में तेरा अक्स भी दिखता है क्या....
बिक चुके खून की हर बूँद धिक्कारेगी तुम्हे,
साजिशें तुम्हारी ही इक रोज़ को मारेंगी तुम्हे....
कविता में नयापन नहीं है। इसे और बेहतर ढंग से कहा जा सकता था। कविता थोड़ी लम्बी भी हो गई है।
एक और बात मुझे चुभी- कहीं तुकांत और कहीं अतुकांत कर देने से पाठक को कहीं कहीं निराशा भी होती है।
इस पर आपको और काम करने की आवश्यकता थी निखिल जी
कविता का शिल्प बहुत कमज़ोर है। काफ़ी वक्त से 'तुम सिखा दो', 'मैं मीडिया का एक छात्र' और क्षणिकाओं जैसी कविता नहीं पढ़ा रहे हैं आप।
निखिल जी
सर्वप्रथम अच्छी कविता के लिए बधाई.. मै ये बातें कहना चाहूँगा आपकी कविता के बारे मै
१) बहुत अच्छी संकल्पना के तहत कविता लिखी है अतः किवता की लय अंत तक बरक़रार है
२) उर्दू शब्दों का अच्छा पर्योग देखने को मिला है
३) अंत कविता का अच्छी तरह किया गया है की, इंसान को सच्चाई से रूबरू करवाया जाये..
एक दो बातें जिनको मै समझना चाहूँगा
१) शीर्षक कविता से किस तरह मिलता है.. क्या आप ये कहना छह रहे है की भगवान आप का ही रूप है?
२) "तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया," इस का मतलब नहीं समझ आया :(
३) कुछ सब्द जैसे "परिस्तिश" और कजा का मतलब भी नहीं समझ पाया ...
सादर
शैलेश
तुमने इंसान को बख्शी तो थी जन्नत-सी ज़मीं...
हमने परिस्तिश के लिए बुत में तराशा तुमको....
तुमने सोचा कि हम इन्सां बने सब के यहाँ सरमाया,
आह! हमने हर तरह बना डाला तमाशा तुमको.....
बहुत खूब अगर ये बात सबके समझ आती तो ये धर्म रूपी दीवार ही न होती...
maasha-allah !
"zameer ki suntein nahi, mazhab ki baat kya manegein . apne aks ko qaid kar, khud ko aazaad kehtein hai. "
ab, seedhe shabdo mein kahoo toh koshish lajawaab hai.
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)