वीराने में पत्थर से टकरा कर
लौटती हुई लहरें
मेरे मन के भीतर के
सूख चुके स्नेह से
धुवां धुवां बाती को
फूंक कर लाल तो करती है
लालिमा फिर सहमती है
धुवा और कसैला कसैला सा फैल जाता है
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल
ये कैसी क्षुधा थी कि
आग सीनें में आँखों में
और पलकों पर धर गयी
और ये कैसी सदा है
कि दिल की सारी तपिश पी कर भी
कहती है क्षुधा है क्षुधा है
मेरे मन के सूखे हुए सोतो
सुनो मरुस्थल का राग
वीरानियों में हवाओं का मृदंग
मैं कांप उठता हूं अपनें भीतर के व्योम की
घुटी घुटी चीखों के राग से
कहता है मुर्दे!! जाग रे! जाग रे!
मैं खमोश रहता हूँ
थक जाती है ध्वनि भी प्रतिध्वनि भी
लहरें लौट जाती हैं...
लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है
लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?
*** राजीव रंजन प्रसाद
१८.०४.१९९५




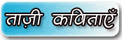




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
25 कविताप्रेमियों का कहना है :
पत्थर पिघलता हैै सही है, पर लहर भी तो उस पर टूटती है। टूटन तो दोनों ओर है फिर विरक्ति क्यों???
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल
यहां आत्मसात से क्या तात्पर्य
आत्मसात का अर्थ होता है मिलना। नदी किनारे आपने देखा होगा कि किस प्रकार लहरे पत्थरों से बाद-बार टकारती हैं जैसे पत्थरों के कण-कण के अस्तित्व को अपने में समाहित कर लेना चाहती हों और सम्भव पाषाण भी अपना कण-कण उन्हें सौंप देता है।
वैसे भाषाई दृष्टिकोण से आत्मसात किया जाता है, आत्मसात हुआ नहीं जाता। मगर कविताओं में भाषा के सभी नियम नहीं लगते।
राजीव जी, सुन्दर रचना है
लहरो का बार बार पाषाण किनारे से टकराना भी उसकी आसावादिता को दर्शाता है... कभी कभी पाषाण भी समुन्दर का एक हिस्सा बन जाते हैं लहरो के आवेग में बह कर.. और कुछ नही तो लहरें कुछ समय के लिये तो उस पाषाण पर छा जाती हैं
लहरें समुन्दर की हों या मन की इनका आना आशावादिता ही है..यही तो हमें झकझोर कर फ़िर से उठने और राह पर चलने के लिये प्रेरित करती हैं
"मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल"
"कांप उठता हूं अपनें भीतर के व्योम की
घुटी घुटी चीखों के राग से
कहता है मुर्दे!! जाग रे! जाग रे!"
राजीव जी,
आपका अन्तर्द्वन्द्व ऐसी अभिभूत कर देने वाली रचनाओं को जन्म देता है हमेशा
संवेदनशील हृदय से निकली अद्भुत कृति
साभार
गौरव शुक्ल
लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है
लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?
bahut khub........
कविता में एक सोच है..जो सोचने को विवश करती है..
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल
मैं खमोश रहता हूँ
थक जाती है ध्वनि भी प्रतिध्वनि भी
लहरें लौट जाती हैं...
मुझे इन पंक्तियों मे
लहरों के आत्मबल में
विरोधाभास लग रहा है
तथा
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
पहली बात तो यह्, जो सभी को,विशेषत: नये रचनाकारों को समझनी अनिवार्य है, कि कविता कोई शाब्दिक खेल नहीं होती है।केवल तत्सम शब्दों क प्रयोग करने मात्र से कविता की गुणवत्ता में अन्तर नहीं आता। तत्सम प्रयोगों में बहुत सावधानी बरतनी इस लिये आवश्यक है क्योंकि वे सामान्यत:प्रयोग में कम किये जाते हैं।जिस शब्द पर चर्चा हो रही है वह है-आत्मसात। इस का अर्थ होता है अपने में अपने को विलीन कर लेना या किसी चीज को स्वयम् में समाहित कर लेना ।जो कि इस संदर्भ में नितांत निरर्थक है। अर्थ कि अन्विति ही नहीं बैठ रही। कविता में अर्थ की भी एक लय होती है,शब्दों की भी। (लय का अर्थ तुक या ट्यून नहीं होता।यह विषय काव्यशास्त्रीय है सो बाद मे॥)
अत: पहली बात तो यह कि यह प्रयोग ही गलत है। दूर की कौडी लाने जैसा। पर इस से भी अधिक यह कि पानी वा अग्नि दो विरोधी तत्व हैं,इन का कोई सहसंबन्ध ही नहीं बनता। "विरुद्धों का सामंजस्य" के नाम पर कुछ को भी कुछ के साथ नहीं जोडा़ जाता। यह केवल शाब्दिक रस भी पैदा नहीं कर पा रही। अखर रहे हैं बहुत से प्रयोग। शब्दों को सार्थक रूप में, चामत्कारिक विधि से संजोने की प्रक्रिया होती है कविता। इस कविता पर अभी श्रम करने की काफ़ी जरूरत है।
मेरे मन के सूखे हुए सोतो
सुनो मरुस्थल का राग
वीरानियों में हवाओं का मृदंग
मैं कांप उठता हूं अपनें भीतर के व्योम की
घुटी घुटी चीखों के राग से
कहता है मुर्दे!! जाग रे! जाग रे!
राजीव जी कितनी सुन्दर है ये अभिव्यक्ति मगर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये भाव बस इस कविता तक ही सीमित रहे ..... आपके जीवन में कभी आशावादिता की कमी ना आये
"मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल"
क्या खूब लिखा है.. ऐसी पंक्तियाँ थके हुए आदमी के मन में नया जोश फ़ूक देती हैं..
पानी पत्थर को काट सकता है..इसी तरह की कुछ पंक्तियाँ हमने बचपन में भी पढ़ीं थीं.. "रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान"
प्रकृति से इतनी सब कुछ मिल सकता है सीखने को ये हम नहीं जानते.. अथाह ज्ञान भरा हुआ है..
" मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल "
आशा और जोश से भरी हैं ये पंक्तियाँ .. फिर अंत यह क्यों :
"लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?"
मेरे मन के भीतर के
सूख चुके स्नेह से
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल
मैं कांप उठता हूं अपनें भीतर के व्योम की
घुटी घुटी चीखों के राग से
कहता है मुर्दे!! जाग रे! जाग रे!
थक जाती है ध्वनि भी प्रतिध्वनि भी
लहरें लौट जाती हैं...
लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है
लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?
man ki aashavadita sada kayam rahe maula se yahi dua hai.well written
कविता एसी है कि पत्थर पिघल जाए।
गौरव
बहुत सुन्दर लिखते हो ।
किन्तु जीवन में कभी भी आशावादिता को
मरने मत देना । ऐसा होता है कभी- कभी ।
किन्तु एक कवि केवल कविता में दिल का दर्द
प्रकट करता है । अपनी जिजीविषा को कभी
मरने मत देना । एक कवि की सोच निराशा नहीं
आशा दे तो अचछा होगा । आशीर्वाद सहित
राजीव जी,
देरी से टिप्पणी के लिये क्षमाप्रार्थी हूँ. कविता को यदी अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी लगती है. शब्द-विशेष को लेकर तो शैलेष जी कह ही चुके हैं. इसके अलावा कविता किसी भाव विशेष को प्रकट करने के बजाय अलग-अलग और कुछ विरोधाभाषी बिंबों का समूह अधिक नजर आती है.
वीराने में पत्थर से टकरा कर
लौटती हुई लहरें
मेरे मन के भीतर के
सूख चुके स्नेह से
धुवां धुवां बाती को
फूंक कर लाल तो करती है
ये पँक्तियाँ स्नेह के ईंधन से जलते दीपक का बिंब दिखातीं हैं, वहीं अधोलिखित पँक्तियाँ आग के एक बिल्कुल अलग रूप को उकेरतीं हैं.
ये कैसी क्षुधा थी कि
आग सीनें में आँखों में
और पलकों पर धर गयी
ऐसे ही कुछ और बिंब भी कविता में नज़र आते हैं, जो कविता के प्रभाव को बढ़ाने की जगह कम करते प्रतीत होते हैं.
आशा है कि आप मेरी टिप्पणी को अन्यथा नहीं लेंगे. बेहतर की प्रतीक्षा में-
अजय यादव
राजीवजी,
कविता सुग्राही नहीं लग रही है, कुछ पंक्तियाँ एक दूसरे का समर्थन करती प्रतित नहीं होती, जैसे-
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते..
मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल
जहाँ पहली पंक्ति में आप पाषाण के आत्मसात होने का श्रेय लहरों के अनवरत समर्पण को दे रहें है तो वहीं दूसरी पंक्ति में आप लहरों के आत्मबल द्वारा पाषाण के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं।
हालांकि कविता के अंत में जाते-जाते आप अपने अंतर्द्वन्द को सामने लाने में कामयाब रहे हैं, बधाई स्वीकार करें।
इस रचना पर मैं कुछ भी कहने से पहले चाहूँगा कि खुद राजीव जी आकर अपनी बात को अच्छी तरह से हमें समझाएँ। शायद बहुत सारे पाठकगण इस रचना में छुपे भाव को समझ नहीं पा रहे या फिर आत्मसात [:)] नहीं कर पा रहे। मैं अपनी लेखनी को टिप्पणी करने से तबतक दूर रखूँगा जब तक राजीव जी से मैं इस रचना में छुपी अभिव्यक्ति न समझ लूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे।
राजीव भैया,
कविता जी से बिल्कुल भी सहमत नही, किन्तु कविराज जी से आंशिक समर्थित ।
किस शब्द को कहां लोखना चाहिये, मैं समझता हूँ, इस प्रकरण पर पहले भी चर्चायें होती रही है, और अंत में सार यही होता है कि कवि सर्व बन्धन मुक्त है, तो हमें इस सच को आत्मसात कर लेना चाहिये ।
और रही बात भावों की तो वे काफी अच्छे है और हमें अपनी ओर सहज ही आकर्षित करतें है ।
कुल मिलाकर रचना अपने मकस़द में कामयाब होती है, जो हर रचना के लिये एक आवश्यक है ।
अभिवन्दन स्वीकार करें ।
आर्यमनु
प्रिय तनहा जी..
आपके स्नेह से अभिभूत हुआ हूँ और न चाह कर भी स्पष्टीकरण देने पर बाध्य हुआ हूँ। जो समालोचनायें आयी हैं वह पूर्णत: दर्शा रही हैं कि रचना अपनी बात पूरी तरह पहुंचाने से चूक गयी है और विरोधाभास उत्पन्न करती है। तथापि मैं शब्दों के प्रकार में रचना को बाँधे जाने की वकालत नहीं करता। विरोधाभास पर मेरा अपना दृश्टिकोण है। कविता के आरंभ से इसे देखें:
लहरें केवल पाषाण को मार नहीं रहीं समाप्त नहीं कर रही अपितु उसके चेतनाशून्य हो जाने पर उसे जगाती भी हैं
"लौटती हुई लहरें
मेरे मन के भीतर के
सूख चुके स्नेह से
धुवां धुवां बाती को
फूंक कर लाल तो करती है"
पाषाण थक चुका है, लडने की जिजीविषा नहीं इस लिये
"लालिमा फिर सहमती है
धुवा और कसैला कसैला सा फैल जाता है
मैने देखा है कण कण पाषाण को
लहरों के अनवरत समर्पण पर आत्मसात होते.."
अब लहरों की हताशा भी है कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ....और पाषाण की चेष्टा भी है कि अब बस बहुत हुआ...आत्मसात हो लू....
"लहरों का समर्पण" और "चट्टानों का आत्मसात होना" ही तथ्य को मेरे अनुसार काव्यात्मक करता है, यह विरोधाभास ही वह अलंकार है जिससे मेरे अनुसार ये पंक्तियाँ कविता की परिभाषा में आती हैं।
क्योंकि आगे की पंक्तियाँ उसी बात को विस्तार देती हैं
और ये कैसी सदा है
कि दिल की सारी तपिश पी कर भी
कहती है क्षुधा है क्षुधा है
मेरे मन के सूखे हुए सोतो
सुनो मरुस्थल का राग
वीरानियों में हवाओं का मृदंग
मैं कांप उठता हूं अपनें भीतर के व्योम की
घुटी घुटी चीखों के राग से
कहता है मुर्दे!! जाग रे! जाग रे!
कि अभी कहीं दबे..चट्टान सांसे ले रहा है, सोच की सांसे चल रहीं हैं। इसी लिये:
"लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है"
तनहा जी, रचना मैंने 18.04.1995 में लिखी थी। मुझमें परिपक्वता की कमी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी टिप्पणी की मुझे प्रतीक्षा है।
*** राजीव रंजन प्रसाद
सबसे पहले तो इतनी देरी के लिये क्षमाप्रार्थी हूं।
मेरे उपद्रवी इंटरनेट के चलते यह देरी हुई और आंशिक रूप से मेरा आलसी स्वभाव भी जिम्मेदार रहा। हालांकि पढ़ तो मैंने उस दिन ही ली थी।
जैसा आप खुद कह रहे हैं राजीव जी, कुछ परिपक्वता की कमी मुझे भी लगी थी। लेकिन फिर पढ़ा तो लगा कि ये अपरिपक्वता नहीं है, बस एक समय में कुछ विरोधाभासी से भावों की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन यह तो कविता का नियम नहीं है कि उसमें एक जैसे भाव ही झलकें।
कविता आप के वर्तमान जितनी सुन्दर तो नहीं बन पाई है पर फिर भी बहुत अच्छी कविता है..विशेषकर अंत
लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है
लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?
शैलेश जी,
"वैसे भाषाई दृष्टिकोण से आत्मसात किया जाता है, आत्मसात हुआ नहीं जाता।"
अपने इस कथन से सम्बन्धित कोई प्रमाण दे सकते तो बड़ी कृपा होगी,वैसे आत्मसात शब्द और उस पर आपका भाषाई दृष्टिकोण। आपको भाषाविद कहने का जी चाहता है खैर बाकी बातें एक तरफ़ मेरा थोड़ा ज्ञानवर्द्धन हो जायेगा........
राजीव रंजन
आपकी कविता बहुत सुन्दर है । मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना विवाद किस लिए है ।
कविता क्षणिक आवेग होता है । यदि दिमाग खुरच- खुरच कर ही लिखना है तो मैं उसे
कविता नहीं मानती । अचछा आलोचक वह होता है जो कवि की मनःस्थित को समझे
और उसका आनन्द कविता समझकर ही ले । कविता में मुझे कोई कमी नहीं लगी ।
शुभकामनाओं सहित
राजीव जी , क्षमाप्रार्थी हूँ मैं। आपसे स्पष्टीकरण माँग कर मैं खुद गायब हो गया , इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। मैंने आपकी टिप्पणी पढने के बाद सोचा था कि आराम से टिप्पणी करूँगा और आराम हीं करता रह गया।[:(]
आपकी लेखनी पर मुझे कभी भी अपरिपक्वता का अंदेशा नहीं रहा। बस अपने मित्रगण के संदेह को देखकर आपसे स्पष्टीकरण माँग बैठा।
"मैने देखा है पाषाण का अस्तित्व छीन लेती
लहरों का आत्मबल"
"मेरे मन के सूखे हुए सोतो
सुनो मरुस्थल का राग
वीरानियों में हवाओं का मृदंग"
"लहरें पुनः लौटती हैं नयी जिजीविषा लिये
चट्टान के मोम होनें की प्रक्रिया जारी है"
इन पंक्तियों में आपने लहरों और पत्थर के बीच की कशमकश दीखाकर जिंदगी की सच्चाई को दर्शाया है।
"लेकिन मेरे मन की आशावादिता क्यों मर गयी?"
लहरों से लड़कर भी अगर आशावादिता मरती है, तो पत्थर के हौसलों को कौन बचाए?
बहुत हीं खूबसूरत लिखा है आपने।
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)