सड़क किनारे हरे-भरे पेड़ों के बीच,
खड़ा मैं ठूँठ,
सोचता हूँ ,
कभी मुझे पर भी हरियाली होती थी ,
मेरी शाखें भी पवन की गुदगुदी से मचलती थीं
मुझ पर भी पत्ते खिलते थे,
पंछियों के काफ़िले मुझ पर भी आ कर रुकते थे ,
पर न जाने क्या हुआ !
शायद हवा ही ज़हरीली हो गयी !
या किसी की नज़र लग गयी
खड़ा हूँ, दुबला-सा बिना पुष्प ,पत्र
जैसे कोई फ़िल्मी तारिक़ा और उसके आधुनिक वस्त्र
मैं,
निर्वस्त्र, अशक्त ,
खड़ा हूँ, पेड़ों से मिट्टी पकड़े,
मिट्टी जिसमे नमी कम ,
ज़्यादा है कड़वी यादें
जाने क्या-क्या देखा है,
पर मैं निर्लज्ज,
खड़ा हूँ आज भी,
अविचल, मिटता ही नहीं
मुझसे टकराकर जब वो वाहन पलटा था ,
ओह ! उस बच्ची का कितना करूण रुदन था !
कैसी जी होगी बिन माँ-बाप के ?
वो अधूरापन ,
ज़िम्मेदार शायद मैं ही था !
मैं साक्षी हूँ उन लम्हों का ,
जब उन्होंने डकैती की योजना बनाई थी ,
लूट लिए थे सारे ज़ेवर,
उस मासूम की बारात वापस लौटवाई थी
सच मेरी छाया भी पापी है ,
जो ऐसे अधमों के काम आई थी
मैने देखा है ,
सड़क बनते हुए ,
फिर उखड़ते हुए, मरम्मत होते हुए ,
और फिर उखड़ते हुए ,
कारण? उस लोभी ठेकेदार ने रेत थोड़ी ज़्यादा मिलाई थी
मैने देखा है, वो सूखी लकड़ी के लिए भटकता आदमी ,
उसकी बीवी को लकवा मार गया था ,
बच्ची बुख़ार से तप रही थी ,
और वो भूखी रूह !
बेचारी जंगल में लकड़ी के लिए भटक रही थी !
उसकी झोंपड़ी की दरारों से झाँकती दरिद्रता ,
मेरी आत्मा को छेद जाती थी,
उस परिवार के करूण कराहों को सुन,
मुझ ठूँठ को भी नींद नही आती थी
मेरे पीछे बनी वो पीर-बाबा की मज़ार ,
वहाँ से लोभान की बड़ी पाक गंध आती थी
कुछ चमत्कार था शायद वहाँ ,
जुम्मेरात के दिन अकसर भीड़ लग जाती थी
पास का हेंडपंप ,
जून में भी नहीं सूखता था ,
बावरा था या शायद नादान,
छूत-अछूत का भेद भी नहीं समझता था !
सबका गला तर करता था, सबको बराबर सुकून देता था
मैने सुनी है, वो दबी सी घुटी हुई आवाज़ !
जो उस रात उस कार से आ रही थी ,
एक असहाय युवती,
उन दरिंदों के बीच छटपटा रही थी
मैं कोस रहा था ख़ुद को,
अपनी जड़ता को, शिथिलता को .
हे ! ईश्वर मुझे बस थोड़ी देर के लिए गति दे दे ,
अरे पत्थर दिल पसीज़ जा !
अब और मैं नहीं देख सकता यह सब,
चल, मेरी आँखे ही हमेशा के लिए बंद कर दे
ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं ,
गति है, दुरुपयोग करना चाहते हैं
हे विधाता ! सुन ,
बहुत कुछ दिखाया तूने,
मैने बहुत कष्ट झेले ,
रहम कर ....
एक आरज़ू सुन ले ,
कुछ भी करना, नर्क में डलवाना ,
पर एक ही तमन्ना है,
बस मुझे कभी इंसान मत बनाना !!




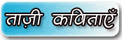




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
12 कविताप्रेमियों का कहना है :
विपुल जी..
आपके ठूंठ नें मन हरा कर दिया। एक आदर्श नयी कविता। यह बिम्ब तो बेहद अनूठा है:
"खड़ा हूँ, दुबला-सा बिना पुष्प ,पत्र
जैसे कोई फ़िल्मी तारिक़ा और उसके आधुनिक वस्त्र"
चित्र खीचने में आप पारंगत है,आपके शब्द चयन भी सटीक हैं। कविता का अंत आपके एसे सवालो के साथ किया है जिसका उत्तर शायद ही मिल सके:
"ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं"
"एक आरज़ू सुन ले ,
कुछ भी करना, नर्क में डलवाना ,
पर एक ही तमन्ना है,
बस मुझे कभी इंसान मत बनाना !!"
वाह!!! आपसे एसी रचनाओं की ही अपेक्षा है।
*** राजीव रंजन प्रसाद
ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठूँठ नही, हिन्दुस्तान अपनी ज़िन्द़गी की कहानी कहता हो ।
यह क्रन्दन सिर्फ उस ठूँठ का नही वरन् हरेक भारतवासी का है, जो रोज़ लुटता है, अपनो के ही हाथों से, फिर भी रोज़ मार सहता है, फिर से ।
बस मुझे कभी इंसान मत बनाना॰॰॰॰॰कहकर लेखक ने एक यक्ष प्रश्न पाठकों के सामने रखा है ।
लेखक ने ठूँठ के माध्यम से कई बार समाज के अन्दर की मार को बाहर प्रदर्शित किया है ।
अंत मे तो कवि ने ज़माने भर का दर्द सामने लाकर रख दिया है ।
कहीं कहीं रचना में पद्य कम और गद्य प्रयोग अधिक महसूस हुआ लगता है ।
पर फिर भी पूर्ण-रुपेण काव्य रचना अच्छी बन पडी है ।
बहुत बहुत अभिवन्दन ।
आर्यमनु
This must have required a very deep thinking of long hours, its really ammmmazzzzing !!!!!!
Keep it up
बहुत खूब विपुल।
एक खूबसूरत कविता।
जैसे कोई फ़िल्मी तारिक़ा और उसके आधुनिक वस्त्र
खड़ा हूँ आज भी,
अविचल, मिटता ही नहीं
मैं साक्षी हूँ उन लम्हों का ,
जब उन्होंने डकैती की योजना बनाई थी ,
लूट लिए थे सारे ज़ेवर,
उस मासूम की बारात वापस लौटवाई थी
सच मेरी छाया भी पापी है ,
जो ऐसे अधमों के काम आई थी
ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं ,
गति है, दुरुपयोग करना चाहते हैं
हर पंक्ति सीधे दिल से निकली हुई...
लिखते रहो।
poem is telling a story itselff.....
ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं ,
गति है, दुरुपयोग करना चाहते हैं
but u can improve it with gatyatmakta.....
i think..
its nt ur style............
m i right vipul....
if u do it...
no one can defeat u...
wishes...
piyush pandya
विपुल जी,
कविता का भाव-पक्ष बेहद सशक्त है और मर्म पर चोट करता है. आपने ठूँठ के माध्यम से समाज की विसंगतियों और मानव की हृदयहीनता पर करारा प्रहार किया है. विशेषत: अंतिम पँक्तियों में जाकर कविता बेहद मार्मिक हो जाती है.
इन सब खासियतों के बावजूद कविता में कहीं कहीं पद्यात्मकता का अभाव खटकता है. इस दिशा में कुछ मेहनत करके आप इसे और भी बेहतर बना सकते हैं.
सुंदर रचना के लिये बधाई.
--अजय यादव
विपुल जी आप अपनी बात कहने में सफल हुए हैं। मुझे पद्यगत या गद्यगत कोई भी शिकायत नहीं है आपसे। हाँ शुरू में कविता की लंबाई देखकर मुझे डर लगा था की कहीं भटक न गए हों आप, लेकिन पूरी रचना ने लय को थामे रखा है। बहुत हीं लुभावने एवं हृदयस्पर्शी बिंब प्रयोग किए हैं आपने।
राजीव जी ने सही हीं कहा है कि इस रचना को पढने के बाद हमें आपसे अपेक्षाएँ बढ गई हैं।
कविता में इससे अधिक गंभीरता क्या होगी। बहुत कम कवि मानवीकरण अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग कर पाते हैं। जिस तरह का रूपक आपकी कविता में दिखता है उससे आपमें संभावनाओं का क्षितिज बड़ा हो जाता है। जेसे-
ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं ,
गति है, दुरुपयोग करना चाहते हैं
काव्य की परिभाषा और उसके गुणधर्म के बारे में छोटे से बताया जाता है कि कविता में दो तरह की सुंदरता है एक बाह्य (जिसमें अलंकार, लयात्मक गति आदि आते हैं) और दूसरा आंतरिक (जिसमें रस, भाव, सरोकार इत्यादि तत्व सम्मिलित हैं)। मतलब आपकी कविता को आतंरिक सौंदर्य में १० में ९ अंक दिया जाय तो गलत नहीं होगा।
विपुल बेहद अनूठी शैली है रचना की...
अच्छा लगा पढ़्कर...
मगर पेट की भूख सब से बडी होती है
जान पर बन आती है जब उठ खडी होती है
पेट पीठ से सट कर
दिमाग सब बातों से ह्ट कर
सिर्फ़ रोटी और रोटी से चिपक जाता है
बधाई...
शानू
विपुल जी..
कभी मुझे पर भी हरियाली होती थी ,
मेरी शाखें भी पवन की गुदगुदी से मचलती थीं
मुझ पर भी पत्ते खिलते थे,
पंछियों के काफ़िले मुझ पर भी आ कर रुकते थे
.....
ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं ,
गति है, दुरुपयोग करना चाहते हैं
और इस पंक्तियों के बीच पंक्ति-दर-पंक्ति कवि की अचूक गरुण-दृष्टि... सबकुछ सराहनीय है।
मुशीं प्रेमचन्द की कहानी आम का ठूंठ की याद ताजा हॊ गई पर यह ठूंठ उससे अलग है।
"ठूँठ हूँ पर सोचता हूँ ,भावनाएँ हैं ,
उन अरबों चलते फिरते ठूँठो सा नहीं ,
जो बस ज़िंदगी से क़दम मिलाकर दौड़ते चले जाते हैं"
रचना सचमुच काबिले तारीफ है।
प्रतीकों के सहारे जीवन के यथार्थ को बेहतरीन तरीके से छुआ है आपने । साधुवाद एक सार्थक रचना के लिए
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)