मैं ,चाँद तुम्हारा,
देखता हूँ रोज़-
काले आसमान में
टंगी नीली बिन्दी को;
जो लगती है,
दुनिया समेटे,
दुलहन किसी की ।
जाने
कौन छोड़ गया है
बेचारी को,
जाने किस
काली स्लेट पर
टिमटिमाने को !
पता नहीं,
मैं कैसा लगता हूँ
दूर से-
हो कोई दर्पण
तो देखूँ
सूरत अपनी भी ।
और तुम भी
जाने क्यों
समझते हो मुझे
दर्पण-
हर घड़ी
चाहते हो,
दिखाऊँ
चेहरा
किसी का-
भ्रम है तुम्हारा,
इधर तो
सब ओर
पड़ी है धूल,
और पड़ा है-
वीराना ।
बनानेवाले ने भी
बना डाले
मेरी तरह के
सब टुकड़े,
अकेले,
अपनी तरह के-
बेजोड़-
और , कुछ टुकड़ों में
तुम जैसे,
जोड़ियाँ खोजने वाले,
हम टुकड़ों की आँखों से,
जिनका खुद का
जोड़ा
बना ही नहीं ।
रोज़ सुबह
जब उगती है
नीली वाली बिंदी
मेरे अंतरिक्ष में-
तो
सोचता हूँ,
दिखा डालूँ
चेहरे
जितने हो सकें ,
तुम्हारी दुनिया
डूबने से पहले ।
- आलोक शंकर




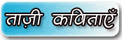




आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
11 कविताप्रेमियों का कहना है :
आलोक जी!
तीन बार पढ़ने पर भी मैं इस कविता के गूढ़ अर्थों को नहीं समझ सका। फिर भी जो समझा हूँ उससे यह समझ पाया कि यहाँ पर मेरे मित्रों द्वारा मेरे आसक्त होने की शंका को कविता रूप में कवि ने खूब लिखा है-
और तुम भी
जाने क्यों
समझते हो मुझे
दर्पण-
हर घड़ी
चाहते हो,
दिखाऊँ
चेहरा
किसी का-
भ्रम है तुम्हारा,
इधर तो
सब ओर
पड़ी है धूल,
और पड़ा है-
वीराना ।
और स्त्री-पुरूषानुपात के कम होने से शायद भारतीय युवाओं में एक तरह का असंतोष को कवि ने खूब महसूस किया है-
बनानेवाले ने भी
बना डाले
मेरी तरह के
सब टुकड़े,
अकेले,
अपनी तरह के-
बेजोड़-
और , कुछ टुकड़ों में
तुम जैसे,
जोड़ियाँ खोजने वाले,
हम टुकड़ों की आँखों से,
जिनका खुद का
जोड़ा
बना ही नहीं ।
और यहाँ पर युवा मन की आंतरिक प्रतिज्ञा
रोज़ सुबह
जब उगती है
नीली वाली बिंदी
मेरे अंतरिक्ष में-
तो
सोचता हूँ,
दिखा डालूँ
चेहरे
जितने हो सकें ,
तुम्हारी दुनिया
डूबने से पहले ।
कुल मिलाकर इस कविता से हो सकता है बड़े-बूढ़े भले ही न इत्तफ़ाक रखें, परन्तु मेरे लिए यह अकाट्य सत्य है।
आलोक जी आप बधाई के पात्र हैं।
सुन्दर रचना..प्रकृति का परिवेश लिये हुये
जो आशय मुझे समझ आया वो यह है कि चांद नीचे धरा को देख कर कह रहा है "आसमान में टंगी नीली बिन्दी"
साथ ही उसे अफसोस है कि वो खुद आसमान में अकेला है और अपना रूप भी स्वंय नही जानता क्योकि कोई बताने वाला ही नही है
वह यह जान कर भी दुखित है कि दुनिया उसे इतना उजला समझती है जब की व धूल से अटा पडा है
जिन टुकडों का जिक्र कवि कर रहा है वह है अन्य ग्रह, सितारे, सूरज आदि जो अपने में विशाल हैं परन्तु नितांत अकेले हैं
परन्तु मेरे हिसाव से अन्त में "रोज सुबह जब उगती है" कि जगह रोज शाम को जब उगती है" होना चाहिये क्योंकि चांद और धरा शाम के पहर ही मिलते है
बाकी आलोक जी बेहत और सही व्याख्या कर सकते हैं
कविता के गूढ़ार्थ के विषय में तो निश्चय ही आलोक जी ही सबसे बेहतर बता सकते हैं। परंतु कविता निस्संदेह बहुत सुंदर है, तथा आपने आप में कई अलग अलग अर्थ संप्रेषित करने में समर्थ है। इनमें से एक अर्थ शैलेष जी ने भी निकाला है, जो कविता को एक सर्वथा नया रूप प्रदान करता है। यह कविता निश्चय ही कवि की प्रतिभा को पूरी तरह सामने लाने वाली है। ऐसी सुंदर और बहुआयामी रचना के लिये आलोक जी को साधुवाद।
आलोकजी सबसे पहले तो बधाई स्वीकारें!
शैलेशजी, मोहिन्दरजी और अजयजी अपनी-अपनी समझ के अनुरूप भावार्थ खोज रहें है, यह सुखद है। कवि के विचारों को समझ पाना शायद इतना आसान नहीं है।
पता नहीं,
मैं कैसा लगता हूँ
दूर से-
हो कोई दर्पण
तो देखूँ
सूरत अपनी भी ।
वाह! मन की पीड़ा का बखूबी वर्णन किया है आपने यहाँ पर.. सम्पूर्ण कविता पसंद आयी।
बेहतर होगा यदि आलोक जी स्वयं ही सही भाव हमें समझायें। कविता अच्छी लगी।
घुघूती बासूती
बनानेवाले ने भी
बना डाले
मेरी तरह के
सब टुकड़े,
अकेले,
अपनी तरह के-
बेजोड़-
और , कुछ टुकड़ों में
तुम जैसे,
जोड़ियाँ खोजने वाले,
हम टुकड़ों की आँखों से,
जिनका खुद का
जोड़ा
बना ही नहीं ।
बहुत ही गहरी और सुंदर भाव लिए हुए है यह कविता
मुझे यह पंक्तियाँ विशेष रूप से पसंद आई !!
मैनें जिस भाव से कविता लिखी थी उसको मोहिन्दर जी ने बखूबी पकड़ा पर शैलेश जी ने अर्थ को एक नया आयाम देकर और ही रंग जमा दिया … कविता जहाँ भी जैसे भी स्वीकार हो , असर करे तो अपना उद्देश्य पूरा करती है ।
"मैं ,चाँद तुम्हारा,……………………सूरत अपनी भी ।"
यहाँ तक तो मोहिन्दर जी ने बयान कर दिया ।
आगे ……
"और तुम भी……………वीराना ।"
यहाँ चाँद कहता है धरती पर रहने वाले हम लोगों से … कि तुम मुझे दर्पण समझ बैठे हो और जब चाहो मुझमे अपने प्रिय का चेहरा देखना चाहते हो … मेरी सतह , मेरे हालात में आकर देखो - यहां सिर्फ़ धूल और वीराना पड़ा है … मैं कोई दर्पण नहीं ।
"बनानेवाले ने भी………बना ही नहीं ।"
अब चाँद ईश्वर से कहता है… कि तुमने जो अपने अंतरिक्ष में ये सारे पिण्ड बना रखे हैं … उनकी हालत भी तो कुछ मेरी तरह ही होगी , उनका अकेलापन भी मेरी तरह होगा और उनपर भी होगा बोझ उम्मीदों का , उनकी उम्मीदों का जो हमें आईना समझ अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं … हमारे लिये तो तुमने कोई जोड़ा बनाया ही नहीं ।
रोज़ सुबह
जब उगती है
नीली वाली बिंदी
मेरे अंतरिक्ष में-
तो
सोचता हूँ,
दिखा डालूँ
चेहरे
जितने हो सकें ,
तुम्हारी दुनिया
डूबने से पहले ।
जैसे धरती के लोग सूरज और चाँद को उगता देखते हैं वैसे ही मैं धरती को ,जो नीली बिन्दी की तरह दिखती है, उगते हुए देखता हूँ और सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जो मुझमें अपना सुकून ढूँढते हैं , मुझे दर्पण समझकर । … चाँद सोचता है कि मैं धरती के विरह वेदना से पीड़ित लोगों को उनके प्रिय को दिखाने वाला दर्पण लगता हूँ , तो जितने हो सके उतने लोगों को चैन दे डालूं ,जितने हो सके उतने चेहरे दिखा डालूँ ,इस से पहले कि यह जो धरती/पृथ्वी(दुनिया) उगी जा रही है आसमान में, डूब जाये । या ,उन लोगों के उम्मीदों की दुनिया डूब जाये ।
आलोक जी मैं क्या कहूँ, कई बार पढा और कई अर्थ निकाले..अपने आप से शिकायत है कि समझ नहीं सका..मोहिन्दर जी और आपकी व्याख्या नें मुझे कविता कुछ हद तक समझने में मदद की। आप निस्संदेह अच्छे कवि हैं, व्याख्या पढ कर आपके सुन्दर दर्शन को समझ सका। बधाई..
*** राजीव रंजन प्रसाद
और तुम भी
जाने क्यों
समझते हो मुझे
दर्पण-
हर घड़ी
चाहते हो,
दिखाऊँ
चेहरा
किसी का-
भ्रम है तुम्हारा,
इधर तो
सब ओर
पड़ी है धूल,
और पड़ा है-
वीराना ।
बड़ी हीं सुंदर एवं सुगढ कविता है। जगत के सत्य को प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से दर्शाती है। हिन्द युग्म को आपके रूप में एक बड़ा हीं होनहार कवि मिला है।
बधाई स्वीकारें।
pata nahi mein kaisa lagta hoon door se
ho koi darpan to dekhoon surat apni bhi
bahut hi sunder tareeqe se apni baat kahi hai alok ji aapne .chand mera favt. topic hai .bahut khoob ,lajawab.per thodi si kathin lagi pedhne mein.aap likhte rahein chand per ,hum zaroor padhenge.
thanks alok ji
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)