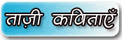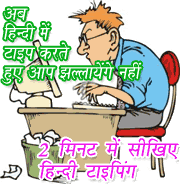याद आए दुष्यंत - प्रेमचंद सहजवाला
 |
| दुष्यंत कुमार |
|---|
मैं कमलेश्वर द्बारा संपादित 'सारिका' पत्रिका के उस विशेषांक को देखकर मानो दीवाना सा हो गया. कमलेश्वर ने एक कवि दुष्यंत कुमार की कई ग़ज़लें उस विशेषांक में छापी थी. मित्र ने पूछा - दुष्यंत कुमार नाम पहले कभी सुना था?
मैं साहित्य में अपने दायरे में सब से उत्साहित व्यक्ति माना जाता था. हर नाम बर-ज़बानी याद रहता था. कहानी लिखने में कुछ नाम भी कमा चुका था. पर दुष्यंत कुमार के बारे में मैंने मित्र से अबोधता से कहा - मैंने तो केवल शकुंतला वाले उस राजा दुष्यंत का नाम सुना है जिस ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी और शकुंतला से वह अंगूठी नदी में गिर गई थी..
मित्र ठहाका मारकर हंस पड़ा. पर सोनीपत शहर के जितने भी उत्साहित नौजवान साहित्यकार थे, मैंने देखा की सारिका के उस विशेषांक के बाद इस नाम के दीवाने से हो गए हैं. कमलेश्वर ने हर ज़बान को दुष्यंत के शेर याद करवा दिए. वह बहुत मज़ेदार ज़माना था सचमुच. कोई मित्र हाथ मिलाते ही कह उठता था -
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए.
सब के एक दूसरे से मिलने का स्टाइल ही बदल गया. मिल कर बैठते थे तो एक-दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते थे, बस अपनी ही रौ में बोलते जाते थे. कोई कहता था इमरजेन्सी की पूरी पहचान एक ही शेर में -
दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो
उनके हाथों में है पिंजरा उन के पिंजरे में सुआ
सचमुच, व्यवस्था के हाथों में सख्त और कड़े पहरे वाले कई पिंजरे थे. उनमें कैद तोते दूरदर्शन पर आ कर कहते थे - बीस सूत्रीय कार्यक्रम देश के लिए सर्वोत्तम कार्यक्रम है - और इस परिस्थिति के लिए दुष्यंत का शेर था -
जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें
हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं.
दुष्यंत कुमार की कई ग़ज़लें इंदिरा गाँधी की निर्मम व्यवस्था पर करारा प्रहार करती थी. उन्हीं दिनों 'सारिका' के सम्पादकीय पृष्ठ 'मेरा पन्ना' में कमलेश्वर, व 'कहानी' पत्रिका के संपादक श्रीपतराय अपने संपादकीय में कमोबेश एक ही बात लिखते थे कि असली साहित्यकार वही है जो अपने समय की नब्ज़ हाथ में पकड़ कर उसकी पहचान रख सकता है. निर्मल वर्मा कहते थे कि जैसे कटीली झाडियों में कोई कबूतर फंसा है और उसे बाहर निकाल कर लोगों को दिखाने में हाथ लोहू लुहान हो जाता है, वैसे ही सच्चाई को कागज़ पर उतारने में व्यक्ति को पूर्णतः छिल जाना पड़ता है.
दुष्यंत कुमार केवल व्यवस्था के विरुद्ध ही एक बगावत का स्वर ले कर नहीं उभरे, वरन उन्होंने तो तकनीकी तौर पर हिन्दी ग़ज़ल को मान्यता तक न देने या उसे हीन कह डालने की धृष्टता करने वालों को दो टूक जवाब दिए. ग़ज़ल बेहद अनुशासित विधा है. माना. उसमें मतला, काफिया, रदीफ़, बह्र (छंद) व रुक्न को लेकर कई शायरों की खूब मारामारी चलती रहती है. पर जब दुष्यंत कुमार की ग़ज़लों में 'शहर' नहीं 'शह्र ' लिखना चाहिए आदि जैसी बातें कह कर उन्हें टोका गया, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि आप हमारे 'ब्रह्मण' शब्द को 'बिरहमन' बना सकते हैं, 'ऋतु' को रुत, तो हम 'शह्र' को 'शहर' क्यों नहीं लिख सकते. अपने सर्वाधिक व सर्वप्रसिद्ध दीवान 'साए में धूप' (प्रकाशक 'राधाकृष्ण' नई दिल्ली) की भूमिका रूप लेख 'मैं स्वीकार करता हूँ...' में वे कहते हैं कि 'इन शब्दों का प्रयोग यहाँ अज्ञानता वश नहीं जानबूझ कर किया गया है. यह कोई मुश्किल काम नहीं था कि 'शहर' की जगह 'नगर' लिख कर इस दोष से मुक्ति पा लूँ, किंतु मैं ने उर्दू शब्दों का उस रूप में इस्तैमाल किया है जिस रूप में वे हिन्दी में घुलमिल गए हैं'. इस का अर्थ कि दुष्यंत कुमार ने, बोलचाल की भाषा को ही उचित मानदंड बनाया. मुझे एक साहित्यकार ने एक बार एक रोचक बात कही थी कि भाषा वह नहीं जो विद्वान् बनाते हैं बल्कि भाषा वह जो लोग बोलते हैं. इसीलिए दिल्ली का 'नारायण विहार' बन गया नरैना और 'कर्मपुर' बन गया 'करम पुरा'! वैसे अंग्रेज़ी के कवि तो यह भी मानते हैं कि कविता में rythm के लिए शब्द का उच्चारण भी बदला जा सकता है.
वैसे दुष्यंत कुमार ने कुछ नगण्य संख्या की ग़ज़लों में कुछ ज्यादा अति-क्रमण भी किया है. जैसे:
भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ,
आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दआ
गिड़गिडाने का यहाँ कोई असर होता नहीं
पेट भर कर गालियाँ दो आह भर कर बद-दुआ
इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो
जब तलक खिलते नहीं हैं कोयले देंगे धुआँ
इस ग़ज़ल में बार बार रदीफ़ बदलता है. पर ऐसा बहुत ज़्यादा ग़ज़लों में नहीं है.
दुष्यंत की ग़ज़लों की मूलतः दो उपलब्धियां रहीं. एक तो यह कि उन्होंने शायरी को मुल्क से जोड़ा और मुल्क की हालिया परिस्थितियों पर शायर की नज़र केंद्रित की. ऐसा नहीं है कि उससे पहले राष्ट्रीय काव्य लिखा ही नहीं गया. दिनकर जैसे राष्ट्र कवि रहे और आजादी के संघर्ष के समय रामप्रसाद बिस्मिल जैसे शायर रहे जो 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है' जैसी अमर ग़ज़लें लिख गए. कई देशभक्ति से ओत-प्रोत कवितायें भी लिखी गई. पर दुष्यंत ने इस मुल्क की व्यवस्था के सामने आदमी की बबसी को इतना सशक्त और चुभने वाला स्वर दिया जो उससे पहले नहीं दिया गया और न ही उतनी चीर कर रख देने वाली पंक्तिया कोई उन के बाद दे पाया. देश में गरीबी व्याप्त है, आम आदमी की तस्वीर उन से अच्छी कौन खींच सकता है भला:
कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए
कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए
देश की आज़ादी के बाद के मोह भंग की स्थिति:
खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को,
सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए
और फिर इस बेबसी और लाचारी के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्वर काट दिए गए, इसीलिए:
लहू लुहान नजारों के ज़िक्र आया तो,
शरीफ लोग उठे दूर जा के बैठ गए.
पर दुष्यंत की मुठियाँ भिंचती हैं और वे कहते हैं:
सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक्सद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए.
दुष्यंत प्रेरणात्मक स्वर भी उभारते हैं:
जियें तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले ,
मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए.
(गुलमोहर देश के उस गौरव का प्रतीक है, जो शायद समस्याओं के बावजूद हर भारतीय महसूस करता है).
वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, दीक्षित दनकौरी द्वारा संपादित व मोईन अख्तर अंसारी द्वारा संकलित वृहद् संग्रह 'ग़ज़ल-दुष्यंत के बाद' के एक भूमिकात्मक लेख 'दुष्यंत एक युग का नाम है' के लेखक अनिरुद्ध सिन्हा लिखते हैं: 'दुष्यंत कुमार एक युग का नाम है, जहाँ से हिन्दी ग़ज़ल की विकास यात्रा आरम्भ होती है'. यह दुष्यंत कुमार की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अनिरुद्ध यह मानते हैं कि ग़ज़ल मूलतः हिन्दी की विधा नहीं है, वरन उसे उर्दू से उधार ले कर हिन्दी में स्थापित किया गया है. पर इस इमारत को सब से अधिक मजबूती किस ने प्रदान की? दुष्यंत ने ही. कोई ज़माना था कि हिन्दी पर ज़ोर देने वालों को निम्न उदाहरण दिया जाता था:
गालिब का एक शेर है:
उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक,
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है.
अब ज़रा इसे शुद्ध हिन्दी में लिख कर देखें तो शेर एक प्रकार से बेहोश ही हो जाता है:
उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर शोभा,
वो समझते हैं कि रोगी की दशा अच्छी है.
उपरोक्त व्यंग्य अपनी जगह जायज़ है. ठेठ हिन्दी शब्दों से गालिब के शेर का असर ही जाता रहा. पर दुष्यंत ने उर्दू के सटीक से सटीक शब्दों का उपयोग कर के हिन्दी ग़ज़ल को मजबूती प्रदान की. दोनों भाषाओँ के शब्द आपस में गुत्थम गुत्थ कर के एक ही खजाना सा बन जाता है तो क्या हर्ज़ है. जहाँ उर्दू शेरों में फारसी व अरबी शब्दों के साथ कई हिन्दी शब्द भी हैं, वहीं हिन्दी गज़लों में उर्दू फारसी अरबी शब्दों के साथ संस्कृत व हिन्दी के शब्द स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल हुए हैं. भाषाएँ सीमा बना कर तलवारों या बंदूकों से अपने अपने शब्दों की रक्षा नहीं करती, वरन मित्रता पूर्वक आदान-प्रदान करती हैं. उदाहरण, ठेठ तत्सम, तद्भव और देसी हिन्दी शब्दों का उपयोग:
एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी,
आदमी की पीर गूगी ही सही गाती तो है.
1 सितम्बर को दुष्यंत कुमार का जन्मदिवस पड़ता है. पर 1 सितम्बर 1933 को जन्मे दुष्यंत कितनी जल्द साहित्य जगत को एक असहनीय आघात दे कर चले गए थे! मात्र 42 वर्ष की आयु में, 30 दिसम्बर 1975 को. आपातकाल, जिस पर 'साए में धूप' के अधिक से अधिक शेर लागू होते थे, तो अभी 14 महीने और चला था. दुष्यंत अपनी कलम में न जाने कितनी और पीर छुपा कर सहसा साहित्य जगत को फिलहाल सूना कर गए. पर उनके द्वारा जलाई गई हिन्दी ग़ज़ल की मशाल कई अन्य शायरों ने हाथ में ले कर ग़ज़ल यात्रा को आगे बढ़ाया. जहाँ उर्दू की शायरी तीन चार शताब्दियों तक इश्क से बाहर नहीं आ पाई, वह केवल साकी, बज्म, तगाफुल, मकतबे-इश्क, शराब, सागर, बुलबुल, सैयाद,कफस आदि में कैद रही, गमे-जानाँ वाली शायरी ही अधिक पली पनपी, वहीं दुष्यंत ने शायर को सीधे व्यवस्था से टकराना सिखाया, परिस्थितियों के प्रति एक सेन्सीटिविटी ले कर जीने की प्रेरणा दी. साए में धूप की गजलें उनकी पहली गजलें नहीं थी. वहां तक पहुँचने के लिए उन्होंने असंख्य और गजलें लिखी, पर वे सब जैसे मंजिल तक पहुँचने का रास्ता थी. आज अनेक युवा शायर तक दुष्यंत कुमार की विरासत सीने से लगा कर ग़ज़ल को नित नए आकाशों और ज़मीनों तक ले जा रहे हैं, तो यह दुष्यंत की शाश्वतता का ही प्रमाण है.
इस युग पुरूष को मेरा शत शत प्रणाम.