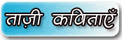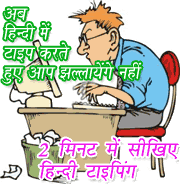तुलसीदास जन्मदिवस पर बोधिसत्व, श्याम सखा 'श्याम' और प्रेमचंद सहजवाला के मंतव्य
आज विक्रम संवत् के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। ज्यादातर विद्वान महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के दिन मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में तो सभी ने कुछ ना कुछ सुन ही रखा होगा। हमने सोचा कि उनकी जयंती कैसे मनाई जायँ? उत्तर आया कि कुछ विशेष होना चाहिए। जब भी तुलसीदास का नाम आता है, उनको राम से जोड़कर देखा जाने लगता है। हमने सोचा कि आज के दिन तुलसीदास से जुड़े और उनके द्वारा रचित चरित्र राम के बारे में अलग-अलग विद्वानों के विचार लिये जायें। तो हम हाज़िर हैं प्रसिद्ध कवि बोधिसत्व, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ॰ श्याम सखा श्याम और वरिष्ठ कथाकार प्रेमचंद सहजवाला का विश्लेषण लेकर। सभी एक-दूसरे से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे अंतरजालीय पाठक जो इन विषयों पर आर एण्ड डी करना चाहते हों, उनके लिए हमारी यह पेशकश बहुत उपयोगी होगी।
रामबोला
मंतव्यक- डॉ॰ श्याम सखा श्याम
 राम बोला -जी हाँ, यही नाम था उस अभागे बालक का जो संवत १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में बारह माह गर्भ में रहकर बान्दा जिले के राजापुर गांव के प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण दम्पति के यहां पैदा हुआ था। मां का नाम हुलसी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनके जन्म के संबन्ध में, उनके जीवन के संबन्ध में अनेक किंवदंतिया प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस बालक के मुख में ३२ दांत थे तथा जन्मते ही रोने के बजाय इनके मुख से राम शब्द निकला। डील-डौल भी विकराल था। पिता द्वारा अमंगली शिशु कहने पर, मां हुलसी ने इसे चुनिया नामक दासी के साथ चुनिया की ससुराल भेज दिया। बालक अभी पांच वर्ष का था कि चुनिया का देहान्त हो गया।
राम बोला -जी हाँ, यही नाम था उस अभागे बालक का जो संवत १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में बारह माह गर्भ में रहकर बान्दा जिले के राजापुर गांव के प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण दम्पति के यहां पैदा हुआ था। मां का नाम हुलसी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनके जन्म के संबन्ध में, उनके जीवन के संबन्ध में अनेक किंवदंतिया प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस बालक के मुख में ३२ दांत थे तथा जन्मते ही रोने के बजाय इनके मुख से राम शब्द निकला। डील-डौल भी विकराल था। पिता द्वारा अमंगली शिशु कहने पर, मां हुलसी ने इसे चुनिया नामक दासी के साथ चुनिया की ससुराल भेज दिया। बालक अभी पांच वर्ष का था कि चुनिया का देहान्त हो गया।विनम्रता, विनयशीलता, श्रृद्धा, विश्वास, ज्ञान एवं भक्ति की प्रतिमूर्ती बाबा तुलसी का अनाथ भटकते बालक को रामशैल पर्वत पर रहने वाले साधुश्री नरहर्यानन्द ने अपने आश्रम में रख लिया व इनका नामकरण किया रामबोला वहां से गुरु के साथ चल शूकरक्षेत्र आये वहीं श्री नरहरि ने इन्हें भगवान राम का चरित सुनाया उसके पश्चात १५ वर्ष काशी जी में वेद-वेदांग की शिक्षा लेकर अपने गांव लौटकर रत्नावली नाम की कन्या से विवाह हुआ। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी से झाड़ खाकर कि अगर इतना प्रेम भगवान से करते तो प्रभु मिल जाते, तुलसी अयोध्या होते हुए काशी पहुंचे व साधु बनकर रहने लगे। किंवदंति के अनुसार यहां काशी में उनके भीतर कवित्व जागा और वे संस्कृत में रचना करने लगे, वे जो दिन में लिख कर रखते वह रात को लुप्त हो जाता। यह सात रोज चला। कहा जाता है कि आठवीं रात भगवान शंकर ने इन्हें कहा कि तुम अयोध्या जाकर अपनी भाषा[अवधी] में रामचरित की रचना करो। सम्वत् १६३१ रामनवमी के दिन आरम्भ कर २ वर्ष सात महीने २६ दिन में यह विश्वप्रसिद्ध काव्य रचना पूर्ण हुई। यूं तो बाबा तुलसी के जीवन से जुड़ी दंतकथाओं की सीमा ही नहीं है यहां मैं बस एक और ऐसी कथा का जिक्र कर तुलसीकृत रामचरित मानस के जीवन उपयोगी प्रसंगो का जिक्र करूंगा। कहते हैं
कि रामचरित मानस की रचना के पश्चात बाब तुलसी की नींद गायब हो गई, वे परेशान रहने लगे तब उन्हें हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि तुलसी तुमने इस ग्रंथ में भक्ति से अधिक विद्वता भर दी है। यह तुम्हारे अपने ज्ञानी होने के अंहकारवश हुआ है, तुम इसे दोबारा भक्तिपूर्वक लिखो। इसके बाद तुलसी ने गीतावली नाम से रामचरित मानस को दोबारा लिखा, इसमें दो-तिहाई भाग भगवान राम के बालचरित पर बालकांड ही है। तथा शेष कथा मात्र एक तिहाई ग्रंथ मे सिमटी है। उसके बाद भी बाबा तुलसी ने दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि लिखी।
मित्रो, यह तो था बाबा तुलसी के जन्म के बारे में, आइये अब देखें रामचरित नामक इस अद्भुत ग्रंथ में क्या है? वाल्मिकी रामायण राम के चरित को वह ऊंचाई न दे सकी जो तुलसीकृत रामायण ने दी। राम को मर्यादा पुरूषोत्तम की ऊंचाई तक ले जाने का कौशल तुलसीकृत राम चरितमानस से ही संभव हुआ है। मैं अब आप का ध्यान राम चरित मानस के दो प्रसंगो में निहित आम मनुष्य के लिये छुपी जीने की कला की ओर ले जाने का प्रयत्न करता हूँ।
पहला प्रसंग है मुनि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ रक्षा हेतु, राम व लक्ष्मण को लाने के लिये राजा दशरथ के पास जाना। कथा है कि वन में मुनिवृंद जब यज्ञ करते तो मारीच व सुबाहु के साथ राक्षस यज्ञ का विद्धवंश कर डालते थे, बाल-काण्ड के दोहा नं २०५ के बाद चौपाई है-
विश्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी।।
जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं,अति मारीच सुबाहुहि डरहिं।।
देखत जग्य निशाचर धावहिं। करहीं उपद्र्व मुनि दुख पावहिं।।
निसाचरों के उपद्र्व देखकर महामुनि ने विचार किया
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतरेहु हरन महि भारा।
आगे कुछ चौपाइयों का अर्थ है कि मुनि ये विचार करते हुए कि भगवान ने राक्षसों के अत्याचारों से आमजन को मुक्ति दिलाने हेतु ही अवतार लिया है अतः राजा दसरथ से उन्हे मांग लाता हूं। विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर चल पड़े।
मुनि आगमन सुना जब राजा।मिलन गयउ लै बिप्र समाजा।
करि दंडवत मुनिहि सनमानी।निज आसन बैठारेन्हि आनी।।
तब त्यागी मुनियों का सम्मान इतना होता था कि राजा ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण पखारे, भोजन करवाया। फिर राम लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाला।
पुनि चरननि मेले सुत चारी।
बिनोवा भावे का कथन
महात्मा बुद्ध के बाद इतना महान कोई नहीं हुआ, जितने तुलसीदास। तुलसी दास जी ने भारत बचाने का जो काम किया वह अकबर राज्य में पचास राजा मिलकर भी नहीं कर पाये, वह तुलसी के इस ग्रंथ ने किया। तुलसी ने कोई काव्य ग्रंथ नहीं लिखा, अन्तर की भावना लिखी है। राम चरित मानस के रूप मे एक ऐसा ग्रंथ जनता को दिया, जिसमें एक अंश नीतिशास्त्र का है, एक अंश सत्पुरुषों की कथाओं का जिसके माध्यम से moral शिक्षा दी, एक अश भक्ति का जिससे [आम मनुष्य चिन्ता से मुक्त रहना सीख ले], एक अंश विधि-निषेध का- इस तरह यह ग्रंथ एक रसायन बनाकर लोक्भोग्य, लोक प्रिय रूप में दिया। यह गृहस्थ के लिये गीता है। मैंने तुलसी रामायण का पाठ कई बार किया=पाठ के लिये ही नहीं, चिन्तन के लिये मनन के लिये। और पढ़ाया भी है
--श्याम सखा 'श्याम'
फिर यह कहते हुए कि महाराज आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया, आप मुझ सेवक को बुला भेजते? मुनि के आने का कारण पूछा। मुनि ने आने का कारण बतलाते हुए यज्ञ रक्षा करने के लिये राम व लक्षमण को अपने साथ भेजने को कहा। यह सुनते ही-सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी।।
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी।।
मित्रो, यह कथा आप सभी ने सुनी-पढ़ी होगी, अब इस में निहित कुछ बातों को जानने के लिये हमे चार चौपाइयाँ फिर पढ़नी होंगी।
विश्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी।।
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतरेहु हरन महि भारा।।
मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ लै बिप्र समाजा।।
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी।।
पहली चौपाई में विश्वामित्र अपने आश्रम में हैं। दूसरी में अपने आश्रम में बैठे हुए राजा दसरथ के पुत्र राम की सहायता के बारे में सोच रहे हैं। तीसरी में सहायता लेने अयोध्या पहुंच गये है, लेकिन अभी सहायता मांगी नहीं है।
चौथी में सहायता मांग ली है। अब इन चौपाइयों को व bold अक्षरों पर ध्यान देते हुए देखें-
विश्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी।
अपने घर बैठे विश्वामित्र महामुनिज्ञानी हैं।
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतरेहु हरन महि भारा।।
दूसरे से सहायता लेने का विचार आते ही वे मात्र मुनिवर [श्रेष्ठ मुनि रह गये]
मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ लै बिप्र समाजा।।
सहायता हेतु दूसरे के द्वार पर जाते ही वे मुनिवर भी नहीं मात्र मुनि रह गये।
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी।।
सहायता मांगते ही वे मुनि भी नहीं रहे मात्र एक ब्राह्मण भर रह गये। अब आप समझ गये होंगे कि तुलसी रामायण में ऐसे अनेक अनमोल सूत्र हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रो,
राम चरित मानस में कथा आती है। नारद के अंहकार की, उसके माध्यम से बड़ी गूढ़ बात कहते हैं बाबा तुलसी। एक बार नारद जी वन से होकर जा रहे थे। वन की सुन्दरता देख सहज भाव से प्रभु का ध्यान करने लगे। उन्हें ध्यान में मगन देख देवराज इन्द्र डरे कि कहीं नारद जी की तपस्या से प्रभु प्रभावित हो, नारद को ही इन्द्र का पद न दे दें।
निरखि सैल सरि बिपिन विभागा।
भयऊ रमापति पद अनुरागा।।
सुहावने वन को देखकर देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि इसी सुन्दर स्थान पर रमापति भगवान विष्णु की श्री आराधना करनी चाहिए।
तुलसी रामचरित मानस बनाम आज की फ़िल्में
मित्रो,
महाभारत व रामायण ग्रंथो से बाहर साहित्य को सोचा ही नहीं जा सकता, यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, और उर्दू पढे को फ़ारसी क्या।
आज अधिकांश फ़िल्मों में आप हीरो-हिरोइन को पार्क में पेडों के ईर्द-गिर्द गाना गाते देखते हैं। तुलसी रामचरित मानस में राम-सीता का सामना प्रथम बार जनकवाटिका में हो या दुष्यन्त-शकुन्तला का क्ण्व आश्रम में।
यही नहीं, बालकांड दोहा 228 के बाद की चौपाई देखें।
स्याम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी।
सीता जी राम लक्ष्मण के श्याम-गौर रूप को देख अचम्भित खड़ी हैं।
न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है।
दोहा २३१ के बाद दूसरी चौपाई देखें
लोचन मग रामहिं उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी
अब यह गाना याद करें
हम आपकी आँखो में, इस दिल को बसा दें तो
हम मूंद के पलकों को, इस दिल को सजा दें तो
यही नही सीताजी के गौरी पूजन के समय का दृश्य देखें-
बालकांड दोहा २३५ के बाद
गौरी पूजन करते हुए जानकी जी कहती हैं।
मोर मनोरथु जानहुं नीके। बसहु सदा उर पुर सबही कें
कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही। अस कहि चरन गहे बैदेही
हे मां गौरी! आप तो सबके मन में वास करती हैं, अतः आपको मेरा मनोरथ भी पता है यह कहकर वैदेही ने मांगौरी के चरण पकड़ लिये।
विनय प्रेम बस भई भवानी।खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
सीता जी की विनय भरी वाणी सुन गौरी जी प्रेम वश हो गई और गौरी जी की मूर्ति मुस्काने लगी व उनकी मूर्ति से माला खिसक कर सीता जी पर आ पड़ी॥
मित्रो, इन प्रसंगो के कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे साहित्य ,कला, या जीवन में विवेक सीखना हो तो तुलसी के ग्रंथ इन सबका अद्भुत स्रोत हैं। इन्हे केवल धर्म ग्रंथ समझ कर न तो पढ़े, न ही इन्हें पाखंड मान इनका परहेज करें अपितु इन्हें मनन चिन्तन के लिये पढें।
--श्याम सखा 'श्याम'
देखिये स्थान वही होता है मगर मनुष्य अपने चित के कारण उसके अलग-अलग उपयोग ढूँढ़ लेता है। तीर्थ स्थानों पर भक्त दर्शन हेतु जाते हैं। मगर जेब कतरे जेब दर्शन हेतु। अतः अगर नारद जी के स्थान पर कोई लकड़ी का ठेकेदार तो वह वन के लकडिय़ों का भंडार देखेगा- डाकू को छुपने का उचित स्थान लगेगा। इसी तरह सुन्दर सुहावने वन देखकर लोग टूरिस्ट स्पाट की बात सोचने लगेंगे मगर देवर्षि के मन में 'भयऊ रमापति पद अनुरागा' चरणों में अनुराग मुख पर नही, हाथ पर नहीं चरणों में क्योंकि ऋषि हैं हाथ को क्यों देखेंगे। जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है वे जेबकतरे थोड़े ही हैं जो जेब को देखें। उसी तरह मुख भी नहीं देख रहे क्योंकि उन्हें मुख से कुछ मांग पूरी करवाने की इच्छा नहीं है। उनका अनुराग तो रमापति भगवान विष्णु के चरणों में है।सुमरित हरिहि श्राप गति बाधी।
सहज विमल मन लागी समाधि।।
सहजता से ही बिना प्रयत्न समाधि लग गई। समाधि-माने मन एकाग्र हो गया। भगवानके चरणों में संत हैं अतः यह सहज संभव था। मगर
मुनि गति देख सुरेस डराना
दो बातें हैं जो जैसा होता है
जाकी रही भावना जैसी
प्रभु-मूरत नित देखी तैसी
मुनि ने वन देखा प्रभुचरणों में अनुराग साधना तपस्या के लिए जाग गया मगर, इन्द्र ने देखा जब मुनि को उसी वन में समाधि रत तो उसे डर जाग गया।
मुनि गति देख सुरेस डराना
मुनि का रूप देखकर इन्द्र डर गया कि तेरा राज्य छीनने को साधना रत हैं
जे कामी लालुप जग माहीं
कुटिल काक इव सबहिं डरोहीं
इन्द्र स्वर्ग का राजा है। वहाँ भोग है, भक्ति नहीं है तो स्वामी जी ने लिखा है जो कामी है, लोभी है, जितने भी ऐसे लोग है, जग में वे कव्वे के समान डरते रहते हैं। इधर-उधर ताक-झांक में लगे रहते हैं। सो इन्द्र ने
मुनि गति देख सुरेस डराना
कामहि बोलि कीन्हि सन्माना
बाबा तुलसी हर किसी को समझाते हैं- कामहि बोली कीन्हि सन्माना।
जब आपसे बड़ा अफसर आपको बुलाकर कुछ ज्यादा ही आवभगत करता है तो चौकन्ने हो जाएँ वह आपसे कोई गलत काम करवाना चाहता है।
बड़े प्यार से बोलेगा- आइये मिश्रा जी जो कल कह रहा था, मिश्रा देखो ठीक से काम किया करो। तुम्हारी बहुत शिकायते आ रही हैं और आज कह रहा है मिश्रा जी
'कामहि बोलि कीन्हि सन्माना' सो कामदेव को पटाकर भेज दिया नारद जी के पास:-
बहुत प्रयत्न किये कामदेव ने समाधि तुड़वाने के। सभी काम कलाओं में प्रवीण अप्सराओं का कोई असर नहीं हुआ तो नारद ऋषि पर कामदेव ने हाथ जोड़ कर मुनि से क्षमा मांगी।
भयउ न नारद मन कुछ रोषा
कहि प्रिय वचन काम परितोषा
सुन सब के मन अचरजु आवा
मुनिहि प्रससि हरिहि सिर नावा
देवताओं ने लौटकर आए काम देव की बात सुनी तो अचरज माना क्यों कि कामदेव ने भगवान शंकर तक की समाधि तुड़वा दी थी। मगर सन्तों को भगवान मोह से बचाते हैं। काम को जीता नारद ने मगर देवताओं ने 'मुनहिं प्रससि हरि सिर नावां' नारद की प्रसंशा की मगर सिर झुकाकर भगवान को नमन किया।
तब नारद गवने सिव पाहीं
जिता काम अहिमति मन माहीं
नारद जी को अंहकार हो गया कि वह शंकर जी, नारद जी के गुरु जिस कामदेव को जीत नहीं पाए उसे उन्होंने नारद ने जीत लिया।
मार चरित संकरहि सुनाए- अतिप्रिय जान महेस सिखाए
भगवान शकर दयालु हैं कहने लगे।
बार बार बिनवऊ मुनि तोही
जिमि यह कथा सुनाहुँ मोहीं
तिमि जाने हरिहिं सुनावहूँ कबहूँ
चले हूँ प्रसंग दुराएहि तबहूँ।
हरि को, विष्णु को यह कथा मत सुनाना यह प्रसंग चले तब भी मत सुनाना।
संभु दीन उपदेश हित नहि नारद सोहान
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरिइच्छा बलवान
पहले ब्रह्मा के पाए गए सब कुछ कहा फिर विष्णु के पास जाकर सभी कुछ कह डाला। रमापति भगवान विष्णु ने देख लिया कि ऋषि को अंहकार हो गया है।
रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान
तुम्हरे सुसिरन तें मिटहिं मोह मार सदमान
भगवान का चेहरा तो स्पष्ट रुखा था। उन्हें नारद का अहंकार अच्छा नहीं लग रहा था। मगर वचन बड़े मीठे थे कहने लगे हे नारद तुम्हारे नाम के सुमरिन से मोह-मार मदमान मिट जाते हैं सोकामदेव को जीतना तुम्हारे लिए कौन सा असम्भव काम था।
ध्यान रहे मीठा बोलने वाले का बोल ही नहीं हाव-भाव भी पहचाने ।
नारद कहेऊ सहित अभिमाना
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना
अंहकारी जब यह भी कहता है कि यह तुम्हारी कृपा है तो भी उसका अर्थ होता है कि देखा मेरा बल मेरा पौरूष मेरी बुद्धि। - विनम्रता और अंहकार भरी विनम्रता का अन्तर समझें। विनम्रता अपनाएं। अहंकार नहीं।
भगवान ने अपनी माया से श्री निवासपुर नगरी की रचना कर दी उसी राह में जहाँ से नारद मुनि जा रहे थे- श्री निवासपुर के राजा थे। शीलानिधि- उन नवयुवती बेटी का नाम था राजकुमारी विश्वमोहिनी। नारद राजा के पास गये। राजा ने आवभगत कर अपनी बेटी को बुलाया, उसका रूप देख-
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी
राजा ने नारद से बेटी के भाग्य के बारे में पूछा तो नारद जी ने जन्मपत्री देख कर पाया कि
जो ऐहि बारह अमर सोई होई-
समर भूमि तेहि जीत न कोई
लेकिन मोह में पड़कर असली बात न कहकर इधर-उधर की बातें बता दीं
लच्छन सब विचार उर राखें
कुछ बनाई भूप सन भाषे
फिर बाहर आकर सोचा कि अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाये तो मैं जगतपति बन जाऊँ। मगर इसके लिये तो विष्णु जैसा रूप चाहिये जिससे स्वयंवर मे राजकुमारी मेरा वरण करे। बैठ गये भगवान के स्मरण को, भगवान के दर्शन होने पर बोले
आपन रूप देहु प्रभु मोहि
आन भाँत नही पावैं ओही
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा
कर हूँ सो बेगि दास मैं तोरा
हे प्रभु मुझे अपना रूप दें जिससे मेरा विवाह हो जाय और प्रभु जल्दी से ऐसा काम करें जिससे मेरा हित हो।
निज माया बल देखि विशाला
हिय हम बोले दीन दयाला
जेहि विधि होहहि परम्हित
नारद सुनहूँ तुम्हार
सोई हम करब आन कछु
वचन न मृषा हमार
भगवान बोले हे नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परमहित हो। अब देखें नारद जी कह रहें है कि ऐसा काम करें जिससे मेरा हित हो। मगर भगवान कह रहे हैं, मैं वह काम करूंगा जिससे तुम्हारा परमहित हो। यह तो वही बात हुई जैसे शतरंज का खिलाड़ी छोटे मोहरे के बदले बड़ा मोहरा मिलता देख यह भूल जाए कि यह जाल बिछाया जा रहा है मात के लिये। मगर नारद जी नहीं समझ रहे इसे। ऐसा हम सब के जीवन में भी होता है और अगर हम नासमझे तो नुकसान उठाते हैं, लोगों की मीठी बातों में आकर। यही नहीं आगे भी कहा भगवान ने
कुपथ माँग रूज व्याकुल रोगी
वैद न देहिं सुन मुनि जोगी
हे मुनि सुनो! अगर कोई रोगी कुपथ्य जिसका परहेज हो, वह चीज मांगे, व्याकुल हो उसे पाने के लिये, तब भी वैद्य उसे वह नहीं देते। क्योंकि उससे रोगी का नुकसान होता है। इशारे में भगवान समझा रहे हैं मगर मायावश होकर नारद जी समझ ही नहीं रहे। मनुष्य लोभ-लालच में ऐसा ही अंधा हो जाता है। आपने पढा सुना होगा कि कैसे रुपये दुगने करने का लालच देकर लोग ठग लिये जाते हैं। यानी विवेक खोकर हम नुकसान उठाते हैं।
जिस तरीके तुम्हारा परमहित होगा हित नहीं परमहित होगा वही मैं करूँगा। भाई तुम माँग रहे हो सौ रुपए और कोई उसी चीज के पाँच सौ दे रहा है तो सावधान हो जाइए कि कहीं वह तो पाँच सौ का नोट दे रहा है। वह नकली तो नहीं है या उसका कोई और स्वार्थ तो नहीं है।
शतरंज में खेल में - आप में से कुछ लोग जरूर खेलते होंगे- बुद्धि का खेल जिन्दगी के आरम्भिक दिनों में बुद्धि तेज करने के लिए खेलना चाहिए विलास या लत के लिए नहीं।
शतरंज में खेल में कभी-कभी लगता है कि हमारा विरोधी खिलाड़ी मूर्ख है। प्यादे के बदले में घोड़ा या ऊँट मरवा रहा है मगर असावधान हुए तो वह प्यादे के बदले वह घोड़ा देकर हमारे दुर्ग में सेंध लगा कर मात कर देता है।
ठीक वैसे ही जब नारद जी हित की बात कर रहे हैं तो प्रभु परमहित दे रहे है मगर नारद सावधान नहीं है। प्रभु आगे चेता भी रहे हैं। भगवान भक्त को संभलने का पूरा अवसर देते हैं तो कह रहे हैं।
माँगे कुपथु रूज व्याकुल रोगी
वैद न देहिं सुन मुनि जोगी
अरे भाई रोगी अगर व्याकुल हो जाए आर्तनाद करे तो भी सुघड़ वैद्य उसे वह वस्तु नहीं देते जिसका परहेज है जैसे मधुमेह के रोगी को शक्कर, उच्च रक्तचाप के रोगी को नमक आदि।
भगवान ने कहा-
मांगे कुपथ रुज व्या्कुल रोगी
वैद न देहिं सुन मुनि जोगी
मगर नारद तो प्यादे के बदले घोड़ा प्राप्त करना चाह रहे थे।
माया विवश भये मुनि मूढ़ा
समझी नहीं हरि गिरा गूढ़ा
माया के वश में हो कर नारद मुनि ने तन मन विवेक सभी त्याग दिये थे। अत: प्रभु की सार ग्रभित वाणी को समझ नहीं पाए। जब हम लालच वश इच्छा वश हो जाते हैं यानी स्वयं के वश में न रह दूसरे के वश में हो जाते हैं जैसे बच्चे प्यार, इश्क, वासना के वश हो्कर शराब के वश होकर या नशे के वश होकर कुछ नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, किसी की जायज बात भी नहीं सुनते।
आगे की कथा आप जानते ही हैं कि कैसे भगवान ने, नारद को वानर का रूप देकर उसके अंह्कार का विनाश किया
चन्द बातें रामायण पर- तुलसीदास जन्मदिवस के बहाने
मंतव्यक- प्रेमचंद सहजवाला
 गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जब अपनी स्मृति को पीछे दौड़ता हूँ तो याद आता है कि मैं जब वर्धा विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाओं की तैयारी बचपन की छोटी कक्षाओं की पढ़ाई के दौरान अलग से कर रहा था, तब तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित एक लेख बहुत रोचक लगता था। उन्हीं दिनों (लगभग सन 56 की बात है), एक श्याम-श्वेत फ़िल्म भी आयी थी 'गोस्वामी तुलसीदास'. बड़े भाई के साथ बहुत उत्साह से गया कि यह तो अपनी पढ़ाई का हिस्सा है. थिएटर में 11 साल का एक लड़का यानी मैं देख-देख कर प्रसन्न हो रहा था कि एक किशोरावस्था का लड़का तुलसीदास भोला-भाला व आकर्षक तो है, पर उस का कोई नाम नहीं और हर कोई उसे अपने ढंग से बुलाता है - अरे ओ अनामी. अनामी! बड़े भाई समझाते जा रहे थे - वह देखो, तुलसीदास के गुरु, क्या नाम है इनका? मैं उत्साह से थिएटर के अंधेरे में ही बोल पड़ता - संत नरहरिदास. भाई खुश होते. फिर बालसुलभ तरीके से देखा कि तुलसीदास बड़े हो गए है. बहुत सुंदर लड़की से शादी करने वाले हैं. मैं भाई से पूछता हूँ - यही है न, रत्नावली? भइया पीठ थपथपाते हैं. अब देखना. फिर आगामी दृश्यों में तुलसीदास रत्नावली के प्रेम में ऐसे पग जाते हैं कि एक दिन रत्नावली के ऊंचे घर की खिड़की से लटकते बड़े से सांप को भी रस्सी समझ कर सांप को ही पकड़ कर खिड़की तक और फिर रत्नावली के घर के भीतर पहुँच जाते है. बड़ा रोमांच हुआ. फिर शादी हो जाती है तो एक दिन रत्नावली तुलसीदास से कहती है कि आज दुकान से ज़रा जल्दी आ जाना. तुलसीदास एक दुकान जैसे-तैसे चलाते हैं, हालांकि कोई भी सांसारिक काम करना उनके बस की बात नहीं है . तुलसीदास क्या करते हैं कि दुकान का ताला खोल कर दुकान के अन्दर जाते हैं. कुछ देर यूँ ही अपने आसन पर बैठ इधर-उधर देखते हैं, फिर चंद मिनटों में ही दुकान को ताला लगा कर घर आ जाते हैं. रत्नावली हैरान है. मैंने यह थोड़ा कहा था कि अभी दुकान खोल कर अभी बंद कर देना. खूब हंसा मैं. पर मध्यांतर के बाद एक दृश्य देख घबरा भी गया. तुलसीदास और रत्नावली का झगड़ा. और जिस तुलसीदास को कभी रत्नावली के घर की खिड़की से लटक रहा सांप भी रस्सी लगा था, उसी तुलसीदास को रत्नावली के बालों में सजी वेणी भी सांप लगने लगी. इस के बाद तुलसीदास का जीवन बदलता जाता है.
गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जब अपनी स्मृति को पीछे दौड़ता हूँ तो याद आता है कि मैं जब वर्धा विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाओं की तैयारी बचपन की छोटी कक्षाओं की पढ़ाई के दौरान अलग से कर रहा था, तब तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित एक लेख बहुत रोचक लगता था। उन्हीं दिनों (लगभग सन 56 की बात है), एक श्याम-श्वेत फ़िल्म भी आयी थी 'गोस्वामी तुलसीदास'. बड़े भाई के साथ बहुत उत्साह से गया कि यह तो अपनी पढ़ाई का हिस्सा है. थिएटर में 11 साल का एक लड़का यानी मैं देख-देख कर प्रसन्न हो रहा था कि एक किशोरावस्था का लड़का तुलसीदास भोला-भाला व आकर्षक तो है, पर उस का कोई नाम नहीं और हर कोई उसे अपने ढंग से बुलाता है - अरे ओ अनामी. अनामी! बड़े भाई समझाते जा रहे थे - वह देखो, तुलसीदास के गुरु, क्या नाम है इनका? मैं उत्साह से थिएटर के अंधेरे में ही बोल पड़ता - संत नरहरिदास. भाई खुश होते. फिर बालसुलभ तरीके से देखा कि तुलसीदास बड़े हो गए है. बहुत सुंदर लड़की से शादी करने वाले हैं. मैं भाई से पूछता हूँ - यही है न, रत्नावली? भइया पीठ थपथपाते हैं. अब देखना. फिर आगामी दृश्यों में तुलसीदास रत्नावली के प्रेम में ऐसे पग जाते हैं कि एक दिन रत्नावली के ऊंचे घर की खिड़की से लटकते बड़े से सांप को भी रस्सी समझ कर सांप को ही पकड़ कर खिड़की तक और फिर रत्नावली के घर के भीतर पहुँच जाते है. बड़ा रोमांच हुआ. फिर शादी हो जाती है तो एक दिन रत्नावली तुलसीदास से कहती है कि आज दुकान से ज़रा जल्दी आ जाना. तुलसीदास एक दुकान जैसे-तैसे चलाते हैं, हालांकि कोई भी सांसारिक काम करना उनके बस की बात नहीं है . तुलसीदास क्या करते हैं कि दुकान का ताला खोल कर दुकान के अन्दर जाते हैं. कुछ देर यूँ ही अपने आसन पर बैठ इधर-उधर देखते हैं, फिर चंद मिनटों में ही दुकान को ताला लगा कर घर आ जाते हैं. रत्नावली हैरान है. मैंने यह थोड़ा कहा था कि अभी दुकान खोल कर अभी बंद कर देना. खूब हंसा मैं. पर मध्यांतर के बाद एक दृश्य देख घबरा भी गया. तुलसीदास और रत्नावली का झगड़ा. और जिस तुलसीदास को कभी रत्नावली के घर की खिड़की से लटक रहा सांप भी रस्सी लगा था, उसी तुलसीदास को रत्नावली के बालों में सजी वेणी भी सांप लगने लगी. इस के बाद तुलसीदास का जीवन बदलता जाता है.उन दिनों मैं मुंबई के उल्हासनगर कसबे में पढ़ता था. फिर दिल्ली आ गया तो 8वीं कक्षा में लक्ष्मण-परशुराम संवाद भी खूब दिलचस्प था. अवधी भाषा में इन पंक्तियाँ में खूब मज़ा था:
बहु धनुहीं तोरेउँ लरिकाई, कबहूँ न असि रिस कीन्हीं गोसाई.
एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनी रिसाइ कह भृगुकुलकेतु.
हमने लड़कपन में बहुत धनुहियाँ तोड़ डाली. पर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया. इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है. यह सुन कर भृगु-वंश की ध्वजा स्वरुप परशु राम कहने लगे:
रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार
धनुहीं सम तिपुरारि धनु बिदति सकल संसार.
हे राजपुत्र, कालवश तू होश हवास में रह कर नहीं बोल रहा. विश्वप्रसिद्ध यह शिव धनुष क्या तुझे धनुही के समान दिख रहा है?
स्कूल की उस पढ़ाई के बाद विज्ञान विषयों के कारण कभी न तो तुलसीदास और ने उनके द्वारा रचित जगप्रसिद्ध ग्रन्थ 'राम चरित मानस' की ओर अधिक ध्यान गया. अलबत्ता रामलीला लगभग हर साल देखता रहा. राम लीला हमारी सभ्यता का हिस्सा बन गयी लगती थी. सत्य की झूठ पर विजय, अच्छे की बुरे पर विजय. सही की ग़लत पर विजय. यह सब और हनुमान की बड़ी-बड़ी पूँछ व कुम्भकरण की गगनचुम्बी आकृति. फिर राम-सीता-लक्ष्मण अचानक दूरदर्शन पर नज़र आए. एक अध्याय में लगा जैसे भगवन राम अयोध्या के महल में खड़े हो कर राष्ट्र के नाम संदेश दे गए. इस परिपक्व अवस्था में मुझे लगा कि तुलसी की रामायण भी समय-समय के साथ बदलती गयी. ऐसा दौर भी आया कि तुलसीदास और उनके राम का राजनीतिकरण हो गया. मैंने हाल ही में जब ग़ज़लें लिखनी शुरू की तब उन दिनों की राम तस्वीर को भी चिंतनवश याद करने लगा. राम की कसी हुई कमान पर चढ़े तीर वाली तस्वीर जगह-जगह दिखाई देती थी, जैसे राम युद्धभूमि में खड़े हैं. पर नेताओं का कोप भाजन वास्तव में मुसलमान था. इसलिए एक शेर मेरी लेखनी से स्वयमेव निकला:
राम को यह क्या हुआ है दोस्तो ,
तीर उसका मुस्लिमों की ओर है !
राम को कुर्सी तक पहुँचने का माध्यम बनाया गया. मैंने थोड़ा अध्ययन कर के कुछ नयी और अनूठी सी बातें पता की जिन्हें यहाँ लिखने का तात्पर्य तुलसीदास के विरुद्ध लिखना नहीं है वरन एक अध्ययनशील व्यक्ति द्वारा तथ्यों की खोज की उत्कट प्रवृत्ति को दिखाना मात्र है. आज राम-सेतु भी एक राजनीतिक युद्ध का विषय बन गया है. अमरीका की अन्तरिक्ष संस्था NASA ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच कुछ बर्फीले व मिट्टी के से टीले मिल कर एक सेतु का सा आभास देते हैं. बस शुरू हो गया राजनीति का कुचक्र. मैंने कुछ पुस्तकों से खोजना चाहा कि राम थे या नहीं थे. पता चला कि वास्तव में राम-कथा का वजूद शुरू से ले कर कई सदियों तक वैसा ही रहा जैसा कि देवदास फ़िल्म का. कई बार बनी. हर समय की तकनीक व सोच के अनुसार उस में परिवर्तन आते गए. राम-कथा भी पहले कई सदियों तक ज़बानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही. जैसे रामानंद सागर की रामायण में राम का उपदेश राष्ट्र के नाम संदेश जैसा लगा, वैसे ही राम-कथा भी सामयिक संस्कृति के अनुसार बदलती गयी. जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, वे दरअसल जंगली जातियां थीं जो बाद में कवियों की कल्पनाओं से राक्षस बनती गयी. पहले तो राम-कथा कोई धार्मिक कथा थी ही नहीं और कई सदियों तक इसे केवल गा कर भी सुनाया जाता रहा. फ़िर एक समय आया जब राम-कथा लिखित रूप में लिखी जाने लगी. एक रोचक कथा में बाल काण्ड व उत्तर काण्ड जोड़ दिए गए. और एक कपोल-कथा के जन-नायक देखते-देखते भगवन विष्णु के अवतार बन गए. राम-कथा एक धर्मग्रंथ बन गयी. इस के रचनाकार का नाम वाल्मीकि कर के जोड़ दिया गया और इसे विश्वस्त बनाने के लिए रचनाकार वाल्मीकि को एक अछूत जाति का पूर्व डाकू रत्नाकर बताया गया जो परिस्थितियों से गुज़रते हुए हृदय परिवर्तन के बाद ऋषि बन गया. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने इन तमाम बातों को अपनी पुस्तक 'cultural pasts' के एक लेख में काफ़ी विस्तृत रूप में लिया है. उनका कहना है कि राम-कथा राजा और उसके राजनीतिक तंत्र के अनुसार भी बदलती गयी. यदि कोई नया राजा बने तो वह चाहे किसी भी जाति का हो, अपने दरबार के पंडितों से अपनी नयी वंशावली लिखवा देता था. इस में दो वंश यानी सूर्यवंश व चंद्रवंश सर्वप्रसिद्ध थे. जिस राजा को सूर्यवंशी कहा जाता उस में जिज्ञासा होती थी कि इस वंश में कोई प्रमुख व सशक्त राजा रहा होगा. उसे बताया जाता कि सूर्यवंश में अयोध्या के राजा राम से अधिक सशक्त कोई नहीं. तब अपने राजा को शूरवीर व महान घोषित करने के लिए राम के चरित्र को भी खूब बढ़ा-चढा कर प्रसिद्ध किया जाता. ऐसे राम-कथा दिन दूनी रात चौगुनी होती गयी. इतिहासकारों ने अयोध्या की ज़मीन की भी खूब खुदाई की तथा श्रीलंका की भी. पर न तो राम की जगमगाते नगर जैसी अयोध्या मिली और न ही सोने की लंका. अयोध्या में एक दूरस्थ सा गांव मिला और उसमें कृषि आदि नगण्य, व बहुत ही नगण्य जनसँख्या. फिर लंका का तो कहना ही क्या. पहले-पहल लंका कहीं विन्ध्याचल क्षेत्र में थी. तद्नुसार व्यापार व लोगों के स्थानांतरण के साथ लंका भी दक्षिण-पूर्व की तरफ़ बढती गयी. अब वह सुप्रसिद्ध द्वीप है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं.
तुलसीदास की ही कल्पना के कुछ अंश ही देखिये:
गिरि त्रिकूट इक सिन्धु मझारी, विधि निमित्त दुर्गम अति भारी
सोइ मय दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मनिभवन अपारा.
भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस सुक्रनिवासा ,
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बांका, जग विख्यात नाम तेहिं लंका.
खाई सिन्धु गंभीर अति, चारिहूँ दिसि फिर आव
कनक कोट मणि खचित दृड़, बरनि न जाइ बनाव
इसमें तुलसीदास की ऊंची कल्पना से लंका सोने की है जिसमें कई महल हैं जो मणियों व अन्य अमूल्य पत्थरों से सुसज्जित हैं. रावण के ससुर मय दानव ने रावण को दामाद बनाते समय उसे फिर से संवारा. वह नागराज की राजधानी भोगावती से भी अधिक सुंदर है और शुक्राचार्य की राजधानी अमरावती से भी अधिक सुरम्य है. चाहे सीता स्वयम्वर के बाद जनकपुरी किस कदर सजाई गयी, चाहे दशरथ को जब स्वयम्वर में राम की जीत जा कर दूतों ने बताई तो भरत ने अयोध्या को ही कैसा सोने व मणियों से सजा दिया, यह सब तुलसीदास की खर्चीली कल्पना मात्र है.
राम-कथा केवल समय या राजनीतिक तंत्र व संस्कृति के आधार पर ही नहीं बदली वरन धर्म के आधार पर भी बदली. बौद्ध रामायण में राम-सीता भाई बहन हैं तथा जब राम-सीता को छुड़वा कर अयोध्या लाता है तब दोनों भाई-बहन शादी करते हैं जो कि बौद्ध धर्म के किसी पंथ में रिवाज था. इसके बाद दोनों सोलह हज़ार साल तक राज्य करते हैं. जैन रामायण में तो सीता रावण की बेटी है जो जनक ने पाली है तथा रावण तो एक जैन मुनि है. कथा के अंत में राम-लक्ष्मण आदि सब जैन धर्म अपना लेते हैं तथा सीता जैन मुनि बन जाती है.
एक रोचक बात जो कतिपय हिंदू विद्वानों में देखी गयी वह यह कि उन्हें इस बात की चिंता हुई कि लोगों के मन की इस फाँस का क्या उत्तर दिया जाए कि राम जब सीता को मुक्त करा लाये तब आख़िर उस की अग्नि परीक्षा क्यों ली गयी. इसे विद्वानों ने इस तरह समझाना शुरू किया कि राम जब सीता को ले कर बनवास जा रहे थे तब उन्हें पता था कि रावण सीता को अपहृत करेगा. इसलिए उन्होंने सीता को फिलहाल अग्नि देवता के पास सुरक्षित रखा व उस की जगह एक नकली सीता को बनवास ले गए. जब सीता रावण के चंगुल से छूट कर आ गयी तब उस नकली सीता को अग्नि में प्रवेश करने को कहा गया. इस प्रक्रिया में अग्नि ने नकली सीता वापस ले ली व असली सीता अग्नि से बाहर निकल आयी. इस हास्यास्पद तरीके से लोगों के शंका-निवारण को कई विद्वान 'Mental adjustment' कहते हैं जो कि जिज्ञासु लोगों पर थोपी जाती है.
तुलसीदास रचित 'राम चरित मानस' में तुलसीदास के मनोविज्ञान सम्बन्धी दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं. एक तो यह कि मध्यकाल में हिंदू धर्म को कोई चुनौती बाहरी धर्मों से नहीं मिली. हिंदू-मुस्लिम समाज मध्यकाल में शान्ति से रहते थे. एक-दूसरे के धार्मिक पर्वों पर दोनों समाज जाते थे. कुछ नगण्य अपवाद अवश्य होंगे. धर्म-परिवर्तन भी सभी मुस्लिम राजा नहीं करते थे, न ही संचार व्यवस्था आज जितनी अधिक थी. यदि जैसा कि कुछ राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रचार करते हैं कि मध्यकाल में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होते थे तो ब्रिटिश के आते-आते यह सारा देश इस्लाम कबूल कर चुका होता. पर ऐसा नहीं था. वास्तव में हिंदू धर्म को असली चुनौती अक्सर उस के भीतर से ही मिली. प्राचीन काल के गौतम बुद्ध व महावीर तथा मध्य काल के गुरु नानक, तीनों हिंदू थे और तीनों ने मूल धर्मं के विरुद्ध विद्रोह किया तथा ब्रह्मण की सत्ता को चुनौती दी. गुरु नानक ने तो जनेऊ पहनने से ही यह कह कर इनकार किया था कि जो ब्रह्मण मुझे जनेऊ पहना कर पवित्र करेगा उस के अपने चरित्र का क्या भरोसा! तुलसीदास इसी बात से आहत रहते थे कि समाज में ब्रह्मण का कोई आदर नहीं रहा. इसी मनोविज्ञान के तहत यानी ब्रह्मण की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने हेतु तुलसी ने 'राम चरित मानस' लिखी. पर क्या वे मात्र इतने से ही इतना बड़ा ग्रन्थ लिख लेते? राम-कथा के अनेक परिवर्तनों के दौरान एक युग ऐसा भी आया जब राम का नाम भक्ति से जुड़ गया. एक मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक में 'भक्ति' स्वयं अपने बारे में कहती है कि मैं तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्मी, नौवीं शताब्दी तक गुजरात पहुँची व पंद्रहवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में फैल गयी. मध्य काल में तुलसीदास समेत मीराबाई, कबीर व सूरदास आदि सब कवि भक्ति-कवि माने जाते हैं व उन के काव्य-काल को भक्ति-काल कहा जाता है. तुलसीदास भी उसी भक्ति की परम्परा के भक्त-कवि थे जो राम के अनन्य भक्त बन गए. उसी श्याम-श्वेत फ़िल्म का एक दृश्य यह भी याद आता है कि तुलसीदास एक कृष्ण मन्दिर में जाते हैं तो भगवान् को चुनौती देते हैं कि मैं तुम्हें नमन तभी करूंगा जब तुम तीर कमान में यानी साक्षात राम के रूप में नज़र आओगे. और अगले ही क्षण होते चमत्कार को देख मेरा बाल-सुलभ मन चकित था. पलक झपकते ही कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल जाती है. यह सब फोटोग्राफी का चमत्कार है यह मैं नहीं समझ पाया था.
राम-कथा एक लोकप्रिय कपोल-कथा से विकसित हो कर इतना बड़ा भक्ति-ग्रन्थ बन गयी, इससे राम-कथा का महत्व कम नहीं होता न ही तुलसीदास की काव्य प्रतिभा की ऊँचाइयाँ कम होती हैं. 'राम चरित मानस' एक अद्वितीय काव्य-ग्रन्थ है जैसा शायद उस के बाद फिर नहीं लिखा गया. एक जगह तुलसीदास कहते हैं कि सीता की तुलना तुम चंद्रमा से क्यों करते हो. भगवान् ने सीता को गढ़ने के बाद जब मैला पानी फेंका तो उस मैले पानी से चंद्रमा बना और जब भगवान ने हाथ झटके तो मैले पानी की बूँदें इधर-उधर फ़ैल कर सितारों में बदल गयी! ऐसे असंख्य उदाहरणों से तुलसी की रामायण भरी हुई है. पर जो बात मुझे इस से भी अधिक महत्वपूर्ण लगती है वह रोमिला थापर की यह बात कि राम-कथा झूठी सही और इतिहास में राम का कहीं भी लक्षण न सही पर राम-कथा हमारे culture का अभिन्न हिस्सा बन गयी है. मैं समझता हूँ कि सत्य की झूठ पर विजय के अलावा राम-कथा पूरे समाज को जोड़ती है और दीपों की रौशनी से मन में एक आशा का संचार होता है. साथ ही रामलीलाओं के माध्यम से कला व संस्कृति का समुचित विकास होता रहता है.
अशोक वनिका में खुश थे राम-सीता
मंतव्यक- बोधिसत्व
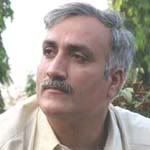 यह प्रसंग बड़ा ही रोचक, जगानेवाला और दुख दाई है । कथाओं से ऐसा लगता है कि राम और सीता ने सुख के दिन देखे ही नहीं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। रामायण में ऐसा लिखा है कि राम और सीता लंका से लौट कर बड़े आनन्द से रह रहे थे। सब ठीक-ठाक चल रहा था...। जीवन पटरी पर आ गया था। लेकिन जैसे की हर युग में पर दुख संतापी होते हैं राम राज्य में भी थे...उनके पेट में बात पची नहीं....।
यह प्रसंग बड़ा ही रोचक, जगानेवाला और दुख दाई है । कथाओं से ऐसा लगता है कि राम और सीता ने सुख के दिन देखे ही नहीं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। रामायण में ऐसा लिखा है कि राम और सीता लंका से लौट कर बड़े आनन्द से रह रहे थे। सब ठीक-ठाक चल रहा था...। जीवन पटरी पर आ गया था। लेकिन जैसे की हर युग में पर दुख संतापी होते हैं राम राज्य में भी थे...उनके पेट में बात पची नहीं....।समय बीता ....देवी सीता पेट से हुईं....और उन्हें साथ लेकर राम अयोध्या की अशोकवनिका ( अन्त:पुर में विहार योग्य उपवन) में गए। वहाँ राम पुष्पराशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे। जहाँ नीचे कालीन भी बिछा हुआ था।
फिर जैसे देवराज इंद्र शची को मधु मैरेय ( एक प्रकार बहु प्रचलित मद्य) का पान कराते हैं उसी प्रकार कुकुत्स्थकुल भूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु मैरेय लेकर सीता जी को पिलाया।
फिर सेवकों ने राजोचित भोज्य पदार्थ जिसमें मांसादि थे और साथ ही फलों का प्रबंध किया और उसके बाद राजा राम के समीप नाचने और गाने की कला में निपुण अप्सराएँ और नाग कन्याएँ किन्नरियों के साथ मिल कर नृत्य करने लगीं।
इसके बाद हर्षित राम ने गर्भवती सीता से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ..बरारोहे मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूरा करूँ...। माता बनने जा रही खुश सीता ने राम से कहा कि मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है ...देव मैं गंगा तट पर रह कर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, मैं उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ...। देव फल मूल का आहार करनेवाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूँ यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है।
पत्नी सीता की इच्छा जान कर राम को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि तुम कल ही वहाँ जाओगी....इतना कह कर श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए।
फिर आगे वह हुआ जिसने सीता के जीवन की दिशा बदल दी । राम अपने तमाम 10 सखाओं से घिरे बैठे थे...उन्होंने कहा कि राज्य में आज कल किस बात की चर्चा विशेष रूप से है । उनके सखाओं में एक भद्र ने बताया कि जन समुदाय में सीता जी का रावन के द्वारा हरण होने और क्रीडा कानन अशोक वनिका में रखने के बाद भी आप द्वारा स्वीकार किया जाना सबसे अधिक चर्चा में है .....लोग अचंभित और परेशान है कि हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेगी...लोग जानना चाह रहे हैं कि आप ने कैसे स्वीकार कर लिया सीता को....बस.....सीता माता के सुख के दिन समाप्त हो गए........राम ने एक तरफा फैसला करके सीता को एक दिन नहीं सदा-सदा के लिए वन में त्याग देने का आदेश दिया .....वह भी लक्ष्मण को....
वन जाकर भी सीता को तो यही पता था कि वह तो अपनी इच्छा से घूमने आई है....गंगा के पावन तट पर.....बस उनकी खुशी के लिए....उसके प्यारे पति ने भेजा है......
देखें- गीता प्रेस गोरखपुर का श्री मद्वाल्मीकीय रामायण, द्वितीय भाग, उत्तर काण्ड के अध्याय 42 से 50 तक की पूरी कथा।
साभार- विनय पत्रिका